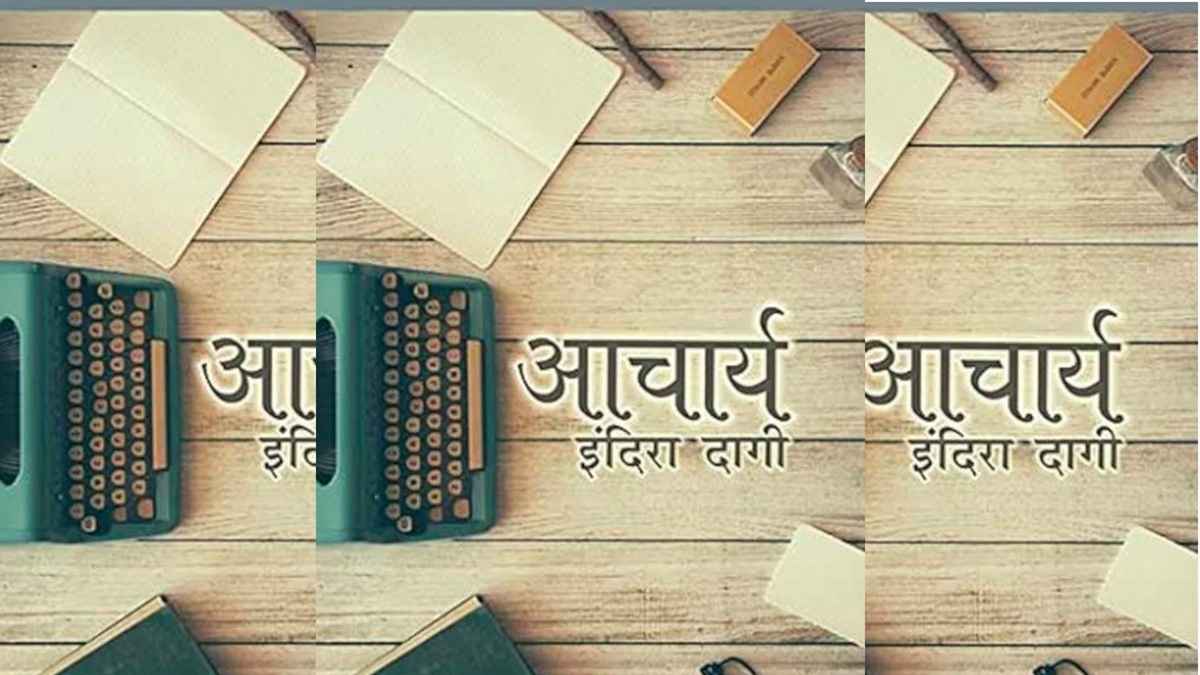
- July 22, 2025
- आब-ओ-हवा
- 1
पुस्तक समीक्षा: 'आचार्य'... लेखकों की भीतरी दुनिया का एक दृश्य
ब्रज श्रीवास्तव की कलम से....
कहा जाता है हर वह जगह जहाँ एकाधिक व्यक्ति रहते हैं, रंगमंच हो जाती है। वहां जीते जागते व्यक्ति अपने मंतव्यों की ख़ातिर जो करते हैं, वह अभिनय ही तो होता है और इस तरह हर व्यक्ति अनजाने में एक नाटक में शामिल हो जाता है। इस विचार का बारीक़ अवलोकन किया है चर्चित कथाकार इंदिरा दांगी ने अपने नाटक ‘आचार्य’ में। यह नाटक साहित्य के साथ–साथ रंग–संवाद की दुनिया में समूचे भरोसे के साथ क़दम इसलिए रख रहा है कि इसमें सौ प्रतिशत समकालीनता का रंग–ढंग घुला–मिला है।

‘आचार्य’, यह शीर्षक ही एक वातावरण ओर मनोदशा निर्मित करता है। हम जानते हैं भाषा किसी भी रचना को रोचक, गंभीर और कालजयी बनाने वाला उपकरण होती है, शब्द तो उतने ही हैं लेकिन एक मंझा हुआ लेखक अपने इच्छित वाक्य गठन में कौन–से शब्दों का प्रयोग करते हुए उसमे प्रभाव पैदा करता है, यही बोध उसे अपने समकालीनों से अलग पंक्ति में रेखांकित करता है। इंदिरा ने जिस त्वरण से अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाया है, उसमें भाषिक निर्वाह में की गयी सावधानी तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में क्लासिक अध्ययन के निष्कर्षों का प्रयोग भी सराहनीय है।
दरअसल ‘आचार्य’ में हम जो जान पाते हैं, वो है कि एक लेखक का जेन्युइन संघर्ष क्या होता है और यह भी कि कामयाब लेखकों की छद्म प्रवृति भी होती है। नाटक अपने मर्म को बहुत शिद्दत से और जस का तस सन्देश संप्रेषित करता है, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ होता है, जब अपने आदर्शों को स्थापित करने की कोशिश में नयी लेखिका रौशनी से वरिष्ठ लेखक विदुर दास संवाद करते हैं या जब सूर्यदेव सरकारी जैसा महत्वाकांक्षी, युक्तिलम्पट, अपने कुटिल खेल खेलता रहता है।
कदाचित इस तरह के विषय पर ‘आचार्य’ पहला नाटक हो सकता है। ख़ास बात यह है चूँकि यह एक कहानीकार ने लिखा है, तो इसका यथार्थ से वास्ता ज़्यादा ही सही लगता है। कुछ ही नाटक ऐसे होते हैं, जो दृश्य प्रधान होते हैं। इनमें दृश्य ही ज़्यादा मुखर होते हैं, पर इस नाटक में दृश्यों का संयोजन न तो लाउड है और न ही धीमे स्वर का है। यही वो मानक है, जो नाटक को क्लासिक कला के क़रीब बैठा सकने में कामयाब होता है।
इस नाटक में आरम्भ से अंत तक दृश्यों, संवादों की, भाव–भंगिमाओं की और उचित क्रमिकता का यथोचित संयोजन किया गया है। हालाँकि साहित्य और कला की दुनिया, पुरस्कारों की लाबिंग, पत्र–पत्रिकाओं में ख़ुद को या अपने पैनल के लेखकों को स्थापित करने के लिए गुपचुप की जाने वाली कार्यवाहियां, कोई ऐसा नया विषय भी नहीं हैं कि लोगों को मालूम ही न हो। पर यह नाटक कदाचित इसलिए क़ाबिले–ग़ौर है कि इसको लिखने वाली एक कहानीकार है ओर निश्चित तौर पर यह अनुभव ओर संवेदन से उपजी ओर सिरजी मानी जाने की संभावना रखने वाली रचना मानी जा सकती है।
पूरी दुनिया के साहित्य के दृश्य में नाटकों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शेक्सपियर और बर्तोल्त ब्रेख्त के अनगिन नाटक लोकप्रिय हैं। वहीं भारतीय साहित्य के दृश्य में हमें पता है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तो एक आधारशिला ही है। आगे कालिदास आते हैं और फिर आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र से होते हुए यह सफ़र मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, हबीब तनवीर तक आगे बढ़ता है और फिर कुछ मंद स्वर में अब के लेखक नाटक लिखते हैं। जबकि कविता संग्रह, कहानी संग्रहों की आमद अच्छी–ख़ासी रही आयी, ऐसे में नाटक अकेले पड़ गये और उनका आना लगभग बंद–सा हो गया, ऐसे में नाटक ‘आचार्य’ की आमद एक उम्मीद की आमद की तरह देखी जा सकती है। ज़ाहिर है अब यह रंगमंच की ओर उम्मीद भरी निगाह से देखेगा और मुमकिन है यह वहां स्थापित हो जाये।
नाटक की कुछ ख़ास–ख़ास बातों पर चर्चा करना हो तो कहा जा सकता है कि वहाँ एक ही घटनास्थल है, जो पत्रिका का दफ़्तर है। लेखक–लेखिका ही इसके पात्र हैं, पेपरवेट, टेबल, परदे, काउच, चाय, कॉफ़ी, बोनसाई का पौधा और कुछ ओर बेजान–सी चीज़ें भी नाटक में जान डालने का कम करती हैं। पत्रिका के संपादक जी अपने दफ़्तर में ही आते–जाते लेखकों से यथोचित संवाद करते हैं, बीच–बीच में नवोदित लेखिका जिसका नाम रौशनी है, सूत्रधार की भूमिका में बातें, सवाल करते हुए नाटक को उद्देश्यपूर्ण बनाती रहती है। संपादक जी, आगंतुकों से बातचीत ओर आवभगत करते हुए, प्रिय लगने लगते हैं और पाठक उनके विचारों के संग हो जाता है। पुरुष लेखकों का महिला लेखिकाओं के प्रति जो आकर्षित व्यवहार हुआ करता है। वह बड़ी बारीक़ी से दर्शाया गया है, उन्हें भाव–पाश में लेने की प्रवृति के साथ महिला लेखिकाएं भी किस तरह से ये सब डील करके लाभ लेती हैं, उसका अंश भी यहाँ है। निसंदेह ‘रौशनी’ इस नाटक की मुख्य पात्र है, जो बहुत ज़हीन, सतर्क और कुशल समन्वयक है, जो बड़े–बड़े लेखकों को अपने प्रश्नों, जिज्ञासाओं और तर्कों से भी नये तरह से सोचने को मजबूर कर देती है। जब एक सुयोग्य लेखक को एक जुगाड़ू लेखक संपादक की कुर्सी से हटाने की कुटिल चाल में कामयाब हो जाता है तब यह ‘रौशनी’ नाम की लेखिका ही उन्हें न केवल संभालती है, बल्कि अपनी पक्षधरता भी स्पष्ट करती है।
‘आचार्य’ एक ऐसा ही नाटक है, जिसमें एक यथार्थ पिन्हां है। साहित्य जो एकमात्र भरोसे का क्षेत्र रह गया था, उसमें भी महत्वाकांक्षी और फ़र्ज़ी लेखक घुसपैठ करके वास्तविक लेखकों का गला दबा रहे हैं। एक चिंता का विषय बन गया है। यह हम तब और भली–भांति समझते हैं, जब मंजी हुई भाषा, सुगठित दृश्यों ओर सटीक संवादों से रचा इंदिरा दांगी का यह नाटक पढ़ते जाते हैं।
उम्मीद की जाना चाहिए कि साहित्यिक और सांस्कृतिक हलकों के अलावा इस नाटक के सन्देश और वास्तविकता को दर्शक और पाठक भी पर्याप्त तवज्जो देंगे।

ब्रज श्रीवास्तव
कोई संपादक समकालीन काव्य परिदृश्य में एक युवा स्वर कहता है तो कोई स्थापित कवि। ब्रज कवि होने के साथ ख़ुद एक संपादक भी हैं, 'साहित्य की बात' नामक समूह के संचालक भी और राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक आयोजनों के सूत्रधार भी। उनके आधा दर्जन कविता संग्रह आ चुके हैं और इतने ही संकलनों का संपादन भी वह कर चुके हैं। गायन, चित्र, पोस्टर आदि सृजन भी उनके कला व्यक्तित्व के आयाम हैं।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky


मंझी हुई सारगर्भित समीक्षा…
बहुत-बहुत बधाई