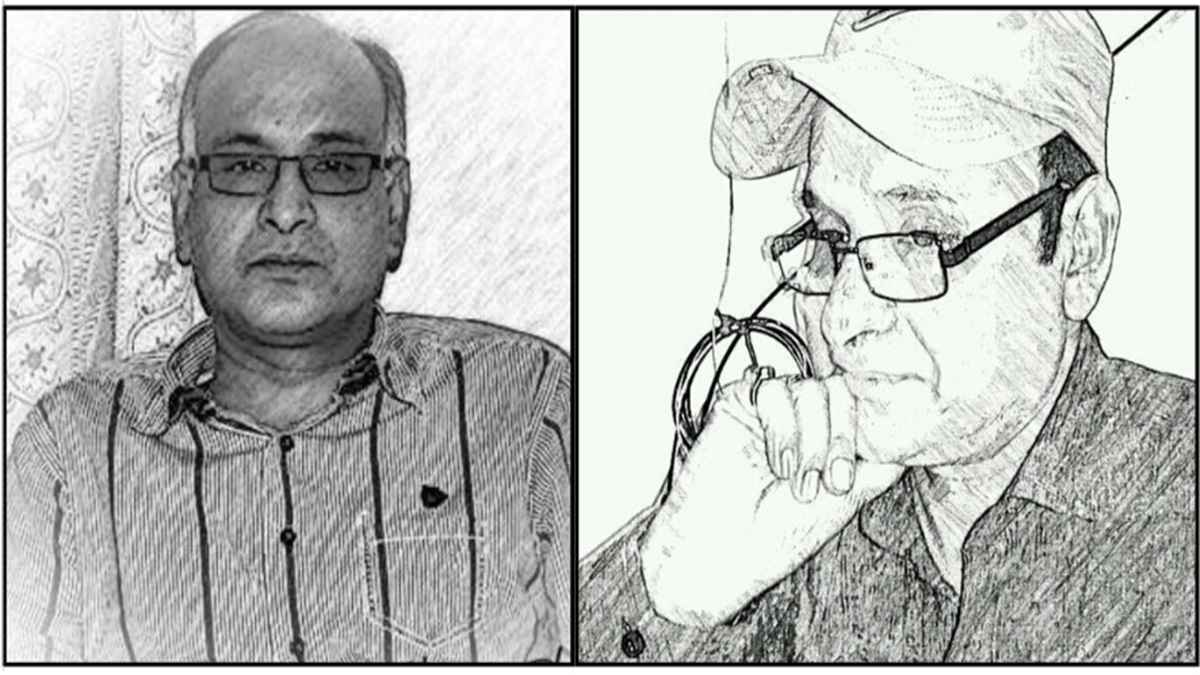
- July 1, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-2
पढ़ना और गढ़ना
1 जनवरी, 2014
पढ़ने और गढ़ने में ज़मीन-आसमान का अंतर है। शायद कोई अजीब-सी उलझन में हूँ। किताबों के पन्नों और जीवन की राहों के बीच की खाई पर सोच रहा हूँ। पढ़ना और गढ़ना—ये दो अलग-अलग संसार हैं, जैसे आकाश और धरती। किताबें ज्ञान की नदियाँ हैं, लेकिन अगर उनका जल जीवन की मिट्टी को सींचे नहीं, तो वह सिर्फ़ शब्दों का शोर बनकर रह जाता है।
कुछ लोग किताबों को सिर्फ़ पढ़ते हैं- उनके दिमाग़ में शब्द ठहरते हैं, लेकिन दिल तक नहीं उतरते। और कुछ हैं, जो पढ़कर उसे अपने जीवन में रचते हैं, जैसे कोई माली बीज बोकर पेड़ उगाता है। किताब का सच्चा पाठक वही है, जो उसके विचारों को अपने आचरण का रंग देता है। वही तो बड़ा इंसान बनता है- न कि वह, जो सिर्फ़ बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने का दावा करता है।
सोचता हूँ, अगर पढ़ना ही इंसान को बड़ा बना देता, तो क्या वजह है कि तथाकथित ‘बड़ी किताबों’ के पाठक आज भी छोटे-छोटे विचारों में उलझे रहते हैं? पढ़े-लिखे समाज में छोटेपन की यह बाढ़ क्यों? शायद इसलिए कि किताबें उनके लिए सिर्फ़ अलमारियों की शोभा हैं, जीवन का हिस्सा नहीं। साहित्य की दुनिया में यह और भी साफ़ दिखता है। वहाँ लेखक शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन उनके आचरण में वह जादू कहीं खो जाता है। वे कहते हैं, “लेखक का निजी जीवन और उसकी रचना को जोड़कर मत देखो।” लेकिन क्या यह सच नहीं कि शब्दों का असर तभी है, जब वे लिखने वाले के जीवन में भी झलकें?
मन में एक बिंब उभरता है— लेखक एक दीपक की तरह है। अगर उसका तेल सिर्फ़ कागज़ पर जलता है, तो वह रोशनी देता है, पर गर्माहट नहीं। सच्चा लेखक, सच्चा पाठक वही है, जो अपने पढ़े और लिखे को जीवन की लौ बनाये। किताबें तो सिर्फ़ नक्शा हैं; राह चलकर ही मंज़िल मिलती है।
अधकचरा चरित्र
आज सुबह, पुलिस लाइन के मैदान से सुबह की सैर के बाद लौट रहा था- कचरे का ढेर देखकर मन फिर खिन्न हो उठा। हम सब कितना नापसंद करते हैं इस कचरे को- अपने घरों में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। हर दिन उसे साफ़ करते हैं, एकत्र करते हैं और बिना सोचे-समझे घर के बाहर फेंक आते हैं।
कहाँ फेंका? किसके दरवाज़े पर? क्या वहाँ की हवा दूषित होगी? क्या किसी का स्वास्थ्य ख़राब होगा? इन सवालों से हमारा कोई वास्ता नहीं।
मैं भी तो यही करता हूँ। कचरे को बाहर फेंककर, उसकी सड़ांध से उपजी बदबू के लिए व्यवस्था को कोसता हूँ। कितना आसान है दोष मढ़ देना! पर सच तो यह है कि मेरा कचरा-विरोध कितना अधूरा, कितना आधा-अधूरा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पड़ोस चमके, मेरा शहर स्वच्छ हो, मेरा देश कचरे से मुक्त हो– लेकिन जब बात उस कचरे को हटाने की आती है, तो मैं औरों की ओर देखने लगता हूँ। सड़क पर कूड़ा दिखे, तो मन में उबाल आता है, पर उसे उठाने की बजाय मैं सरकारी तंत्र को भला-बुरा कहक़र आगे बढ़ जाता हूँ।
यह कैसा कचरा-विरोध है मेरा? यह तो अधकचरा चरित्र है- बाहर की सड़ांध को कोसने वाला, पर भीतर की ज़िम्मेदारी से भागने वाला। कचरा सिर्फ़ सड़कों पर ही नहीं, हमारे मन में भी जमा है- उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ने की वह गंदगी, जो हमें सच्चा कचरा-विरोधी बनने से रोकती है। शायद आज से मैं थोड़ा और सोचूँ, थोड़ा और करूँ। कचरे को सिर्फ़ बाहर फेंकने की बजाय, उसे सही जगह तक पहुँचाने की आदत डालूँ क्योंकि स्वच्छता सिर्फ़ घर की नहीं, मन और समाज की भी होनी चाहिए।
प्रजातंत्र
प्रजातंत्र— यह शब्द कितना सुंदर है, कितना भरोसा जगाता है। प्रजा और तंत्र का मेल, मानो जन की आवाज़ का तंत्र के कंधों पर चढ़कर गूँजना। लेकिन हक़ीक़त में क्या यह वही प्रजातंत्र है, जिसका सपना आज़ादी के मतवालों ने देखा था? या यह तंत्र का वह जाल है, जो प्रजा को अपने इशारों पर नचाता है? शब्द में तो प्रजा पहले आती है, पर व्यवहार में तंत्र का डंका बजता है। यह तंत्र, जो प्रजा का अनुगामी होना चाहिए, कहीं उसका स्वामी तो नहीं बन बैठा?
आज का भारतीय प्रजातंत्र एक विचित्र द्वंद्व में जी रहा है। एक ओर, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है- लाखों-करोड़ों मतदाताओं की उंगलियों पर स्याही का निशान, चुनावों का महोत्सव, और संविधान की वह किताब, जो हर नागरिक को समानता का वचन देती है। दूसरी ओर, यह तंत्र उसी प्रजा को थका देता है, जिसके लिए वह बना। नौकरशाही का जंगल, नीतियों का भंवरजाल, और सत्ता का वह अहंकार, जो जन की पुकार को कागज़ों के ढेर में दफ़न कर देता है। क्या यही प्रजातंत्र है? या यह अँग्रेज़ों का छोड़ा हुआ तंत्र है, जो सिर्फ़ चेहरा बदलकर अब भी तानाशाही की भाषा बोलता है?
सच्चा प्रजातंत्र तब तक अधूरा है, जब तक प्रजा तंत्र की बागडोर अपने हाथों में न ले ले। यह बागडोर कोई भौतिक लगाम नहीं, बल्कि वह जागरूकता है, जो प्रजा को अपने अधिकारों का पहरेदार बनाती है। आज हमारी प्रजा को वोट का हक़ तो है, पर क्या उसे तंत्र को सवाल करने की ताक़त भी है? क्या वह तंत्र के सामने अपनी बात रखने में सक्षम है, या सिर्फ़ वादों के भरोसे अगले चुनाव तक ठगी जाती है? भारतीय लोकतंत्र में प्रजा की आवाज़ अक्सर मतपेटी तक सिमटकर रह जाती है। उसके बाद तंत्र अपनी चाल चलता है- कभी विकास के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर, और कभी धर्म-जाति के उन्माद में उलझाकर।
इसका निवारण क्या है? पहला क़दम है प्रजा का सशक्तिकरण- न सिर्फ़ शिक्षा से, बल्कि उस चेतना से, जो उसे तंत्र का हिस्सा बनाये। सूचना का अधिकार, स्थानीय शासन में भागीदारी और तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले कानून इस दिशा में मील के पत्थर हो सकते हैं। लेकिन यह तब तक संभव नहीं, जब तक तंत्र स्वयं को प्रजा का सेवक न माने। आज का तंत्र अक्सर प्रजा को अपनी प्रजा समझता है, न कि स्वयं को प्रजा का अनुचर। यह मानसिकता अंग्रेज़ी शासन की देन है, जहाँ तंत्र का मतलब था नियंत्रण, न कि सेवा।
सच्ची ख़ुशहाली का रास्ता तभी खुलेगा, जब तंत्र प्रजा की आकांक्षाओं का दर्पण बने। जब हर गाँव का स्कूल, हर शहर का अस्पताल, और हर खेत की फसल तंत्र की प्राथमिकता बने। जब प्रजा सिर्फ़ वोटर न रहे, बल्कि नीति-निर्माण की साझेदार बने। तब शायद वह दिन आएगा, जब प्रजातंत्र सिर्फ़ शब्द नहीं, बल्कि एक जीवंत सच्चाई होगा- जहाँ तंत्र प्रजा के पीछे चले, न कि उसे हाँके।
क्रमश:
(पूर्वपाठ के अंतर्गत यहां डायरी अंशों को सिलसिलेवार ढंग से सप्ताह में दो दिन हर शनिवार एवं मंगलवार प्रकाशित किया जा रहा है। इस डायरी की पांडुलिपि लगभग तैयार है और यह जल्द ही पुस्तकाकार प्रकाशित होने जा रही है। पूर्वपाठ का मंतव्य यह है कि प्रकाशन से पहले लेखक एवं पाठकों के बीच संवाद स्थापित हो।)

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

