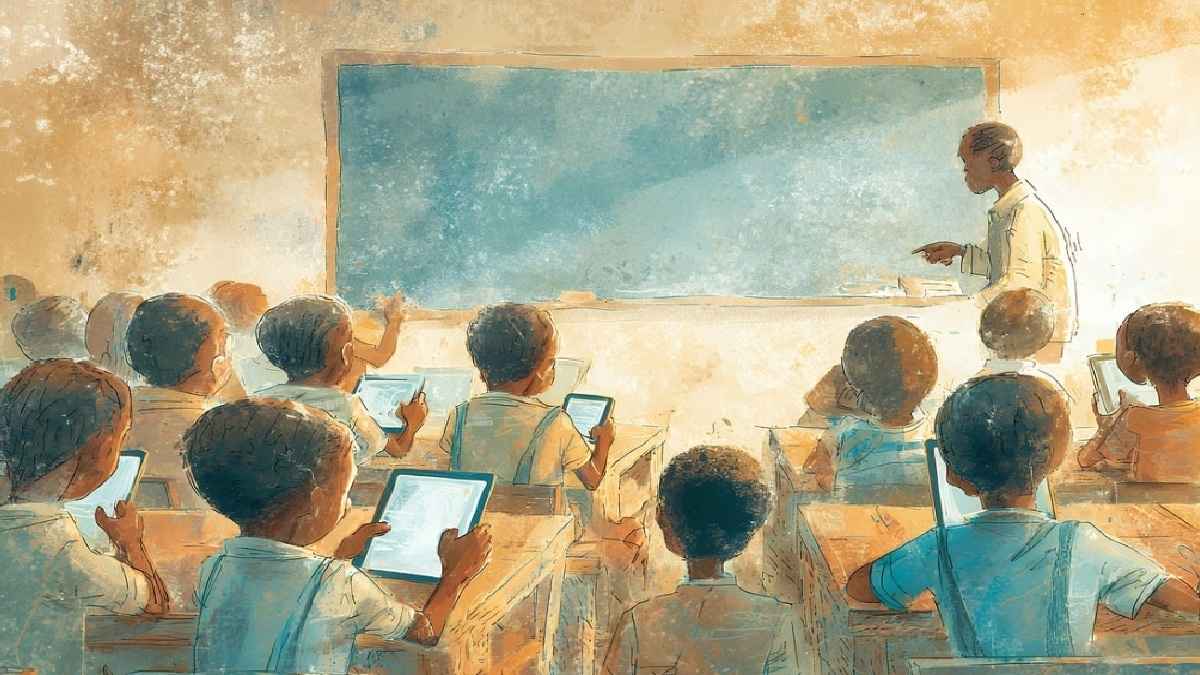
- September 5, 2025
- आब-ओ-हवा
- 1
मूल लेख रोहित धनकर... अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद ब्रज श्रीवास्तव की कलम से....
ज्ञान की भूमिका और विशेषता
किसी निष्कर्ष तक पहुँचने की प्रक्रिया में ज्ञान एक मुख्य घटक होता है। वैसे नैतिक मूल्यों का भी आधारभूत महत्व होता है, लेकिन इनसे सम्बन्धी बोध के लिए, समझ और अनुभव के लिए भी ज्ञान की ही आवश्यकता होती है क्योंकि कोई बात बिना समझे और बिना बौद्धिक तरह से प्रमाणित किये, उसे कोरी भावुकता के साथ संचारित करना अपना मत औरों पर थोपने से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई मूल्य स्थिरता लिये है कि नहीं, इस बात के प्रति सजग होने के लिए भी स्थिति के सापेक्ष उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। हालाँकि किसी भी निर्णयात्मक प्रक्रिया को, इसके भावनात्मक पक्ष के बिना पूर्ण नहीं माना जा सकता। वास्तव में तो स्थिति से उपजे असंतोष के कारण ही एक निष्कर्ष की आवश्यकता का सवाल खड़ा होता है। प्रकारांतर से यह भावनात्मकता की स्वीकृति ही है। परन्तु बमुश्किल प्राप्त नयी स्थिति के लिए पर्याप्त समझ बनाये बिना किसी ठोस निर्णय तक पहुंचना संभव नहीं होता इसीलिए मैं कहता हूँ कि निर्णय निर्धारण का प्रतिफल पाने के लिए ज्ञान का निवेश करना एक मुख्य काम होता है।
ज्ञान और कल्पना दोनों के दायरे में विचार करते हुए मैं प्रमाणित सत्य विश्वास (justified true belief) को ज्ञान का केन्द्र मानता हूँ। यद्यपि सत्य और प्रमाणीकरण की प्रचलित धारणाएं ज्ञान के जन मापदंड तय करने में काफ़ी हद तक भ्रम पैदा करती हैं तथापि हम जीवन में कई मौक़ों पर प्रमाणित सत्य विश्वासों (justified true belief) की ज़रूरत होने पर भी ध्यान नहीं देते और निर्णय पर यह मानकर अमल कर लेते हैं कि ये उचित ही होंगे। जबकि अमल के दौरान हम उनकी सच्चाई के बारे में सुनिश्चित नहीं होते हैं।
उपर्युक्त दोनों बातें यदि मायने रखती हैं तो ज्ञान की गुणवत्ता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और निर्णय भी महत्वपूर्ण असर डालते हैं। यहाँ ज्ञान की गुणवत्ता के पद का उपयोग हम समूची कार्य योजना के स्थान पर करते हैं। किसी को ज्ञान की गुणवत्ता की धारणा अनुचित सी लग सकती है क्योंकि प्रमाणित सत्य विश्वास अंततः सत्यता को ही सुनिश्चित करने वाला पद है। इसके अलावा ज्ञान का निहितार्थ होगा भी क्या। प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि यह धारणा निर्णय निर्धारण के लिए उपयोगी ही है, जिसका सामान्यतः भी महत्व है। इसीलिए पुरे विश्लेषण के लिए थोड़ी गुंजाईश रखते हुए, निर्णय निर्धारण की स्थिति में ज्ञान की गुणवत्ता के पहले अंश पर ज़ोर देने के दौरान मैं ज्ञान पर ही फ़ोकस करूँगा।
किसी भी निर्णय के निर्धारण के समय उस स्थिति में तीन बातें विचारणीय होती हैं, मुद्दों की यथास्थिति, चाही गयी स्थिति और वे तरीक़े जिनको अपनाकर कोई स्थिति, वांछित अवस्था में तब्दील होती है। और सबसे ख़ास तो होते हैं दुविधा रूपी मेज़बान, जो महत्वपूर्ण निर्णय के समय और ज़्यादा परेशां करते हैं। अगर इस सतही विश्लेषण के महत्व को हम ज़्यादा तवज्जो न देते हुए मान लें कि ये मूल्य ही निर्णय के निर्धारण को राह दिखाते हैं तो ये दुविधा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है।
तात्कालिक रूप से कहा जा सकता है कि ज्ञान के सन्दर्भ में ज़रूरी बात होती है, पर्याप्तता। किसी स्थिति और असंतोषजनक स्थिति के बारे में पर्याप्त समझ का मतलब है सम्बंधित कारणों की समझ होना, जिनकी वजह से असंतोष उपज आया है, पर्याप्तता से आशय यहाँ मात्रात्मकता से नही, बल्कि थोडा ज़्यादा है, यहाँ पर्याप्तता से आशय है कि संबंधित सब कुछ जान लिया गया है।
यही बात वांछित परिस्थिति हासिल करने के लिए और वांछित परिणाम प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी है। ज्ञान की गुणवत्ता की दूसरी लड़ी है, उपयोग में लायी जा रही सूचनाओं या विश्वासों की स्पष्टता। कोई दावा करते हुए यह कह भी सकता है कि पर्याप्तता में ही स्पष्टता शामिल है क्योंकि कोई अस्पष्ट चीज़ कैसे अर्जित ज्ञान का हिस्सा हो सकती है। मैं स्पष्टता का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी लक्षित चीज़ के होने का हमें आभास तो होता है मगर हमारा नज़रिया उसके प्रति अपेक्षाकृत बताने में कतराने वाला होता है। उदाहरण के लिए अँधेरे में जब कोई चीज़ हमारी ओर आ रही होती है तो हम यह तय नहीं कर पाते कि वो चीज़ अमुक चीज़ है, अलबत्ता उसकी आकृति और लम्बाई चौड़ाई से हम कुछ कुछ अंदाज़ा लगाते ही हैं। मगर उस आकृति के ठीक ठीक लक्षण हमें याद नहीं रह पाते। ज्ञान के सन्दर्भ में स्पष्टता का अभाव दरअसल हमारी निर्णय क्षमता को पंगु बना देता है। ख़ास तौर से तब जब दूसरों के न्याय करने का मसला हो, वह भी गहरी भावना से संबद्ध।
ज्ञान की गहनता मुझे ज्ञान का एक और आयाम मालूम होता है, जो कि अंततः उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे कि पर्याप्तता। गहनता से अभिप्राय अवधारणात्मक संपर्कों की ऐसी सुगम पहुँच प्रणाली से है, जो न केवल मौजूद स्थिति में उसे विश्लेषित कर सके बल्कि उन कारणों पर भी प्रकाश डाल सके, जिन्होंने इन्हें जन्मा है। वे कारण प्राक्रतिक, ऐतिहासिक या सामाजिक हो सकते हैं। और यह भी कि यह इच्छित परिणाम लाने के लिए अमल की योजना में और बदलावों के भरोसेमंद पायदानों में भी मददगार होना चाहिए।
अगर हम विश्वस्त ज्ञान की बात करते हैं तो उसे तर्कसंगत व्यवहार से स्थापित करना एक ज़रूरी शर्त है। यह कहना यहाँ लाज़िमी है कि प्रमाणीकरण की दृढ़ता को ही किसी विशेष निर्णय निर्धारण सन्दर्भ में ज्ञान की गुणवत्ता के आयाम के रूप में बेहतर समझा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि व्यावहारिक दुनिया में ज़्यादातर उपयोग किया जाने वाला ज्ञान दोषयुक्त होता है। अधिकांशतः सही प्रमाणीकरण तो मिलता ही नहीं इसलिए विशेष निर्णय निर्धारण की स्थिति में विश्वासों के प्रमाणीकरण की विश्वसनीयता, गुणवत्ता का ख़ास आकलन होती है। इसलिए मोटे रूप से विश्लेषण में हम कह सकते हैं कि निर्णय निर्धारण में ज्ञान की विशिष्टता, पर्याप्तता, स्पष्टता, गहनता और प्रामाणिकता की विश्सनीयता के रूप में समझी जा सकती है। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान की विशेषता, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अपर्याप्त, अस्पष्ट, धुंधला और अप्रमाणित ज्ञान किसी काम का नहीं होता, यह किसी की मदद नहीं करता।
अगर हम कक्षा में एक शिक्षक की स्थिति को ध्यान में रखकर सोचें तो वह प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में सैकड़ों निर्णयों का निर्धारण करता है, यद्यपि ऐसे निर्णय मामूली से लगते हैं जैसे कि दो बच्चे जब झगड़ा कर रहे हैं तो किसकी ग़लती मानी जाये? यह भी एक फ़ैसला तो होता ही है, जो बच्चे की ज़िंदगी पर असर डाल सकता है। तो शिक्षक आम तौर पर ऊपर वर्णित ज्ञान के सन्दर्भों से इतर अपने कमज़ोर ज्ञान के बल पर फ़ैसले लिया करते हैं। यह भी एक बड़ी वजह है कि प्रारंभिक स्कूलो में अध्यापन इतना उबाऊ और थका हुआ सा है। इस तरह से शिक्षक को जबरन ही निर्णय निर्धारण में फंसा दिया जाता है जबकि वह अपने ज्ञान की सीमा को ख़ुद ही जानता है। यह सब कुछ तनावजन्य होता है।
जीवन में ख़ुश रहने के लिए, प्रेरणा का आधार देने वाली सामाजिक और वैयक्तिक सम्बद्धता में हम पुनः अपने इसी अधूरे और कमज़ोर ज्ञान के बल पर ही धकेल दिये जाते हैं। जहाँ अपनी ही सोच मुख्य मार्गदर्शक की भूमिका में होती है और भावनाएं हावी हो जाया करती हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई इस आदर्श ज्ञान की विशेषता पर अमल करने की नाकाम कोशिश करता है, तो वह भ्रमित और बेवकूफ़ कहा जा सकता है। ख़ास तौर से तब जब परिणाम आने के दौरान थोड़ा अधिक समय लग रहा होता है। यह तय है कि अथक परिश्रम और धीरज ज्ञान की इस विशेषता को समझने के लिए बेहतर परिणाम देते हैं। साथ ही यह भी कि अगर दोषपूर्ण या आधा अधूरा ज्ञान हो तो और व्यक्तिगत या व्यावसायिक मामले में किसी ख़ास स्थिति का निर्णय निर्धारण करना हो तो हमेशा अपनी बात को ज़ोरदार तरीक़े से रखना मानीख़ेज़ होता है, बच्चों को ज्ञान की विशेषता सिखाने के अंतर्गत, जहाँ कुछ करना ही पड़े तो जोखिम लेना और परिस्थिति बिगड़ जाने पर उनका सामना करने की तैयारी करना भी सिखाना चाहिए। व्यक्तिगत या व्यावसायिक मामले में यह सिखाना भी शिक्षा का एक उद्देश्य हो सकता है।

ब्रज श्रीवास्तव
कोई संपादक समकालीन काव्य परिदृश्य में एक युवा स्वर कहता है तो कोई स्थापित कवि। ब्रज कवि होने के साथ ख़ुद एक संपादक भी हैं, 'साहित्य की बात' नामक समूह के संचालक भी और राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक आयोजनों के सूत्रधार भी। उनके आधा दर्जन कविता संग्रह आ चुके हैं और इतने ही संकलनों का संपादन भी वह कर चुके हैं। गायन, चित्र, पोस्टर आदि सृजन भी उनके कला व्यक्तित्व के आयाम हैं।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky


अथक परिश्रम और धीरजता से सधी लेखनी ज्ञान की पाठशाला में अपनी भूमिका निर्वहन करती….
बहुत-बहुत बधाई, भाई