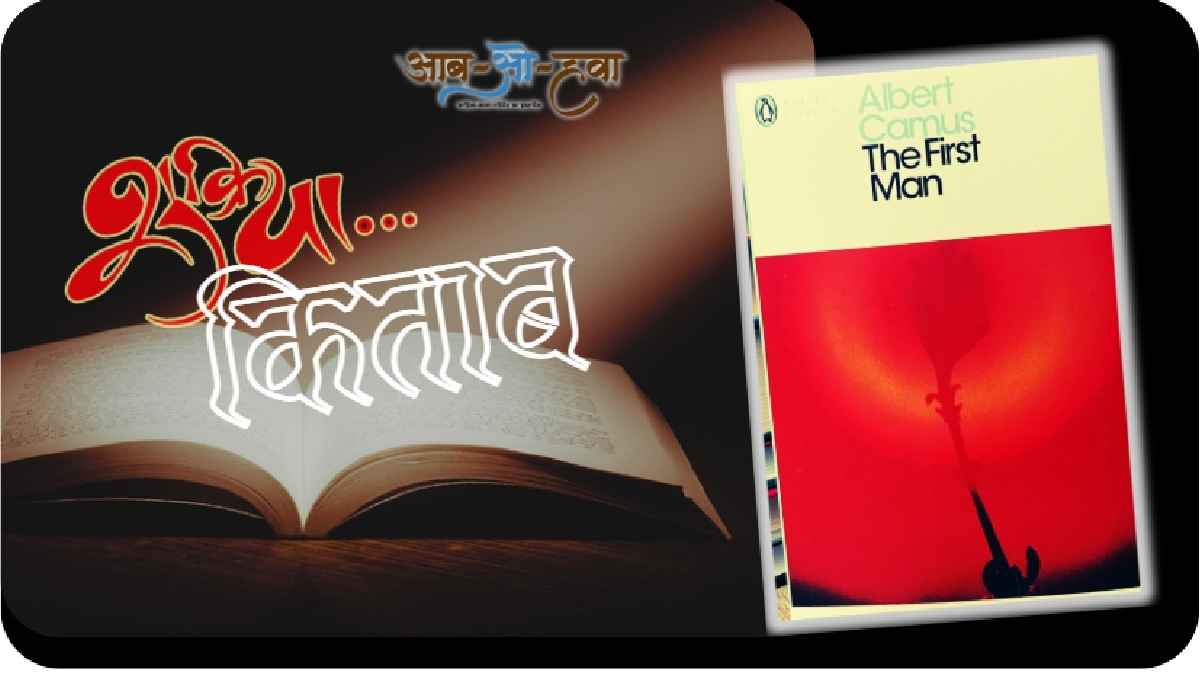
- July 21, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
(विधाओं, विषयों व भाषाओं की सीमा से परे.. मानवता के संसार की अनमोल किताब -धरोहर- को हस्तांतरित करने की पहल। जीवन को नये अर्थ, नयी दिशा, नयी सोच देने वाली किताबों के लिए कृतज्ञता का एक भाव। इस सिलसिले में लगातार साथी जुड़ रहे हैं। साप्ताहिक पेशकश के रूप में हर सोमवार आब-ओ-हवा पर एक अमूल्य पुस्तक का साथ यानी 'शुक्रिया किताब'... -संपादक)
पहले आदमी की तलाश: पाठक को गरिमा देता कामू का उपन्यास
“पहले आदमी की तलाश” फ्रांस के ख्यतिप्राप्त लेखक अलब्येर कामू की एक अधूरी रचना है। इससे पहले ही कामू “आउटसाइडर” और “प्लेग” के लेखक रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। 60 के दशक में ही उनकी मृत्यु मात्र 43 की उम्र में हो गयी थी। “ला प्रीमियम होमे” (जो एक अधूरा उपन्यास है) पचास के दशक में लिखा गया था, पर इसका प्रकाशन कामू की मृत्यु के कई सालों बाद 1994 में संभव हो पाया।
यह उपन्यास कामू की नज़र में भी एक महत्वपूर्ण कृति होने वाली थी। प्रकाशन के पश्चात इसने पश्चिमी जगत में तहलका मचा दिया था। पर बाद में इसे पूरी तरह सबोटाज करने की कोशिश की गयी, क्योंकि तब तक पश्चिमी जगत पूरी तरह पूंजीवाद के गिरफ़्त में क़ैद हो चुका था और यह उपन्यास खुले तौर पर पूंजीवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा था, उसे मनुष्यता विरोधी साबित कर रहा था।
इस उपन्यास की अर्थवत्ता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध आलोचक आनन्द प्रकाश लिखते हैं, “इसमें अद्भुत प्रयोगशीलता और सृजनात्मक श्रम का साक्ष्य मिलता है।” माना जाता है उपन्यास अपने वक़्त का इतिहास होता है, पर यह उपन्यास अपने वक़्त का लेखा-जोखा मात्र नहीं बल्कि इतहास के एक लम्बे त्रासद दौर का प्रतिफलन है।

दूसरे महायुद्ध और शीतयुद्ध के समापन तक के इतिहास पर नज़र डालें तो इस उपन्यास की आवश्यकता और अर्थवत्ता दोनों देख पाएंगे क्योंकि कामू इसी दौर में पैदा हुए और मरे। कामू ने आंखें ही खोली थीं, दूसरे महायुद्ध के विध्वंस और नाश के माहौल में, जब मानवता लहूलुहान थी। मानवीय मूल्य अपनी गरिमा खो रहे थे। पूरी दुनिया में विशेषकर पश्चिमी जगत में निराशा, एकाकीपन, हताशा का वातावरण व्याप्त हो गया था। मनुष्यता का हनन इस क़दर हो गया था कि मनुष्य अपने ही देश में, अपने ही समाज में हताशा और निराशा के कारण आत्महत्या को बेहतर समझने लगा था। समाज में सहभागिता और संवेदना लुप्त होती जा रही थी। मनुष्य के लिए समाज नहीं रह गया था। समाज उसे घुट-घुटकर जीने के लिए विवश कर रहा था।
ऐसे ही भयावह ऐतिहासिक दौर और परिवेश में कामू ने अपना जीवन व्यतीत किया। और इन्हीं भयानक मनुष्य विरोधी परिस्थितियों के कारण अस्तित्ववादी दर्शन का जन्म हुआ। जिस दर्शन ने मनुष्य (अस्तित्व) की वकालत की। कामू को भी अस्तित्ववादी ही माना गया। कामू के चिन्तन में भी मनुष्य और मनुष्यता ही मूल रूप से थे, पर उनका अस्तित्ववाद, अस्तित्ववादियों से भिन्न था। उनका मक़सद मनुष्य की दुर्दशा का, उसकी व्याकुलता का या उसके कष्ट का महज़ वर्णन करना नहीं बल्कि उस दिशा की तलाश थी, उस समाज की परिकल्पना थी, जिसे जाक केरोमेरी ने इस उपन्यास में मूर्त रूप दिया है। इस उपन्यास के कामू एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें व्यवसाय का, धन का नियंत्रण न हो। हर व्यक्ति की समाज में भागीदारी हो, संवेदना हो, मनुष्यता के प्रति आस्था हो।
इस उपन्यास के माध्यम से कामू पश्चिमी पूंजीवादी समाजों की संवेदनहीनता और मानव-विरोधी संरचना की घोर निंदा करते हैं। इस उपन्यास के पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ने से न रोका गया तो मनुष्य, मनुष्य नहीं रह जाएगा, वह एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा।
कामू की यह चुनौती आज कितना मायने रखती है, हम आसानी से देख और समझ पा रहे हैं। आज हम एक ऐसे समाज में जीने को विवश हैं, जिसमें न विश्वास है, न सहभागिता है और न ही संवेदना, बस सब एक अंधी दौड़ में शामिल हैं और दौड़ते रहने को बाध्य कर दिये गये हैं।
उपन्यास में कामू ने एक तरफ समाज में व्याप्त अन्धविश्वास, धर्मांधता, रूढ़ परम्पराओं की सख़्त आलोचना की है और दूसरी तरफ़ पूंजीवाद को राक्षस और मानवता का दुश्मन माना है। और एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जो समानता, स्वतंत्रता और सहभागिता पर आधारित होगा। उसका विश्वास है कि उस समाज का निर्माण मेहनतकश आम लोगों के द्वारा ही होगा।
“कामू को पढ़ने पर पाठक गरिमा महसूस करता है- मनुष्य होने की और मनुष्य के अस्तित्व की।” (आनन्द प्रकाश)
यही लेखन की मूल कसौटी भी है।
‘पहले आदमी की तलाश’ मेरे पसन्दीदा उपन्यासों में से एक रहा है। इसकी वजहें रही हैं। आज हम इंसान नहीं एक आंकड़ा बन चुके हैं। और समाज में रहकर भी तन्हा-तन्हा हैं। बाज़ारवाद ने हमें एक अंधी दौड़ में झोंक दिया है और हम उसमें दौड़ते-दौड़ते मर जाने को बाध्य हैं। यह उपन्यास आदमी को आदमी बनाये रखने की वकालत करता है। मनुष्य की मनुष्यता को बचाने की बात करता है। समाज में समानता, भाईचारा और भागीदारी की बात करता है। और आम आदमी की ताक़त को पहचानता है। उसकी एका की ताकत में विश्वास प्रकट करता है। पूंजी संकेंद्रण, जो हमारी सारी परेशानियों की वजह है, की मुख़ालफ़त करता है।
(क्या ज़रूरी कि साहित्यकार हों, आप जो भी हैं, बस अगर किसी किताब ने आपको संवारा है तो उसे एक आभार देने का यह मंच आपके ही लिए है। टिप्पणी/समीक्षा/नोट/चिट्ठी.. जब भाषा की सीमा नहीं है तो किताब पर अपने विचार/भाव बयां करने के फ़ॉर्म की भी नहीं है। edit.aabohawa@gmail.com पर लिख भेजिए हमें अपने दिल के क़रीब रही किताब पर अपने महत्वपूर्ण विचार/भाव – संपादक)

अस्मिता सिंह
कहानीकार एवं आलोचक। लंबे समय तक मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में हिन्दी-साहित्य का अध्यापन। प्रमुख पुस्तकों में 'रंग से बेरंग होती ज़िंदगी', 'इन्तज़ार तो ख़त्म हुआ' (कहानी-संग्रह), 'फुलिया' (उपन्यास), 'शमशेर: अभिव्यक्ति की कशमकश (आलोचना पुस्तक), नारी मुक्ति: दशा एवं दिशा (नारी विमर्श), दलित अनुभव का सच (दलित-विमर्श) हैं। साथ ही, लू-शुन के पत्रों के अनुवाद और अन्य संकलित व संपादित पुस्तकें भी। बहुपठित एवं बहुप्रकाशित लेखक अस्मिता सिंह इन दिनों एस.ए. डांगे इंस्टीट्यूट आफ सोशलिस्ट स्टडीज़ एंड रिसर्च में निदेशक-प्रमुख हैं।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

