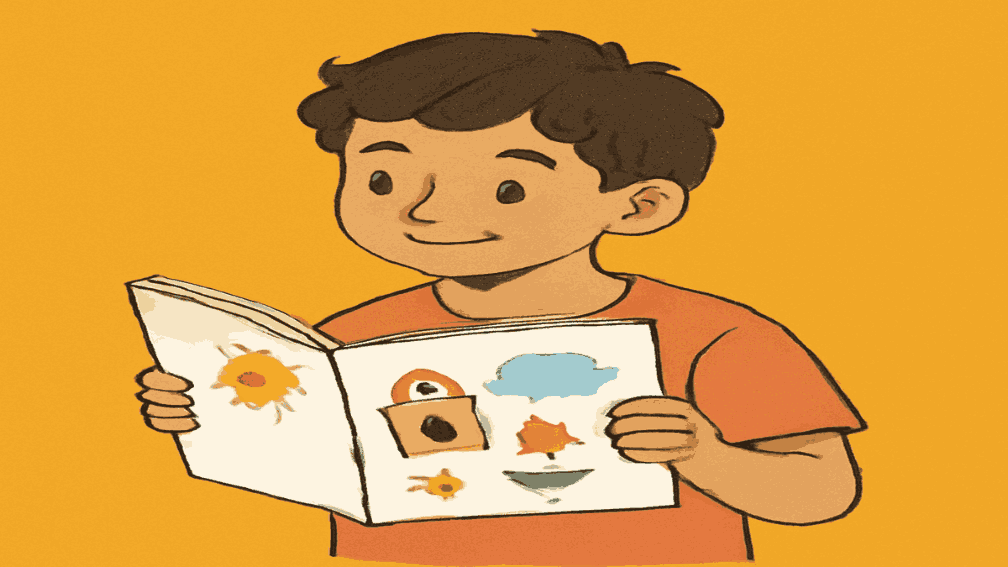
- April 25, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
तख़्ती
बच्चे कोरे कागज़ नहीं
आलोक कुमार मिश्रा
शिक्षाविदों ने ऐसी मान्यताओं को तार्किक आधार पर सिरे से ख़ारिज किया है जो बच्चों को महज कोरा कागज़ समझती हैं या फिर गीली मिट्टी, जिस पर शिक्षकों, अभिभावकों और बड़ों के द्वारा जो भी लिखा जाएगा वही अंकित होगा। वह जैसे ढाले जाएँगे, उसी तरह ढल जाएँगे। इसमें स्वयं उनके प्रयासों, अवलोकनों, अंतर्निहित क्षमताओं या सहज रूप से उपलब्ध परिवेश की भूमिका गौण ही रहेगी। किंतु आज भी कमो-बेश हमारी संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था में यही समझ प्रभावी बनी हुई है। गुरु और शिष्य के संबंधों की पंरपरागत व रूमानी व्याख्याएँ लोगों के दिलो-दिमाग़ से लेकर व्यवहार तक में हावी हैं। ‘गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ि-गढ़ि काढ़े खोट’ की कहावत विद्यालयों में शिक्षकों और बच्चों के आपसी संबंध का मानक बनी हुई है।
पर बच्चे अक्सर इस प्रचलित समझ के परे अपनी स्मृद्ध उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वे अपनी गतिविधियों, बातचीत और सहज मेधा से यह सिद्ध करते रहते हैं कि उन्हें महज़ कोरे कागज़ समझा जाना ग़लत है। वे अपने सामाजिक-साँस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप अनुभवों और समझ से लैस होते हैं। औपचारिक रूप से सीखना वे बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं करते। पैदा होने के बाद और स्कूलों में प्रवेश पाने तक के बीच वे भाषा, शारीरिक कौशलों एवं संस्कृति के सरल सूत्रों को कुछ हद तक आत्मसात् कर चुके होते हैं। वास्तव में आगे के औपचारिक व सुनियोजित अधिगम को ग्राह्य करने और उसके साथ अंतःक्रिया करने में ये विशिष्टताएं बहुत काम की होती हैं। इनको आधार बनाकर सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर और आसान बनाया जा सकता है। पर स्कूलों में स्कूल के बाहर सीखे गये अनुभव या ज्ञान को तरजीह देने की संस्कृति अभी भी बहुत कमज़ोर है। उनके अपने अनुभवों को पूर्वनिर्धारित पाठ्यचर्या में जगह मिलना या उन्हें साथ लेकर चलना मुश्किल से ही दिखायी देता है। फिर भी, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे अपने शिक्षण कार्य के दौरान ऐसे अनुभव प्राप्त होते रहे हैं।
एक बार मुझे अपनी छठी की कक्षा में’असमानता और भेदभाव’ की संकल्पना को बच्चों के स्तरानुरूप बनाने के लिए उपयुक्त उदाहरण ढूँढना मुश्किल पड़ रहा था। पाठ में जातीय, धार्मिक, लैंगिक या आर्थिक आधार पर होने वाले भेदभावों का उदाहरण दिया है। पर मैं शुरूआत स्वयं बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली परिस्थितियों के वर्णन से करना चाहता था। बात करने पर इसमें मेरी मदद कक्षा के विद्यार्थियों ने ही की। उनमें से किसी ने बताया कि ‘हम बच्चे जब दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं और यदि कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बाद वहाँ कुछ खरीदने आ जाये तो अक्सर दुकानदार हमें सामान न देकर पहले उन्हें देते हैं। उनकी नज़र में हम बच्चों के समय की कोई क़ीमत नहीं होती। यह उम्र के आधार पर होने वाला भेदभाव ही तो है।’
इस अनुभव आधारित उदाहरण ने कक्षा में भेदभाव की संकल्पना को खोलने में शुरूआती आधार का काम बख़ूबी किया। बच्चों का अपना अनुभव जब किताबी ज्ञान से जुड़ता है तभी वह जीवंत बनता है।
बच्चों को बच्चा तो समझा जाना चाहिए पर बच्चे का मतलब अनाड़ी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हमें उनको अपने परिवेश की जीवंत सामाजिक-साँस्कृतिक इकाई मानकर आगे बढ़ना होगा। एक ऐसी इकाई जो अपने अवलोकन, अवसरों के दोहन, ग़लतियों और प्रयासों से निरंतर सीखती है।
विद्यालय में सीखने की यह प्रक्रिया समता, स्वतंत्रता से पूर्ण वातावरण में संपन्न की जानी चाहिए। बच्चों की भाषा, संस्कृति, उनमें व्याप्त विविधता, उनकी गरिमा सभी का सम्मान करते हुए आलोचनात्मक चेतना से लैस शिक्षा देने का प्रयास होना चाहिए। आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों से लैस इकाइयां ही न्याय और बंधुत्व पर आधारित सामाजिक समष्टि का निर्माण करेंगी जो कि अभी तक विषमता, वर्चस्व और अन्याय पर टिकी हुई दिखायी देती हैं।

आलोक कुमार मिश्रा
पेशे से शिक्षक। कविता, कहानी और समसामयिक मुद्दों पर लेखन। शिक्षा और उसकी दुनिया में विशेष रुचि। अब तक चार पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जिनमें एक बाल कविता संग्रह, एक शैक्षिक मुद्दों से जुड़ी कविताओं का संग्रह, एक शैक्षिक लेखों का संग्रह और एक कहानी संग्रह शामिल है। लेखन के माध्यम से दुनिया में सकारात्मक बदलाव का सपना देखने वाला मनुष्य। शिक्षण जिसका पैशन है और लिखना जिसकी अनंतिम चाह।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

