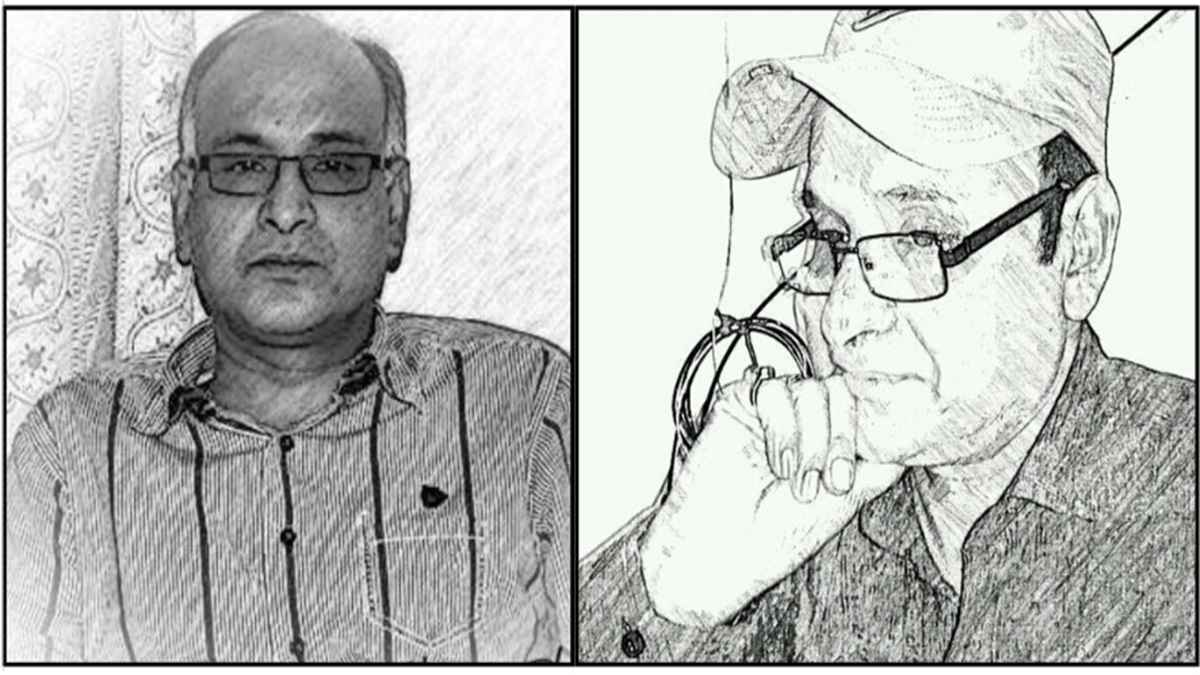
- July 12, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-5
लेखक की कातरता
8 जनवरी, 2014
वर्षों से वागर्थ मेरे लिए सिर्फ़ एक पत्रिका नहीं, बल्कि साहित्य का एक जीवंत दस्तावेज़ रहा है। इसकी लोकप्रियता और समकालीनता का आलम यह है कि हर रचनाकार यहाँ छपने को आतुर रहता है, चाहे संपादक कोई भी हो। मैं भी दो-तीन बार इसकी पंक्तियों में जगह पा चुका हूँ, और यह मेरे लिए लगभग संतोष की बात है। जब से छत्तीसगढ़ के प्रिय कवि एकांत श्रीवास्तव ने वागर्थ की कमान संभाली है, यह पत्रिका पाठकों के दिलों में कुछ अधिक ही उतरने लगी है।
जनवरी 2014 का अंक मेरे सामने है और इसमें दो बातें मेरे मन को गहरे छू गयीं। पहली, एकांत जी का संपादकीय, जिसमें उन्होंने अंर्स्ट फ़िशर को याद करते हुए एक साहसी और सटीक बात कही: “साधारण गद्य-भाषा को सृजनात्मकता ही रचना-भाषा में बदलती है। अभिव्यक्ति की कलात्मकता ही कला का जादू है, जिसके बिना रचना या कला का कोई अर्थ नहीं।” यह कथन कविता की प्रगतिशीलता के उन कथित पैरोकारों के लिए एक करारा जवाब है, जो कलात्मकता को दक्षिणपंथी या बेमानी ठहराते रहे हैं।
प्रगतिशीलता के नाम पर कविता की सौंदर्य-सृष्टि को तार-तार करने वालों ने इस विधा को कितना नुकसान पहुँचाया, यह हम सब जानते हैं। एकांत ने यह बात कहकर एक जोखिम उठाया है, और यह जोखिम सौ टके की सच्चाई है। मुझे उत्सुकता है कि वे कवि, जो बोलचाल की भाषा को ही कविता का पर्याय मान बैठे हैं, इस कथन को किस अर्थ में ग्रहण करेंगे।
दूसरी बात, उपन्यासकार राजी सेठ का ‘तत्सम’ पर लिखा वह मार्मिक आलेख, जो लेखकीय कातरता को एक सच्चे रचनाकार के अनुभव की तरह उजागर करता है। वे लिखती हैं:
“अपनी रचना को लेकर यह कातरता रचनाकार के मन में कितनी गहरी होती है, इसे समझा सकना कठिन है। कितनी अकल्पनीय बातों पर, संवेदना पर कितने छोटे-छोटे आघातों से, कितने अनदेखे अवरोधों पर आत्मविश्वास का संकट आ सकता है और कभी-कभी डिप्रेशन के उन अँधेरों तक ले जाता है, जहाँ से वापसी कभी संभव ही नहीं लगती।”
ये पंक्तियाँ सिर्फ़ शब्द नहीं, एक रचनाकार की आत्मा का आलाप हैं। रचना का संघर्ष केवल कथ्य तक सीमित नहीं; यह अपने आप से, अपने परिवेश से, और यहाँ तक कि अपने पात्रों की हक़ीक़त के लिए लड़ी गयी अनगिनत जंगों का समावेश है। राजी सेठ का यह बयान हर उस लेखक की पुकार है, जो अपनी रचना को जन्म देने के लिए न जाने कितने अंतर्द्वंद्वों से गुज़रता है।
वागर्थ का यह अंक मुझे सोचने पर मजबूर करता है: रचना का जादू सिर्फ़ शब्दों में नहीं, बल्कि उस संवेदना में है, जो उसे जीवंत बनाती है। और यह संवेदना, यह कातरता, रचनाकार को सिर्फ़ लेखक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मानव बनाती है, जो अपने और अपने पात्रों के लिए एक साथ साँस लेता है। एकांत जी और राजी सेठ की ये बातें मेरे मन में देर तक गूँजती रहेंगी, जैसे कोई कविता जो लिखी नहीं, महसूस की जाती है।
जानकारी और सूचनाएँ, जब ज्ञान की जगह घेर लेती हैं तब वे भटकाने लगती हैं।
आसपास
मेरे आसपास बहुत सारे घर हैं। सारे घरों में लोग-बाग भी होंगे, पर मेरे पड़ोसी कहाँ चले गये? पड़ोसियों के आसपास मेरा घर कहाँ चला गया?
सच-सच बताना
9 जनवरी, 2014
सुबह की पहली किरण ने अभी पलकें भी नहीं झपकायी थीं कि पानी, हाँ, वही जीवन का आधार, मेरे सपनों में आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में एक गहरी पुकार थी, जैसे कोई पुराना मित्र दिल की बात कहने चला आये। उसने मुझे झकझोरते हुए कहा, “मानस, सच-सच बता! यह क्या खेल रचाया है? मुझे, जो तुम्हारी नसों में बहता है, जो तुम्हारी धरती को सींचता है, उसे भी क्यों बाज़ार की मंडी में बेच-ख़रीद रहा है?”
उसके शब्द मेरे मन में किसी नदी की तरह गूँजे, जो किनारों से टकराकर सवाल उछाल रही हो। पानी की वह पुकार, वह कातर स्वर, मेरे भीतर कहीं गहरे उतर गया। मैं चुप रहा क्योंकि जवाब मेरे पास नहीं था।
कवि की सामाजिक स्वीकृति
10 जनवरी, 2014
किसी कवि को बड़े से बड़ा बता देना बहुत सरल है किन्तु उसकी घटती सामाजिक स्वीकृति को रोक पाना सबसे कठिन। और इसे पत्रिका, संपादक, संगठन, झंडाबरदार, समीक्षक, पाठ्यक्रम तथा आलोचक मिलकर भी क़तई नहीं- मात्र कवि और उसकी कविता ही रोक सकती है।
जंगल की शब्द-संपदा
आज सुबह मन में एक आत्मीय उमंग लिये ‘युद्धरत आम आदमी’ के पन्ने पलट रहा था, और जैसे ही रमणिका गुप्ता जी का नाम ज़ेह्न में आया, मेरे सामने तीन चीज़ें साकार हो उठीं- रमणिका फाउंडेशन की दिल्ली वाली गर्मजोशी, युद्धरत आम आदमी की बेबाक आवाज़ और आदिवासी साहित्य की वह पृथक संकल्पना, जो हिंदी को ज़मीन से जोड़े रखती है। रमणिका जी का नाम हिंदी-संसार में सिर्फ़ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक विचार का पर्याय है, जो हाशिये की आवाज़ों को मंच देता है।
युद्धरत आम आदमी को पढ़ते हुए हर बार लगता है, जैसे हिंदी की गोद में उसकी आँचलिक बोलियों के नये रंग बिखर रहे हों। इस बार भी कुछ अनजाने शब्द मेरे मन को भा गये- गोठ, पाको (महुआ का फल), डोरी, सुतान टांडी, पटवाह, पट खून, थरिया, सेवा-सुसार, धँगरिन, पंची, छापा कुर्ता। ये शब्द सिर्फ़ शब्द नहीं, गाँव की मिट्टी की सौंधी महक हैं, जो हिंदी को और समृद्ध करते हैं। ख़ासकर ‘गोठ’ ने तो मेरा दिल जीत लिया। छत्तीसगढ़ी में भी ‘बात’ को ‘गोठ’ कहते हैं और इस ‘गोठ’ में वह आत्मीय रस है, वह सौंदर्य है, जो शहरी ‘बात’ में कहाँ!
जब गाँव में चौपाल पर ‘गोठ’ होती है, तो उसमें ज़िंदगी की गहराई, हँसी-मज़ाक और अपनापन समा जाता है। ‘बात’ में वह ठहराव कहाँ? ‘गोठ’ जैसे कोई पुराना दोस्त हो, जो बिना लाग-लपेट के दिल की बात कह जाता है। युद्धरत आम आदमी ऐसी ही ‘गोठ’ को हिंदी में पिरो रही है और रमणिका जी का यह प्रयास मुझे हर बार अभिभूत करता है।
रमणिका फाउंडेशन हो या उनकी पत्रिका, दोनों ही हिंदी को उसकी जड़ों से जोड़े रखने का ज़िम्मा बख़ूबी निभा रहे हैं। आदिवासी साहित्य को एक अलग पहचान देना, उनकी बोली और संस्कृति को सहेजना- यह कोई साधारण काम नहीं। आज युद्धरत आम आदमी के पन्नों में खोया, तो लगा जैसे मैं किसी गाँव की चौपाल पर बैठा हूँ, जहाँ ‘गोठ’ चल रही है, और हर शब्द में ज़िंदगी की धड़कन सुनायी दे रही है।
क्रमश:
(पूर्वपाठ के अंतर्गत यहां डायरी अंशों को सिलसिलेवार ढंग से सप्ताह में दो दिन हर शनिवार एवं मंगलवार प्रकाशित किया जा रहा है। इस डायरी की पांडुलिपि लगभग तैयार है और यह जल्द ही पुस्तकाकार प्रकाशित होने जा रही है। पूर्वपाठ का मंतव्य यह है कि प्रकाशन से पहले लेखक एवं पाठकों के बीच संवाद स्थापित हो।)

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

