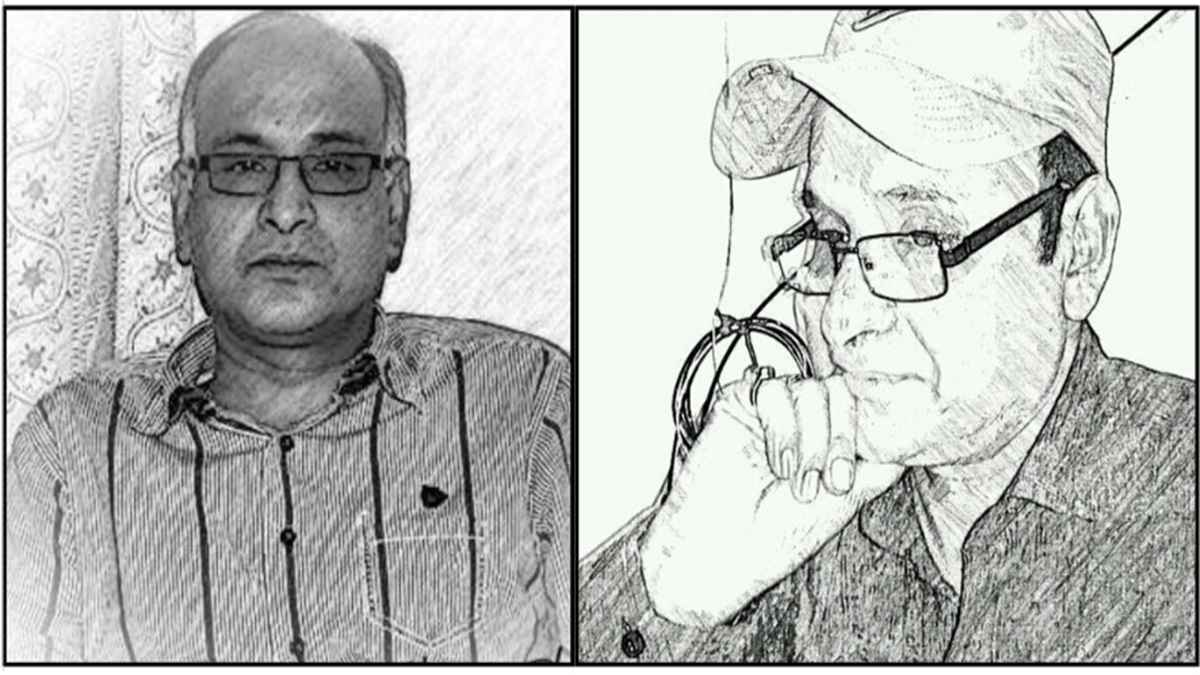
- July 26, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-9
कवि की दुनिया
6 फरवरी, 2014
कुछ कवियों के लिए कविता ही उनकी दुनिया है और कुछ कवियों के लिए दुनिया ही उनकी कविता।
एक ग़लती = दो छड़ी
हमारे बचपन के सबसे पहले गुरुजी थे रामचंचल ओझा। वह खजूर की छड़ियाँ रखते थे- खजूर की, बाँस की- पिटाई के लिए। एक ग़लती पर खजूर की दो छड़ियां। चार ग़लती पर स्कूल से निकाल देते थे। हमने एक बार ग़लती की थी- दोष शब्द में तालव्य श लिख दिया। उस पर हमको दो छड़ी लगीं।”- बाबा नागार्जुन
एक कली दो पत्तियाँ
पिछले माह सप्ताह भर श्रीलंका रहा। श्रीलंका की धरती पर क़दम रखते ही जैसे समय ठहर-सा गया। हवा में चाय की पत्तियों की वह ख़ुशबू, जो नाक से उतरकर सीधे आत्मा को छूती है। सात दिन, सात रातें, और हर पल भूपेन हज़ारिका की वह गूँज- “एक कली, दो पत्तियाँ, नाज़ुक-नाज़ुक उंगलियाँ…”। यह गीत नहीं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र था, जो हरे-भरे बाग़ान के बीच, अनजान भाषाओं के पार, मेरे भीतर गूँजता रहा। रतनपुर यहाँ नहीं था, पर क्या फ़र्क़ पड़ता है? चाय के बाग़ान तो वही हैं- हरियाली का वह अनंत विस्तार, जहाँ श्रम और सौंदर्य एक-दूसरे में गूंथे हुए हैं।
सुबह की पहली किरण में, जब कोहरा अभी पत्तियों पर ओस की तरह टिका था, मैंने देखा— वे नाज़ुक उँगलियाँ। अनाम चेहरों की वे औरतें, जिनके हाथों में चाय की पत्तियाँ नहीं, समय की नाज़ुक रेखाएँ थीं। एक कली, दो पत्तियाँ- यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं, यह एक तपस्या है। उनकी आँखों में वही दर्द, जो भूपेन की आवाज़ में था। वही दर्द, जो शायद हर उस मेहनत में बसता है, जो अनदेखी रह जाती है। उनकी भाषा मेरी नहीं थी, पर उनकी चुप्पी मेरी थी। उनकी थकान मेरी थी।
शाम ढलते-ढलते, जब सूरज बाग़ान के पीछे छिपने को होता, मैं सोचता— यह सौंदर्य क्या है? यह जो पत्तियों का हरा, उंगलियों का नृत्य, और श्रम का मौन गीत एक साथ रचता है, क्या यह कविता नहीं? क्या यह वह नहीं, जो जीवन को उसकी सबसे नाज़ुक, सबसे गहरी सतह पर छूता है? श्रम का सौंदर्य वह है, जो अपनी अनश्वरता में अनाम रहता है। वह पत्ती है, जो चाय के प्याले तक पहुँचकर भी अपनी कहानी भूल जाती है।
रात को, जब तारे श्रीलंका के आकाश में टिमटिमाते, मैं अपने कमरे में बैठा उस गीत को फिर सुनता। “तोड़ रही है कौन वो रतनपुर बाग़ीचे में…”। रतनपुर नहीं, श्रीलंका। पर बाग़ीचा वही। दर्द वही। और वह सौंदर्य भी वही, जो श्रम की हर साँस में बसता है।
वर्ना शराबी होता या आवारा!
“पत्नी के त्याग और तपस्या ने मुझे लेखक बनाया। यदि मैंने विवाह नहीं किया होता तो मैं लाख प्रतिभासंपन्न होने पर भी एक शराबी और आवारा आदमी होता। मेरे स्वभाव और चरित्र में आवारा आदमी बनने की सारी संभावनाएं हैं। अपनी जन्मकुंडली के अनुसार भी मैं संन्यासी या गुंडा होते बाल-बाल बचा हूँ। विवाह के पश्चात मैंने जो लिखा है, उसमें केवल शब्द ही मेरे हैं और शेष सभी कुछ मेरी पत्नी का है।”- नरेश मेहता (कमलकिशोर गोयनका से वार्तालाप में)
7 फरवरी, 2014
दुख
दुख नदी-जल है: उसका बह जाना ही धर्म है, रोकेंगे तो कभी न कभी बांध टूटेगा ही और तबाही आएगी ही।
कहीं बौर कहीं फल
हमारे देश में अभी बौर आ रहे हैं पर श्रीलंका में आम कबके फल चुके।
दोनों हाथ
स्त्री प्रार्थना में दोनों हाथ अपने लिए नहीं, औरों के लिए जोड़ती है।
8 फरवरी, 2014
फ़ेसबुक के कुछ पर्यायवाची शब्द
ईशबुक ऐशबुक केसबुक कैशबुक क्लेशबुक मेषबुक भेषबुक प्रेसबुक प्लेसबुक फ्लैशबुक फ्रेशबुक भैंसबुक तैशबुक देशबुक द्वैषबुक ठेसबुक रेसबुक येसबुक शेषबुक बाक़ी आप बताएं?
साथ
शब्द अँधेरे में भी अकेले नहीं, अपनी भावना, कल्पना, स्मृति और संघर्ष के उजियालों के साथ होते हैं।
क़द
पितृपुरुषों की मूर्तियों का क़द बढ़ाने से देश और जनता का क़द नहीं बढ़ता।
मैं सबसे सुखी हूँ
क्योंकि मुझे दुख के बारे में नहीं पता। वह सबसे दुखी है क्योंकि उसे सुख के बारे में कुछ भी अता-पता नहीं। सुख और दुख मूलत: तुलनात्मक और संदर्भजनित अवधारणाएँ मात्र हैं और कुछ भी नहीं।
सुख और दुख, ये दो शब्द जैसे ज़िंदगी की सारी उलझन को अपने में समेटे हुए, पर कितने फिसलन भरे, कितने धोखे के। जो कहता है वह सबसे सुखी है, क्या वह सचमुच सुखी है? या दुख की ठंडी साये ने उसे अभी नहीं छुआ? और जो दुखी है, क्या इसलिए कि सुख उसकी चौखट पर कभी ठिठका नहीं? ये सुख और दुख, जैसे एक ही चादर के दो किनारे, पर चादर तुलना की, संदर्भ की। एक के बिना दूसरा क्या है?
मैं सोचता हूँ प्रेमचंद की उस कफ़न के घीसू और माधव के बारे में, जो अपनी ज़िंदगी की त्रासदी में हँसते हैं, ठठरी पीते हैं, तब भी जब माधव की बीवी बुधिया मर चुकी है। क्या वे सुखी थे, उस एक रात, जब उनके पास कफ़न के पैसे थे और पेट भर खाना? या दुखी थे, क्योंकि सुख का मतलब उनके लिए बस वही एक रात था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं?
आज सुबह मैंने एक भिखारी को देखा, लाल बत्ती पर, हाथ फैलाये, चेहरा धूल और धूप से सना। वह हँस रहा था, शायद किसी बच्चे की मुस्कान ने उसे सिक्के से ज़्यादा दे दिया। क्या वह सुखी था, उस एक पल में? या दुख को इतना जी चुका कि हँसी उसका आख़िरी सहारा थी?
सड़क के उस पार, चमचमाती गाड़ी में एक शख़्स। चेहरा तना हुआ, आँखें फ़ोन में गड़ीं, शायद किसी टूटी डील का गुस्सा, शायद किसी और की कामयाबी का काँटा। वह दुखी है, क्योंकि सुख उसके लिए वह है जो उसकी हथेली से फिसल गया। घीसू-माधव का सुख था एक रात की ठठरी, इस शख्स का सुख शायद और बड़ा बंगला, और चमकीली गाड़ी। तुलना। संदर्भ। सुख-दुख कुछ नहीं, बस हमारे मन के बनाये फंदे। जो इन दोनों को छूकर, घीसू की तरह हँसते हुए, या माधव की तरह उदास, आगे बढ़ जाये, वही मुक्त है। बाक़ी सब, मैं और तुम, इन दो शब्दों के बीच झूलते रहते हैं।
9 फरवरी, 2014
अवश्यंभावी
विचार के मर्तबान को बीच-बीच में कड़ी धूप में नहीं रखने से विचार के सड़ने का ख़तरा बढ़ जाता है।
सुबह 5:30 बजे: आज सुबह नींद और मच्छरदानी से बाहर निकलकर सीधे खिड़की से सटे सोफ़े पर जा बैठा। आसमान में हल्के बादल थे, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। मन में एक विचार कौंधने लगा- जैसे मर्तबान में रखा अचार बिना धूप के नमी से सड़ने लगता है, वैसे ही विचारों को भी समय-समय पर ताज़गी चाहिए। चाय की चुस्की लेते हुए सोचा, आज अपने दिमाग़ को कुछ नया सोचने का मौक़ा दूँगा। किताबों की अलमारी से एक पुरानी कविता की किताब निकाली और कुछ पंक्तियाँ पढ़ने लगा। विचारों का मर्तबान हिल गया, हल्की धूप-सी लगने लगी।
दोपहर 11:00 बजे: ऑफ़िस में काम का बोझ था, लेकिन बीच-बीच में दिमाग़ को बंद कमरे की नमी से बचाने के लिए बाहर टहलने निकला। पार्क में पेड़ों की छाँव में बैठकर एक नयी कहानी का ख़ाका बनाया। लगा कि विचारों को धूप मिल रही है- न ज़्यादा तीखी, न बिल्कुल ठंडी। एक सहकर्मी से नयी तकनीक पर चर्चा की, कुछ ताज़ा नज़रिये मिले। सोचा, अगर रोज़ एक ही ढर्रे पर चलता रहा, तो विचार सड़ जाएँगे।
शाम 4:30 बजे: घर लौटते वक़्त बाज़ार से गुज़रा। एक मर्तबान में रखे नींबू के अचार को देखकर मुस्कुरा दिया। दुकानदार ने कहा, “इसे हर हफ़्ते धूप दिखानी पड़ती है, वरना ख़राब हो जाता है।” मन में वही बात गूँजी। घर पहुँचकर डायरी खोली और दिन भर के विचारों को लिखा- कुछ कच्चे, कुछ पके। लगा कि इन्हें कागज़ पर उतारकर मैंने इन्हें सड़ने से बचा लिया।
रात 9:30 बजे: दिन के अंत में खाना खाते हुए एक पुरानी फ़िल्म देखी। उसमें एक किरदार कहता है, “जो सोचते हो, उसे बोल दो, वरना दिमाग़ में दबकर गंदगी हो जाती है।” सोचा, कितना सही है। आज जो सोचा, उसे लिखा, कुछ दोस्तों से साझा किया। विचारों को हवा मिली, धूप मिली। अब सोने से पहले मन हल्का है- न कोई नमी, न कोई सड़न।
असली कारण
वह पिछले दिनों जंगल से निकलकर शहर तक पहुँचा था। अब पता चला- हाल ही वह बाज़ार की ओर जा रहा था, सुनते हैं तबसे ग़ायब है।
10 फरवरी, 2014
उत्तरपाड़ा : एक तीर्थस्थल
कोलकाता जाने की बात मन में उठी, तो एक जगह बार-बार याद आयी- उत्तरपाड़ा, जोयकृष्ण पब्लिक लाइब्रेरी। जैसे कोई तीर्थ हो, कोई पुरानी किताब का पन्ना, जो पलटने पर धूल और यादों की ख़ुशबू देता है। मैं सोचता हूँ, वहाँ जाऊँगा। उन किताबों को छूऊँगा, जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। किताबें, जिनमें शब्दों के साथ-साथ वक़्त की साँसें बसी हैं। किताबें, जो शायद जोयकृष्ण मुखर्जी के सपने की तरह खुली थीं- एक ऐसा समाज, जो पढ़ता हो, सोचता हो, अपने को जानता हो।
1856 में बनी यह लाइब्रेरी, कहते हैं, एशिया की पहली पब्लिक लाइब्रेरी थी। जोयकृष्ण जी ने इसे बनवाया, 85 हजार रुपये लगाये, जैसे कोई मंदिर बनवाता है। मैं सोचता हूँ, उस ज़माने में 85 हजार रुपये कितने बड़े सपने के बराबर होंगे? 60 हज़ार किताबें थीं तब, 17वीं से 19वीं सदी की। हर किताब जैसे एक दुनिया, हर पन्ना जैसे किसी अनजान की डायरी। मैं वहाँ खड़ा होऊँगा, सोचूँगा- ये किताबें किसने पढ़ी होंगी? कितने लोग यहाँ आये, कितने सपने यहाँ से ले गये?
कहते हैं, माइकेल मधुसूदन दत्त बीमार थे, तो जोयकृष्ण जी ने उन्हें यहीं रखा, उनकी देखभाल की। मैं सोचता हूँ, ये लाइब्रेरी सिर्फ़ किताबों की जगह नहीं थी। यहाँ इंसानियत भी थी, दोस्ती थी। और उस मैदान में, जहाँ महर्षि अरविंद ने भाषण दिया था, वहाँ खड़ा होकर मैं क्या सुनूँगा? शायद हवा में अभी भी उनके शब्द तैरते हों, जैसे पुरानी किताबों की स्याही की महक।
1998 से यह लाइब्रेरी बंगाल सरकार के अधीन है। पर मेरे लिए यह कोई इमारत नहीं, यह एक तीर्थ है। मैं वहाँ जाऊँगा, किताबों के बीच खड़ा होऊँगा। शायद अपने अतीत को छू लूँ, शायद अपने को थोड़ा और जान लूँ। जैसे कोई बच्चा अपनी पुरानी स्लेट उठाता है, और उस पर लिखे अधूरे अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करता है।
क्रमश:

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

