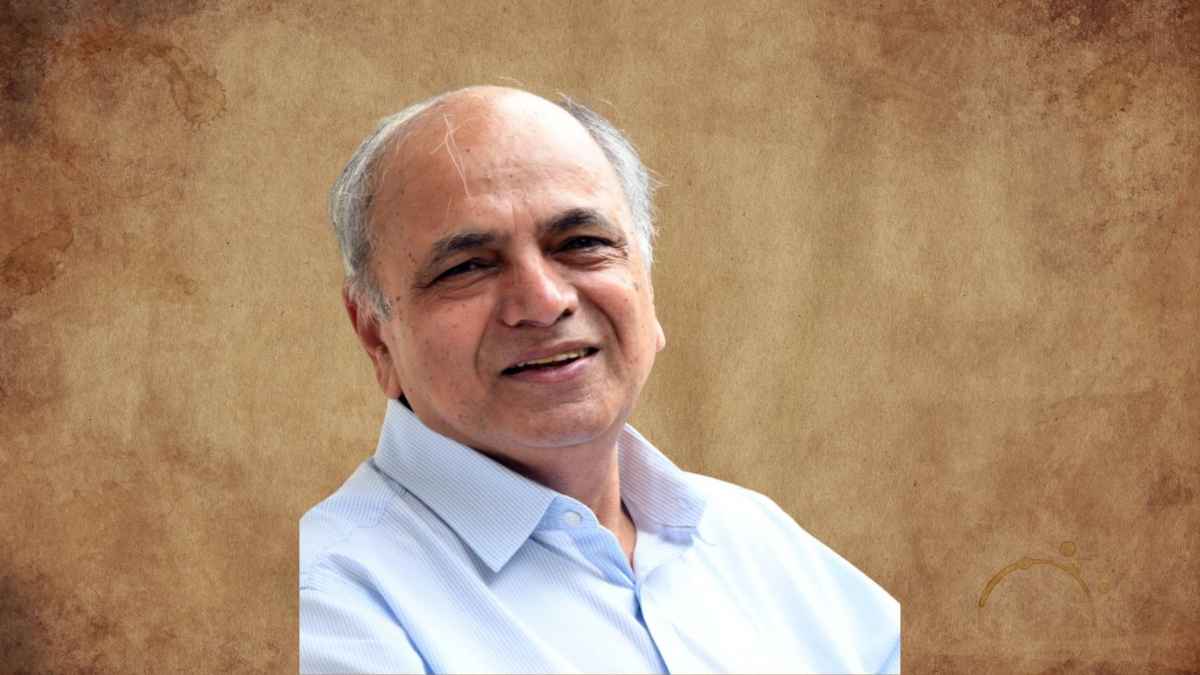
- May 15, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
भाषा : राजनीति, लोक और एआई युग के मुद्दे
भारत के पीपल्स लिंंग्विस्टिक सर्वे के माध्यम से 780 भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण करने वाले गणेश नारायणदास देवी सांस्कृतिक कार्यकर्ता, साहित्य आलोचक एवं अंग्रेज़ी के पूर्व प्राध्यापक हैं। जी.एन. देवी आदिवासी अकादमी के साथ ही भाषा रिसर्च एवं प्रकाशन केंद्र के संस्थापक हैं। 75 वर्षीय भाषाविद देवी से कामिनी मथाई ने जो बातचीत की, उसमें पूरे भारत में एक भाषा के प्रश्न के साथ ही भाषाओं के वैश्विक बदलाव के परिदृश्य को भी विचारा। हिंदी के पाठकों के लिए बातचीत के अंश संडे टाइम्स से साभार। (अनुवाद: भवेश दिलशाद)
- त्रि-भाषा नीति को लेकर कुछ राज्यों में एक हिचक और प्रतिरोध देखा गया, एक भाषाविद होने के नाते इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है?
मानक नीति के लिहाज़ से यह अच्छी बात है। हालांकि भारत के सभी भाषाई समूहों में इसे थोपना जायज़ नहीं है क्योंकि इससे होता यह है कि अपने भाषा परिवार से बाहर की भाषा सीखने के लिए भी लोगों को बाध्य होना पड़ता है। चूंकि हिंदी हिंद-आर्याई परिवार की भाषा है इसलिए पंजाबियों के लिए यह सीखना आसान होगी लेकिन कन्नड़ या तमिल जैसी भाषा बोलने वाले द्रविड़ भाषा परिवार के लोग इसमें कठिनाई ही महसूस करेंगे। अपने इतने लंबे इतिहास में पूरे भारत में कभी भी किसी एक भाषा का एकछत्र विस्तार नहीं रहा।
भारत हमेशा बहुभाषीय राष्ट्र रहा है और यह जो भारतीयता है, इसी बहुभाषीय चरित्र में ही अवस्थित है।
- ऐसा कैसे हुआ कि हिंदी को ‘एकीकृ’ भाषा के रूप में देखा जाने लगा?
चूंकि हिंदी पट्टी का बहुत बड़ा इलाक़ा ब्रितानी हुक़ूमत के अंतर्गत आता था इसलिए हिंदी औपनिवेशक शासकों का चयन थी। तो व्यवहार में 19वीं सदी तक हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभर आयी। आज़ादी के बाद, संविधान सभा ने यह फ़ैसला किया कि राष्ट्रभाषा के तौर पर कोई एक भाषा नहीं रहेगी बल्कि 15 सालों के लिए हिंदी या अंग्रेज़ी को राज्यों के बीच संवाद की भाषा के रूप में बरता जाएगा। उम्मीद तो यही थी कि हिंदी जल्द ही अंग्रेज़ी का स्थान ले लेगी लेकिन प्रशासनिक और क़ानूनी उपयोग की प्रचुर शब्दावली के अभाव में ऐसा हो नहीं सका। बल्कि, वास्तविकता तो यह है कि संचार की भाषा के रूप में कोई भी भारतीय भाषा अंग्रेज़ी की जगह नहीं ले सकती।
- हिंदीभाषियों की संख्या बढ़ने के आंकड़ों पर आप संदेह जताते हैं, असहमत होते हैं, क्यों?
क्योंकि उम्मीद यही रही कि हिंदी अन्य भाषाओं का स्थान लेगी इसलिए केंद्र सरकार के लिए यह ज़रूरी हो गया कि हिंदी की लगातार बेहतरी को दर्शाया जाये। 2011 जनगणना के दौरान, भारतीयों ने अपनी मातृभाषा के रूप में 19,569 नाम गिनवाये थे। इनमें से 17 हज़ार को तो सीधे ही ख़ारिज कर दिया गया। शेष में से 1474 भाषाओं में पर्याप्त विद्वता का अभाव देखा गया इसलिए उन्हें महत्व नहीं दिया गया। केवल 1369 यानी 6 प्रतिशत भाषाएं बचीं, जिन्हें 121 लेबलों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। और इन्हीं को देश भर में इस तरह बताया गया कि देश में इतनी भाषाएं हैं। इन्हीं में से 22 भाषाओं को संविधान में अधिसूचित भाषाओं में रखा गया है।
- मातृभाषाओं को ख़ारिज करने का काम क्या वैज्ञानिक आधारों से किया गया?
जनगणना की संरचना दरअसल, बहिष्कार के सिद्धांत को अपनाती है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहें तो यह नागरिकों पर अनैच्छिक वाचाघात थोपने की तरह है। तर्क यह है कि अगर किसी भाषा को मान्यता दी जाना है तो करोड़ों की आबादी वाले देश में उसके बोलने वालों की संख्या न्यूनतम 10 हज़ार तो हो। किसी भी वैज्ञानिक धरातल पर यह तर्क उचित नहीं है लेकिन यही चलन चला आ रहा है। भाषाई सर्वे के दौरान अधिकतर ऐसी भाषाओं से मेरा साक्षात्कार हुआ जिनका कोई लिखित स्वरूप है ही नहीं, केवल वाचिक परंपरा ही है। महाराष्ट्र में गोंधाली समुदाय की भाषा को उदाहरण के तौर पर लें तो एक व्यक्ति हवा में हाथ घुमा-घुमा कर वाक्यों को संप्रेषित करता है और दूसरा समझता है। यह अदृश्य लिपि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है।
अब आप ग़ौर से देखें तो पाएंगे कि जनगणना के आंकड़ों के बाद जो वर्गीकरण किया गया है, वह ज़्यादातर बलात् है तार्किक नहीं।
- इससे हिंदी के ‘उन्नयन’ में मदद कैसे हुई?
1971 में, भारत के 54 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ को हिंदीभाषी के तौर पर सूचीबद्ध किया गया। 2011 तक, यह आंकड़ा 52 करोड़ हो गया। प्रतिशत में देखें तो हिंदीभाषी 36.9 से 43.6 प्रतिशत हो गये। लगभग 50 अन्य भाषाभाषियों को जोड़कर हिंदी का डेटा मज़बूत किया गया। इसमें भोजपुरी शामिल है जो 5 करोड़ लोगों की मातृभाषा है और इसका अपना सिनेमा, थिएटर और साहित्य है। इसी तरह राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार की भाषाएं भी जोड़ी गयी हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र की पावरी भाषा तक हिंदी समूह में समाहित कर दी गयी है। जबकि पावरीभाषी न तो हिंदी ठीक से समझते हैं और न ही हिंदीभाषी पावरी। अगर हिंदी में जोड़ दी गयी भाषाओं को हटाया जाये तो जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वे लोग सिर्फ़ 32 प्रतिशत रह जाएंगे। और अगर 70% लोग हिंदीभाषी नहीं हैं तो, ऐसे में हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बस राजभाषा है।
- एआई के युग में भाषा का भविष्य?
दुनिया की तमाम प्राकृतिक भाषाओं में 75 प्रतिशत या तो पतन की ओर हैं या विलुप्त होने के क़रीब। सांस्कृतिक ऐक्य के विचार को बढ़ावा देने, ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से यह नुक़सान बहुत तेज़ी से हो रहा है। 8000 साल पहले बिल्कुल इसी तरह के हालात तब थे जब शिकारी क़बीले कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं की तरफ़ शिफ़्ट हुए थे। यह संकट एआई के कारण और घनीभूत तो हुआ है। भाषाविद और न्यूरोलॉजिस्ट यह चेतावनी दे रहे हैं कि इससे स्मृति घटेगी और व्याकरणिक संरचनाएं लुप्त होती जाएंगी।
- भारतीय भाषााओं के बारे में क्या कहेंगे?
दुनिया की हर आठवीं भाषा का घर भारत है। अंडमान में अंतिम बोभाषी और सिक्किम में अंतिम माझीभाषी की मृत्यु के साथ ही ये दो भाषाएं मर गयीं। अनेक तटीय और घुमंतू समुदायों की भाषाएं ख़त्म हो चुकी हैं और आदिवासियों की अनेक भाषाएं धुंधला रही हैं। यही नहीं, शब्दों का ख़ज़ाना भी लुटता जा रहा है। लोग अब सीमित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, रूपक और कहावतें लगभग खो गयी हैं। मसलन, बंगाल में अंग्रेज़ी शब्दों के भारी मिश्रण वाली भाषा अब सामान्य बात है। शुद्ध बांग्ला में पूरा वाक्य बोलना अब दुर्लभ हो गया है। अब जैसे उड़िया है, कई भाषाएं डिजिटल दुनिया में पिछड़ रही हैं तो ये धीरे धीरे बहुत पीछे छूट जाएंगी। मराठी, तेलुगु या बांग्ला की तुलना में तमिल की स्थिति बेहतर है लेकिन स्कूली बच्चों में पढ़ने का कौशल कमतर होता जा रहा है। अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों के कारण मातृभाषा की कविताओं, कहानियों से बच्चे दूर हो रहे हैं। नतीजतन, बच्चों को अब भाषा नहीं बल्कि कथाओं की विरासत मिल रही है।
- कोई भाषा मर रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है?
जब मनुष्य बोलने के स्थान पर चित्र आधारित संचार या संवाद की तरफ़ बढ़ रहा है, तो भाषाओं का पतन हो रहा है, विशेषकर बच्चों के संदर्भ में। दुनिया भर में यह ज्ञान की प्रकृति और सीमाओं के शिफ़्ट का युग है, ऐसे में पुरस्कार देने या संस्थान बनाने से आगे व्यवस्था को चाहिए कि भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषा नीति पर निर्णायक ढंग से कोई सार्थक उपाय खोजा जाये।

कामिनी मथाई
पत्रकारिता में 25 साल का अनुभव। 'एआर रहमान: द म्यूज़िकल स्टॉर्म' किताब की लेखक कामिनी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिज़नेस के साथ ही उन मुद्दों पर लेखन पसंद करती हैं, जो हमारे बदलते परिवेश से जुड़े हैं। वह जीवनीकार भी हैं और मनोविज्ञान का अकादमिक अध्ययन भी कर रही हैं।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

