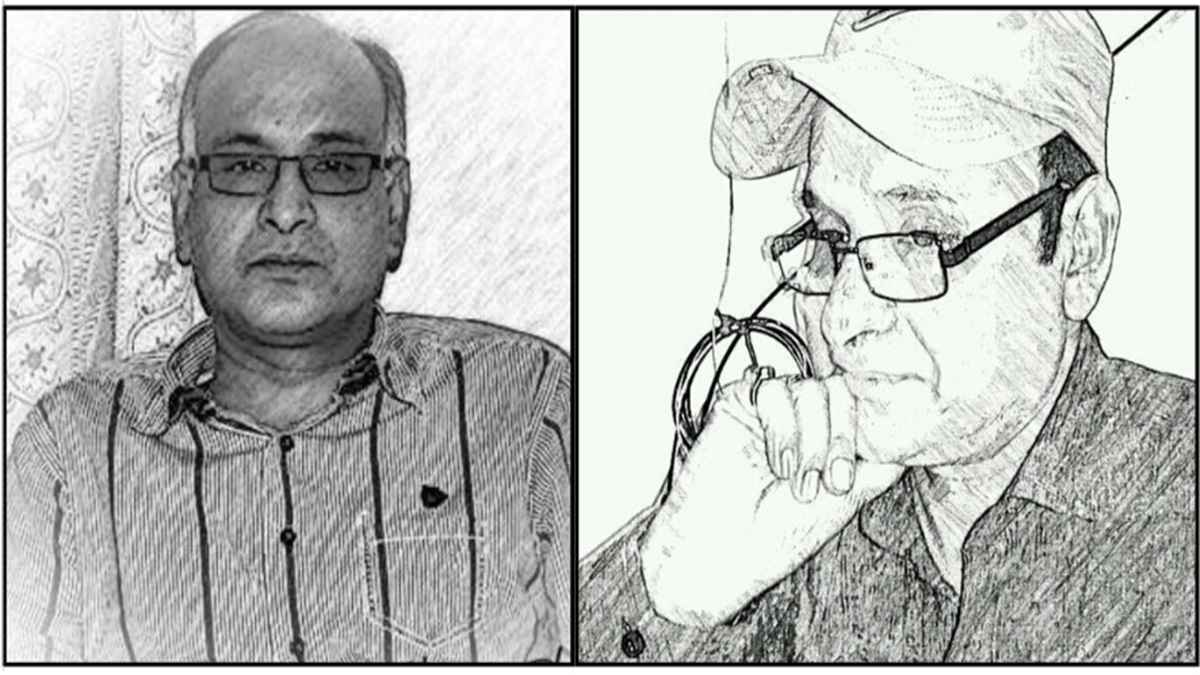
- August 2, 2025
- आब-ओ-हवा
- 1
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-11
समुद्र का भी कोई न कोई प्रवेश-द्वार
29 मार्च, 2014
मैं नहीं, मेरा मन समुद्र के किनारे टहल रहा था, जहाँ लहरें रेत को चूमकर लौट रही थीं। मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था: समुद्र का प्रवेश-द्वार क्या है? क्या यह वह नदी है जो अपनी यात्रा समुद्र में समाप्त करती है? नदियाँ, जैसे गंगा या अमेज़न, अपने साथ मिट्टी, खनिज और जीवन लाती हैं, जो समुद्र की गहराइयों में एक नया संसार रचते हैं। समुद्र का प्रवेश-द्वार शायद वह डेल्टा है, जहाँ मीठा और खारा पानी एक-दूसरे से मिलते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देते हैं। या फिर, यह द्वार वह गहरी समुद्री धारा है, जैसे गल्फ़ स्ट्रीम, जो गर्मी और पोषक तत्वों को विश्व के कोनों तक ले जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से, समुद्र का द्वार कोई एक स्थान नहीं, बल्कि अनगिनत प्रक्रियाओं का संगम है- एक अनवरत चक्र, जो पृथ्वी के जीवन को संचालित करता है।
समुद्र का प्रवेश-द्वार क्या केवल भौतिक है? या यह जीवन का एक प्रतीक है? हर गंतव्य, हर सत्य, हर अनुभव का एक द्वार होता है। लाओत्सु ने कहा था, “हज़ार मील की यात्रा एक क़दम से शुरू होती है।” शायद समुद्र का द्वार वह पहला क़दम है- वह साहस, वह जिज्ञासा, जो हमें अज्ञात की ओर ले जाती है। मैंने रूमी के शब्दों को याद किया: “द्वार के पार एक और संसार है।” क्या समुद्र का द्वार वह क्षण है जब हम अपने डर को त्यागकर अनंत की ओर क़दम बढ़ाते हैं? यह विचार मुझे बेचैन करता है, क्योंकि यह सुझाता है कि हर समुद्र, हर चुनौती, हर गहराई का एक द्वार होता है- बस उसे खोजने की ज़रूरत है।
शाम ढलते ही मैंने समुद्र के द्वार को शब्दों में बांधने की कोशिश की। विश्व के कवियों की आवाज़ मेरे कानों में गूँज रही थी। रवींद्रनाथ टैगोर ने समुद्र को “अनंत का गीत” कहा था, और उनकी कविता ‘गगन के तट पर’ में वह समुद्र के किनारे खड़े होकर अनंत से संवाद करते हैं। क्या उनका समुद्र का तट ही वह प्रवेश-द्वार था? फिर मैंने पाब्लो नेरूदा की ओर रुख़ किया, जिन्होंने अपनी कविता ‘समुद्र’ में लिखा: “मुझे तुम्हारी गहराई चाहिए, तुम्हारी लहरों का गान।” नेरूदा का समुद्र एक प्रेमी है, जिसका द्वार हृदय में खुलता है। और फिर, विलियम वर्ड्सवर्थ की पंक्तियाँ, जो प्रकृति को एक आध्यात्मिक द्वार मानते थे: “प्रकृति का हर रूप मुझे अनंत की ओर ले जाता है।” मैंने लिखा:
समुद्र का द्वार कोई ठोस फाटक नहीं
यह लहरों की साँस है, जो किनारे को चूमती है
यह वह क्षण है जब चाँद और सूरज एक-दूसरे को देखते हैं
और ज्वार अपने गीत में अनंत को बुलाता है।
रात को, जब मैं अपनी खिड़की से उस समुद्र को याद करते-करते, देख रहा था, मेरे मन में एक चित्र उभरने लगा- एक विशाल द्वार, जो पानी से बना है। यह द्वार न तो स्थिर था, न ही स्पष्ट। यह लहरों के साथ नाचता था, कभी खुलता, कभी बंद होता। इसके पीछे सितारों से भरा आकाश था, और हर लहर जो उस द्वार को पार करती थी, एक नई कहानी लेकर आती थी। यह बिम्ब मुझे कालिदास की ‘मेघदूत’ की याद दिलाता है, जहाँ बादल एक संदेशवाहक बनकर पहाड़ों और नदियों को पार करता है। क्या समुद्र का द्वार भी ऐसा ही है- एक गतिशील, तरल मार्ग, जो हमें विश्व की कहानियों से जोड़ता है?
टैगोर ने कहा था, “हर सीमा के पार एक अनंत प्रतीक्षा कर रहा है।” शायद समुद्र का द्वार वह सीमा है, और उसे पार करना ही जीवन का सत्य है। नेरूदा की तरह, मैं भी समुद्र की गहराई में उतरना चाहता हूँ, और वर्ड्सवर्थ की तरह, उसकी लहरों में अनंत को सुनना चाहता हूँ।
आज, समुद्र का प्रवेश-द्वार मेरे लिए एक विचार बन गया है- वैज्ञानिक रूप से एक चक्र, दार्शनिक रूप से एक सत्य, काव्यात्मक रूप से एक गीत, और बिम्बात्मक रूप से एक स्वप्न। यह द्वार हर जगह है, और कहीं नहीं। यह मेरे भीतर है, और मेरे बाहर भी। जैसे रूमी ने कहा, “तुम समुद्र की एक बूँद नहीं, तुम बूँद में सारा समुद्र हो।” शायद, मुझे द्वार की खोज नहीं करनी, बल्कि उसे अपने भीतर खोलना है।
सोने से पहले मैं अपनी डायरी में यह भी टाँक लेता हूँ: “समुद्र का भी कोई न कोई प्रवेश-द्वार होता है। नाव कहीं से भी नहीं उतार दी जाती। नाविक उसे भली-भांति चिन्हता है।” कल फिर समुद्र से मिलूँगा। शायद वह मुझे एक नया द्वार दिखाये।
एक विचित्र प्रार्थना
हमारे स्कूलों में रोज़ प्रार्थना के समय यह गीत दोहराया जाता है- “हे प्रभु! आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए…” मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि हम ‘आनंददाता’ से जीवन में आनंद के बजाय ज्ञान ही माँगने पर क्यों तुले हुए हैं।
31 मार्च, 2014
कलाकार की जागरूकता
मुझे मेरे अधिकतर मित्र पूछा करते हैं: “आप फ़ेसबुक पर औरों की ही अधिक चर्चा करते हैं? मैं हँसकर बात टाल जाता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी कभी इल्म न इसका। क्यों ज़रूरी यह सब मेरे लिए! पल भर लगता- शायद फ़ितरत यही हो और तबीयत भी मेरी। मन ही मन मुझे अपने बुजुर्गों की बात याद आने लगती है- सिर्फ़ अपने को ही मत देखो। शायद इसीलिए ही हो और इसी लय में मुक्तिबोध की वह अनमोल कथन भी, जिसे बहुत पहले कभी पढ़ा था मैंने:
“अपने से परे जाने, अपने से ऊपर उठने, अपने को दूसरों से मिलाने और और उसमें डूब जाने का यह कार्य अधिक सावधानी से, ज़्यादा गहराई से और अधिक बार होना चाहिए। कलाकार की जागरूकता का अर्थ ही यह है। अपने से परे जाना, अपने से ऊपर उठना, वृथा भावुकता नहीं है, वरन् इसके विपरीत, वस्तु-दर्शन या तत्त्व-दर्शन का वह अनिवार्य अंग है। ज्ञान का जो मनोवैज्ञानिक गुण है, वही इसका गुण भी है।” (कलात्मक अनुभव, नये साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, गजानन माधव मुक्तिबोध)
तुझे कुछ भूलता-सा जा रहा हूँ
चाहे कोई कुझ भी कहे: सर्वोच्च दर्शन तो यही कहता है- प्रेम, प्रेम के लिए ही होना चाहिए। प्रिय मात्र एकाग्रता का माध्यम है तथा जैसे-जैसे प्रेम पूर्णता की ओर बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे प्रिय का विचार शिथिल होकर समाप्त हो जाता है। तब बच रहता है विशुद्ध प्रेम । अर्थात् स्थूलता सूक्ष्मता में तब्दील हो उठती है। प्रेम का उत्कृष्ट भला और क्या है! फ़िराक़ गोरखपुरी भी किस अंदाज़ से हमें कह गये हैं:
मुहब्बत अब मुहब्बत हो चली है
तुझे कुछ भूलता-सा जा रहा हूँ
आप कहाँ हैं रमेश दत्त दुबे जी!
आज 31 मार्च है न- मेरे लिए एक बहुत यादगार दिन। मेरे प्रिय कवि और लोकमर्मज्ञ रमेश दत्त दुबे जी का जन्म दिन। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ. दुबे ने सागर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एमए किया था। सन् 1966 में अपनी कविता ‘असगुनिया’ से साहित्य जगत में चर्चा में आये। कवि एवं आलोचक डॉ. अशोक वाजपेयी से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। बचपन के लंगोटिया। उनका उपन्यास ‘टोला’ काफ़ी चर्चित रहा। कविता, बुंदेली ‘कहनात’ के अलावा उनके और भी कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला ‘शिवकुमार श्रीवास्तव सम्मान’ उन्हें दिया गया था। कविता की समझ विकसित कराने में वे मेरे अत्यंत प्रिय कवियों में रहे।
जब भी रायपुर आते, बड़े भैया चंद्रशेखर व्यास जी के बाद मुझे ज़रूर ख़बर करते। चंद्रशेखर जी न होते तो मैं उनसे जुड़ ही न पाता। उनसे मुझे जो भी सीखने का मौक़ा मिला, उसमें दुबे जी के साथ चंद्रशेखर जी का कम योगदान नहीं है।
दुबे जी और मैंने- हम दोनों ने मिलकर 20वीं सदी की हिंदी कविता में पक्षियों को लेकर एक संकलन भी तैयार किया- विहंग। जो पहले वैभव प्रकाशन के सुधीर शर्मा ने छापा और द्वितीय संस्करण बोधि प्रकाशन के भाई मायामृग ने। दिसंबर 2013 से उनकी अनुपस्थिति मुझे रह-रहकर साल रही है। वे नहीं हैं पर मेरे पास उनका आशीष है। धरोहर भी।
मेरे आग्रह पर उन्होंने टालते-टालते लिख ही दी थी मेरे दूसरे कविता संग्रह ‘होना ही चाहिए आँगन’ की भूमिका। हमारे समय में तो पुस्तक से भूमिका और मनुष्य से आश्चर्य दोनों विलुप्ति के कगार पर हैं। वह आश्चर्य ही तो है जिसके चलते प्रकृति के नानावर्णी रूप उद्घटित हुए हैं। इसी आश्चर्य के सहारे कलाएं अपने अर्थ और अभिप्रेतों के लिए प्रति-प्रकृति की संरचना करती रही हैं। पुस्तक की भूमिका- पुस्तक का आश्चर्य है, जयप्रकाश से वर्षों पूर्व रायपुर में एक संक्षिप्त सी मुलाक़ात हुई थी, उन्होंने मेरा लिखा-पढ़ा भी अधिक नहीं है- हांलाकि वह अधिक है भी नहीं- फिर मुझसे भूमिका लिखवाने का क्या कारण हो सकता है। सोचता हूँ तो पाता हूँ कि आदिम लोकराग को सुनना-तलाशना; हम दोनों को एक ही भावभूमि पर प्रतिष्ठित करता है।
1 अप्रैल, 2014
आलोचना कोई अनाथालय नहीं है
परगोद बैठू यानी पैठू आलोचकों को शर्मसार करने के लिए प्रो. गणेश पाण्डेय जी से मेरा कभी साक्षात् नहीं हुआ, न कभी चलितवार्ता पर कोई बात। बावजूद इसके वे मेरे पठनीय रचनाकार हैं। उनकी धार-धार, बेलाग आलोचना मुझे समय-सापेक्ष और अपरिहार्य लगती रही है। ऐसी मारकता और सच्चाई इधर कम आलोचकों के पास है। यह एक आकर्षण तो स्वाभाविक था, सो मुझे उनके संपादन में निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका ‘यात्रा’ में एकाध बार छपकर छपने जैसा ही लगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएँ भी हमारे दौर में हैं: जहाँ छपना, छपना जैसा नहीं होता। जैसे बहुत बार लिखना, लिखने जैसा नहीं होता।
बहरहाल यात्रा के 7वें अंक पर सीधे जा पहुँचें तो लगेगा कि यह अंक (यही क्यों, हरेक अंक) अपने संपादकीय से बौद्धिक उष्मा की चाहत रखने वालों को जैसे एक आत्मीय आमंत्रण देता है– बस्स, चाव से पढ़ते रहने का। आज की कविता और आलोचना पर संपादक ईमानदार और गंभीर पड़ताल से सहमति जताने के लिए बाध्य कर देता है। ख़ासकर जिस धाराप्रवाह और बतकही भाषा में वे अपने तर्कों और साहित्यिक सच्चाई को रखते हैं, वह भाषा के नाम पर जलेबी परोसने वालों कवियों, लेखकों और विशेषतः नौसीखिए और परगोदबैठू यानी पैठू आलोचकों को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त है। पर समझें तब ना! वह भी सूत्र शैली में। प्रो. पाण्डेय की ऐसे कुछ सूत्रात्मक अनुभव और दिशाबोध:
- अधिकांश आलोचक आलोचना की भाषा के नाम पर बेस्वाद और हलवाई भाई से भी अधिक पेंचदार जलेबियाँ बनाने के लिए मशहूर रहे हैं।
- बनना चाहते हैं आलोचक और पैर हैं नन्हे-नन्हे, करें क्या, बस पाजामा या जींस या प्लास्टिक का पाइप जो भी मिल जाये लंबा-सा, तुरत अपना पैर उसमें डाल देते हैं।
- आलोचना न तो शोधप्रबंध की भाषा है, न प्राध्यापक की भाषा है।
- आलोचना कोई अनाथालय नहीं है। आलोचना किसी कमज़ोर की लुगाई नहीं है। आलोचना कोई लावारिस लाश नहीं है। आलोचना कोई छुईमुई जैसी चीज़ नहीं है कि कोई भी पट्ठा आँख दिखाएगा और डर जाएगी।
- लेखक होने की पहली शर्त है किसी स्वाभिमानी लेखक का अपमान न करना या उसके विरुद्ध षडयंत्र में शामिल न होना।
- क्या साहित्य मार्क्सवाद के भीतर है या मार्क्सवाद साहित्य के भीतर?
- कतरनबाजी और कबूतरबाजी आलोचना का धर्म नहीं है।
- सिर्फ़ विचारधारात्मक लेखन आलोचना नहीं है।
- आज की कविता कम से कम पाठकों और श्रोताओं के पास नहीं है। उनके बीच है जो कविता या आलोचना लिखते हैं।
- लेखक हमेशा अपनी रचना से ज़िंदा रहता है, इतिहास से नहीं।
- कमज़ोर आलोचक, लेखक ही नहीं, संस्थाओं की भी चाकरी करते हैं।
- यह ज़रूरी नहीं कि कथा संपादक की कविता संबंधी समझ अच्छी हो।
- देश का बड़े से बड़ा संपादक कवि का महत्व उसको मिले पुरस्कार से आँकने की नासमझी करता है।
निर्माता
रास्ता किसी देवता के हाथों से नहीं, साधारण इन्सान के पैरों से ही बनता है।

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky


विचार कैसे उमड़ते – घुमड़ते और मथते हैं हमें इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को इस डायरी में महसूस किया जा सकता है।