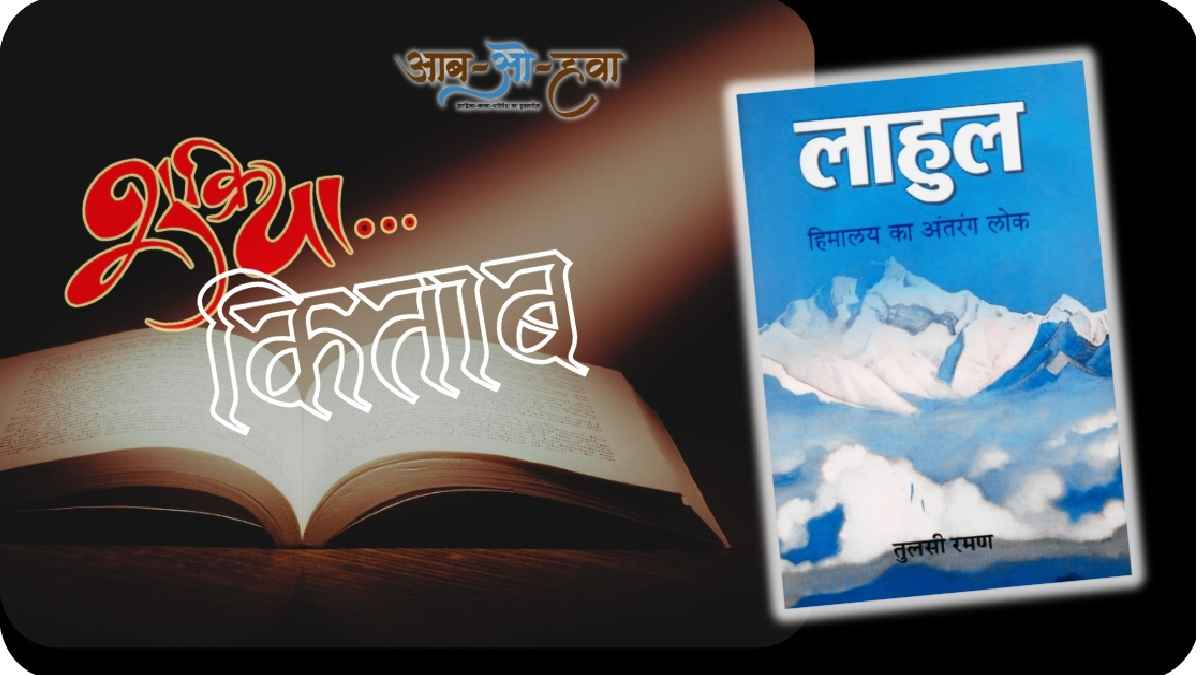
- August 25, 2025
- आब-ओ-हवा
- 3
(विधाओं, विषयों व भाषाओं की सीमा से परे.. मानवता के संसार की अनमोल किताब -धरोहर- को हस्तांतरित करने की पहल। जीवन को नये अर्थ, नयी दिशा, नयी सोच देने वाली किताबों के लिए कृतज्ञता का एक भाव। इस सिलसिले में लगातार साथी जुड़ रहे हैं। साप्ताहिक पेशकश के रूप में हर सोमवार आब-ओ-हवा पर अमूल्य पुस्तक का साथ यानी 'शुक्रिया किताब'.. इस बार तुलसी रमण की बहुचर्चित पुस्तक का विस्तृत पाठ -संपादक)
शशि खरे की कलम से....
लाहुल: दुर्गम घाटी, दूरस्थ लोक से रिश्ता बनवाती किताब
आज जब, लोगों की कविता, कहानी, उपन्यास कुछ भी पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती, ऐसे समय में, हिमाचल प्रदेश की लाहुल घाटी पर एक यात्रा वृत्तांत जैसी रोचक, संस्मरण जैसी विमुग्ध करने वाली, रिपोर्ताज जैसी आमूल-चूल जानकारी देने वाली, आदि से अंत तक बाँधकर रखने में समर्थ यह पुस्तक पढ़ना बहुत ही सुखद है। सबसे आकर्षक है लोकरंग का समावेश और बर्फीली हवाओं से जूझती उद्दाम जिजीविषा। लाहुल की संस्कृति को आत्मसात किये बिना ‘लाहुल’ लिखना संभव नहीं है।
पुस्तक में चन्द्रभागा नदी स्वयं लेखक की लेखनी में स्याही का रूप धरकर लाहुल के साक्षात दर्शन करवा रही है। कभी इतिहास के मैदान से गुज़रती है, कभी बौद्ध और हिन्दू परम्पराओं से, कभी वहाँ की लोककथाओं से, कभी पुरातत्व और कला सम्पदा की घाटियों में घुमाती है और कभी लोकमतों और क़िस्सों के सीप, शंख और मोती बाँटती जाती है।
लेखक तुलसी रमण ने लाहुल के बारे में विषय-सीमाओं को इतना विस्तार दिया है कि भूगोल, इतिहास, पुरातत्व, आर्थिक स्थिति, कृषि, कला संस्कृति, धर्म, भाषाएँ, यहाँ तक कि लोक शब्दों की व्युत्पत्ति भी बतलायी है। जीवन्त व सम्प्रेषणीय चित्रण अपनी व्याख्यात्मक और सहज सरल शैली के कारण बारंबार पढ़ने को विवश करता है।

डॉ. तुलसी रमण हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग की साहित्यिक पत्रिका ‘विपाशा’ के 28 वर्षों तक संपादक रहे एवं हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा अकादमी के सचिव पद पर कार्य करते हुए अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का संपादन भी किया।
हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, लाहुल एक ऐसी घाटी है, जो बर्फबारी के कारण नवंबर से अप्रैल तक लगभग छह माह शेष दुनिया से कटी रहती है। यह स्पीति हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों की एक विलक्षण घाटी है।
पुस्तक के ग्यारह अध्याय
भौगोलिक परिवेश, इतिहास के संदर्भ, देशभाषा, जाति और समाज, लोक देवता और लोक विश्वास, हिन्दू और बौद्ध परम्परा का समवाय, पुरातत्व और कला सम्पदा, लाहुल का नया चेहरा जैसे उपशीर्षकों से ग्यारह अध्याय हैं। प्राक्कथन श्री किशोरीलाल वैद्य ने लिखा है। भूमिका में श्री तुलसी रमण लिखते हैं- “1990 में लाहुल की पहली यात्रा की तो चंद्रभागा की घाटियों में प्रकृति और संस्कृति के कई रहस्य खुलते गये। संस्कृति का निर्माण केवल मनुष्य के माध्यम से नहीं होता, बल्कि मनुष्येतर पहाड़, बर्फ, जल, वायु, जंगल, सूर्य, चन्द्र, वनस्पति व प्राणी जगत की इसमें विशेष भूमिका रहती है। इन्हीं के साहचर्य में मनुष्य के भीतर की मानवीय प्रकृति स्पंदित होती है। बड़े जीवट वाले लाहुली लोगों ने इस कठोर भूगोल और जलवायु के साथ जीवन जीने के लिए आश्चर्यजनक संगति कायम की है। लाहुल की एक पुरानी कहावत है- सेम दुग म-ने तोंग संग सेम यड, लू तोड ब-गा… अर्थात दुखी होकर ईश्वर का मंत्र पढ़ने से अच्छा है, खुश होकर गीत गाना।
लाहुल का कोई लिखित इतिहास नहीं है। लोकवार्ता में ही कुछ तथ्य मिल पाते हैं। पहली यात्रा में ही घाटी के शीर्ष लोकदेवता राजा गेपंंग की मिथक कथा सुनने को मिली और गेपंंग के प्रति लाहुली लोगों की समग्र आस्था भी देखी। जिस समाज के पास ऐसी मिथक कथाएँ हों उसे किसी राजा के इतिहास की ज़रूरत नहीं। ये मिथक ही आदिम मनुष्य की भाषा और जीवन्त कौमों के दस्तावेज़ रहे हैं।”
पुस्तक का प्रारंभ होता है भौगोलिक परिवेश के सम्यक दर्शन से। मनाली में हिड़मा देवी का मंदिर है, जो महाभारत की हिडिम्बा है। कई क़िस्सों की चर्चा है। प्रसंगवश निर्मल वर्मा की डायरी के चुनिंदा अंश हैं। रोहतांग में बेहद ठंडी और हिंस्र हवाएं इस दर्रे पर जान भी ले लेती हैं। रो-शव, थड-मैदान, रोथड-रोहतांग – शव का मैदान। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से बाद तक आये यात्रियों के अनुभव तब और अब के विभिन्न अंतरों को स्पष्ट करते हैं।
एक लोककथा का ज़िक्र इस प्रकार है- ग्यलपो गेसर नामक राजा के पास उड़ने वाला घोड़ा और जादुई कोड़ा था। उसने अपना कोड़ा फटकारकर सामने की ढलान का मार्ग खोल दिया। दुबारा कोड़ा फटकारने के पहले ही देवी गुरमन ने रोक दिया-आवाजाही का मार्ग सुगम मत बनाओ।
देखा जाये तो इन सदियों पुरानी लोककथाओं में चेतावनी के संदेश छुपे हुए हैं-प्रकृति से छेड़छाड़ सीमा में रहकर करो। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन में हुई तबाही ऐसा ही दुष्परिणाम है।
ऋषि वशिष्ठ पुत्र शोक में पाशबद्ध होकर आर्जिकिया नदी में कूद गये थे। नदी ने उनको पाशमुक्त किया इसलिए ‘विपाशा’ कहलायी, जो अब व्यास है।
1964 में दो जीपें टुकड़ों , पुर्जों में , खच्चरों पर सवार होकर मनाली से लाहुल पहुँची थीं। उसके बाद वहाँ जोड़कर इसे तैयार किया गया, भीतरी रास्तों पर चलने के लिए।
आगे क्षेत्रफल, जनसंख्या, समुद्र तल से ऊँचाई, सीमा से सटे प्रदेश या ज़िले, ऋतुचक्र, वर्षा आदि संपूर्ण जानकारी बारीक़ी से दी गयी है। साथ के श्वेत श्याम चित्र उत्सुकता बढ़ाते हैं, जिज्ञासा शांत करते हैं।
चंद्रभागा लाहुल की सबसे विस्तृत उपजाऊ घाटी है। केन्द्रीय पर्वत क्षेत्र में लाहुल के प्रख्यात और पूज्य गेपंग पर्वत शिखर हैं। यहाँ से बड़े ग्लेशियर नीचे घाटियों में उतरते रहते हैं।
इतिहास के संदर्भ में
रमण जी इतने वरिष्ठ और समर्थ साहित्यकार हैं कि किसी भी विषय को उठा लें, भाषा तो उनके कथ्य के पीछे नदी सी प्रवहमान रहती है। उनकी शैली, जैसे सामने बैठे श्रोता से बातचीत कर रहे हों, यह उन्हें अलग पहचान देती है।
लाहुल एक संगठित राज्य कभी नहीं हो पाया। सभी क्षेत्रों और समुदायों का साँझा लोक देवता गेपंग सर्वमान्य राजा मान लिया गया। लाहुल की पुरानी बोलियाँ, पुरा सम्पदा का अध्ययन, लोक कथाएँ, घुरे (गीत) प्रथाएँ, लोकाचार यहाँ का इतिहास जानने में सहायक हैं। दो हज़ार साल पहले भारत-तिब्बती लोग यहाँ बस गये थे। गाँवों में कौरव लोकदेवता हैं। कुछ खानदानों में पाँडव। मध्य तिब्बत से आकर बसने वालों से पहले, पूरा पश्चिमी तिब्बत मोन और दर्द जातियों के अधिकार में था। बहुत परिश्रम से पुस्तक की सामग्री को खोज-परखकर रखा गया है। मूल निवासियों, नयी जातियों के आगमन, बसने और बिखरने के ब्यौरेवार वर्णन हैं। लेखक के अनुसार 635ई. में हुएनसांग कुल्लू में था उसके द्वारा लाहुल का पहला लिखित संदर्भ मिलता है।
परवर्ती इतिहास में भी बारीक़ी से युद्ध, संधि, जुर्माना और लूट, सिखों का हमला, अँग्रेज़ों का बँटवारा व शासन से आज के लाहुल स्पीति जिले के प्रमुख भूखण्ड के रूप में लाहुल की लंबी यात्रा का वर्णन है। देश,भाषा, जाति समाज में लाहुल शब्द के अर्थ से जुड़ी बातें, व्युत्पत्ति और इतिहास है।
लेखक का यह मत उल्लेखनीय है- “लाहुल के लिए पढ़े-लिखे विद्वान सबसे ज्यादा ल्हा-युल यानी देवभूमि का अर्थ निकालते रहे हैं। दरअसल भावविह्वल होकर शोध करने या लिखने वालों की कमी नहीं है और उन्हें मनुष्य कम, सब तरफ़ देवी-देवता ही दिखायी देते हैं। वे मानव जीवन के संघर्ष का इतिहास नहीं जानना चाहते बल्कि देवी-देवताओं की लीलाओं के काल्पनिक मुकुट बुनते हैं। इस बात को परोक्ष में छोड़ते हुए कि आख़िर ये देवता भी मनुष्य ने ही तैयार किये हैं। अपने भय और भावुकता के रहते ही मानव ने देवता और राक्षस कल्पित किये हैं। इस देश में देव-भूमि कहाँ नहीं कही गयी है! इस हिसाब से तो सब जगह देवभूमि ही है, मानव भूमि कहीं नहीं दिखायी देगी।”
भीषण प्रकृति से जूझने वाले लाहुल के लोगों का संघर्ष भी एक मिसाल है। डॉ. ग्रियर्सन ग्राहम बेली, छेरिंग दोरजे आदि ने लाहुली बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया है, जिसका पर्याप्त विवरण दिया गया है।
यहाँ की बोलियों ने बहुत लंबे समय तक अपनी अलग पहचान बना रखी है। सात प्रमुख-पट्टनी, तोद, तिननी, चिनाली आदि का विस्तृत अध्ययन इस पुस्तक में है। जाति और समाज का शोधपरक समाजशास्त्रीय अध्ययन बहुत रोचक भी है।
लोक देवता और लोक विश्वास
अध्याय में वहाँ के हिन्दू, बौद्ध और आदिम समाज के धर्म, उनकी जनश्रुतियां, आचार- विचार, देवी देवता, राक्षस, त्यौहार और उत्सवों का दिग्दर्शन है। लाहुल स्पीति की वे अनसुनी लोककथाएं जो अभी तक घाटी से बाहर नहीं आ पायी थीं, वे अत्यंत रोचक कथाएँ विस्तार से लिखी गयी हैं।
“पूरे लाहुल के देवता गेपंग का सिसू में एक छोटा सा मंदिर है। उसमें भी कोई मूर्ति नहीं है। पुराने समय में युद्ध में गेपंग ल्हा के झंडे को ऊँचा उठाये लोग लड़ाई में भाग लेते थे। गुरु घंटाल का उल्लेख भी है, जो इसी क्षेत्र के हैं एक देव रूप में। केलंग सद का उपाख्यान विस्तार से है और एक नयी दिशा में सोचने की शक्ति देता है। केलंग सद, जवान स्वस्थ और सुंदर व्यक्ति की बलि मांगता था। अन्ततः लोगों ने उसके काष्ठ स्तंभ को काटकर बहा दिया। अन्याय का विरोध अवश्य करना चाहिए।”
ऐसे अनेक क़िस्से विस्तार से हैं। मूलिंग गाँव की लेभे अपा यानी दादी लेभे भी राक्षसी थी लोगों ने उसे भी सुधारकर देवी बनाया। देवी तिल्लो के ‘भय’ से उकताकर उसे भी चन्द्रभागा में बहा दिया। लेखक की क़िस्सागोई शैली के कारण, विस्तार होने पर भी पुस्तक में प्रवाहमयता बनी हुई है।
लाहुल में भी वृक्ष और पर्वत पूजन की रीति है। वहाँ के आदिम धर्म में जीवात्मवाद के तत्व भी पाये जाते हैं। प्रकृति की विकराल घटनाओं में किसी सर्वशक्तिमान का आभास हुआ।लेखक ने आगे बहुत काव्यात्मक रूप में मानव मन पर प्रकृति के प्रभाव का वर्णन किया है। इस जीवात्मवाद के तत्व सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋचाओं के रचयिता वहीं कहीं हिमालय की तराई में बसते थे इसीलिए लाहुल में इस विचारधारा का व्यापक प्रभाव है शमनवाद के आयाम भी हैं.. संहारक शक्तियों, प्रकोप, कुदृष्टि आदि से बचने के लिए इनका शमन करना आवश्यक है। कभी नरबलि भी होती थी, अब पशुबलि का चलन है। लाहुल में जौ का सत्तू और ‘छंग’ देव को चढ़ाया जाता है।
तीरंदाज़ी की प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय है। द (तीर) छंग (गेहूँ सेबना पेय) दछंग.. उत्सव कई दिनों तक चलता है। तीरंदाज़ी का खेल विभिन्न उत्सवों में होता है। किताब में लाहुलवासी हिन्दू, बौद्ध और जनजातीय लोगों के आचार-विचार, मंदिर, लोकोत्सवों का परिचय बहुत बारीक़ी से है।
त्रिलोकीनाथ मंदिर का पुजारी बौद्ध लामा है। मृकुला देवी के मंदिर में एक ही प्रतिमा को हिन्दू महिषासुरमर्दिनी के रूप में और बौद्ध तांत्रिक देवी वज्र वराही-दोरजे फगमो मानकर पूजा करते हैं।
पुरातत्व और कला सम्पदा
इस अध्याय के अन्तर्गत मठ, मंदिर, छोरतेन, और मने, थंका और चित्रकला, मुखौटे, पुरासम्पदा के बहुत महीन विवरण को किंवदंतियों के उल्लेख तथा श्वेत-श्याम चित्रों ने अविस्मरणीय बनाया है।
यहाँ का लोकसाहित्य इस घाटी के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के वर्णन के साथ ऐतिहासिक महत्व का भी है। इसमें समाजशास्त्र, नृतत्वशास्त्र की दृष्टि से भी कई तथ्य सामने आते हैं। गाथागीत जो कि ‘घुरे’ कहलाते हैं, उनमें शिव-पार्वती विवाह बहुत प्रसिद्ध है- ए ईशुरा बीरा बरा माँगूणे लागी/ए जाओ बमूना बरु ए मंगाये..। अर्थात शिव ने नारद से कहा- हे ब्राह्मण जाइए हमारे विवाह के लिए उपयुक्त कन्या ढूँढ लीजिए।
पाँडव अंतिम यात्रा के लिए लाहुल से ही गुज़रे थे, ऐसी मान्यता है। पाँडवों के लोकगीत में प्रचलित बातों से अलग-
ए पांडूडू राजे ए तऊं नौ गाजा माणू ए,
ए नौ गाजा माणू ए तऊं काकाला जूंआ ए।
पाँच पुत्र पांडव कहलाये। पाँच पाँडव राजपाट चलाएँ। पाँडव राज में नौ गज ऊँचे मानव, छिपकलियाँ, उनकी जूँए। गेहूँ का एक दाना सेर भर का। सतयुग में था पाँडव राज।
श्रम और शोषण से जुड़े लोकगीत भी बहुत हैं- विधिसिंह की चाकरी पर तो जाना ही है, फिर जीएँ या मरें… सुगली- किसी के देहांत पर शोक निमग्न स्त्रियाँ मृत्यु गीत सुगली गाती हैं।
यहाँ के जनजातीय क्षेत्र लोककथाओं की दृष्टि से सबसे उर्वर रहे हैं। कहावतों और मुहावरों की भी भरमार है। काठू का रोट और छाछ निगलने दो- यह मुहावरा सुकून और शांति चाहने के अर्थ में लाहुली जीवन को व्यक्त करता है।
लोक और लोकधारा
इस अध्याय में सत्रहवीं सदी से अँग्रेज़ों के समय तक की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण है। आवास, फसलें, दैनिक जीवन, वस्त्र आदि का विस्तृत वर्णन लाहुलवासियों का जीवनवृत्त आँखों के सामने आ जाता है।
वहाँ सभी लोग सामिष होते हैं और हल्के मादक पेय- छंग पीना वर्जित नहीं है। विवाह और मृतक संस्कार अत्यंत विधिपूर्वक होते हैं। छंग, सत्तू, मक्खन, भेड़, शर, शागुण, फर- ये सात चीज़ें हैं जिनके माध्यम से लाहुल के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की विशेष व्याख्या हो सकती है।
लोकधारा में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। पारंपरिक खेती और खानपान बंद हो रहा है। कुल्लू में चाकरी बनाम बेगारी बड़ी दुखदायी समस्या थी, जिसके फैलाव, परिणाम व कारण का गंभीर विवेचन किया गया है। मोरेवियन मिशन का क़िस्सा तो अपने आप में एक बहुत रोचक कहानी जैसा है।
कुठ का रहस्य… यदि किसी को एक बैठक में एक किताब पढ़ने से थकान होती हो तो इस पुस्तक के संदर्भ में कहा जा सकता है कि कुठ का रहस्य पढ़कर चौकन्नापन आ जाता है। मैं स्वयं विचार कर रही हूँ कि पढ़ना छोड़कर कुठ की खेती करने लगूँ। अब तो लाहुल के लोग कुठ, आलू, मटर की खेती करने से प्रगतिशील किसानों में गिने जाते हैं।
जीवन्त व सम्प्रेषणीय शब्द चित्रण अपनी व्याख्यात्मक और सहज सरल शैली के कारण बारंबार पठनीय है। हिमालय की दुर्गम घाटी, जो साल के छह माह बाहरी दुनिया से कटी रहती है, वहाँ की सैर और व्यापक जानकारी यहाँ मिली इसलिए दिल से शुक्रिया किताब ‘लाहुल’ को।
पुस्तक के अन्त में लाहुल का नया चेहरा अध्याय विषय को सम्पूर्णता दे रहा है। लेखक का कथन- अर्थ उपार्जन जीवन का लक्ष्य हो जाये तो राजनीतिक स्वार्थ का संक्रमण भी तेज़ी से होता है। यह बात तो पूरे भारत के लिए है।
परिशिष्ट में लाहुल की सांस्कृतिक शब्दावली रखी गयी है जो बहुत उपयोगी है। लेखक के कविहृदय ने लाहुल घाटी की समृद्ध जीवनशैली को देखकर जो कविताएँ रचीं, उनकी प्रस्तुति पुस्तक का सुंदर उपसंहार है-
लाहुल पुराण
मैंने राजा गेपंग से माँगी
पहनने के लिए भेड़ और
खाने के लिए भेड़
स्वाद के लिए
जौ का सत्तू
और मस्ती के लिए
छंग का गिलास
उसने कहा : तथास्तु!
2-
बर्फ की बिजलियाँ…
हँसती, खनकती, फिर लजाती
हाथों में काँसे की थालियाँ,
गोधूलि के पूर्ण चन्द्र सी,
अतिथियों के सहभोज के लिए..।
(क्या ज़रूरी कि साहित्यकार हों, आप जो भी हैं, बस अगर किसी किताब ने आपको संवारा है तो उसे एक आभार देने का यह मंच आपके ही लिए है। टिप्पणी/समीक्षा/नोट/चिट्ठी.. जब भाषा की सीमा नहीं है तो किताब पर अपने विचार/भाव बयां करने के फ़ॉर्म की भी नहीं है। edit.aabohawa@gmail.com पर लिख भेजिए हमें अपने दिल के क़रीब रही किताब पर अपने महत्वपूर्ण विचार/भाव – संपादक)

शशि खरे
ज्योतिष ने केतु की संगत दी है, जो बेचैन रहता है किसी रहस्य को खोजने में। उसके साथ-साथ मैं भी। केतु के पास मात्र हृदय है जिसकी धड़कनें चार्ज रखने के लिए लिखना पड़ता है। क्या लिखूँ? केतु ढूँढ़ता है तो कहानियाँ बनती हैं, ललित लेख, कभी कविता और डायरी के पन्ने भरते हैं। सपने लिखती हूँ, कौन जाने कभी दुनिया वैसी ही बन जाये जिसके सपने हम सब देखते हैं। यों एक कहानी संकलन प्रकाशित हुआ है। 'रस सिद्धांत परम्परा' पुस्तक एक संपादित शोधग्रंथ है, 'रस' की खोज में ही। बस इतना ही परिचय- "हिल-हिलकर बींधे बयार से कांटे हर पल/नहीं निशाजल, हैं गुलाब पर आंसू छल-छल/झर जाएंगी पुहुप-पंखुरी, गंध उड़ेगी/अजर अमर रह जाएगा जीवन का दलदल।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky


भाई तुलसी रमण की किताब की इतने विस्तार और सशक्त ढंग से समीक्षा लिखी है लाहुल स्फीति की भौगौलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य अपने आप खुलता चला गया।
लेखक और समीक्षक दोनों को बधाई और शुभकामनाएं इस सुन्दर लेखन और महत्त्वपूर्ण जानकारी के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा काॅलम है।
हर बार नयी नयी किताबों का ईमानदार परिचय मिलता है।
लाहुल की चर्चा बहुत दिलचस्प है , पुस्तक पढ़ने की इच्छा हो गई है।