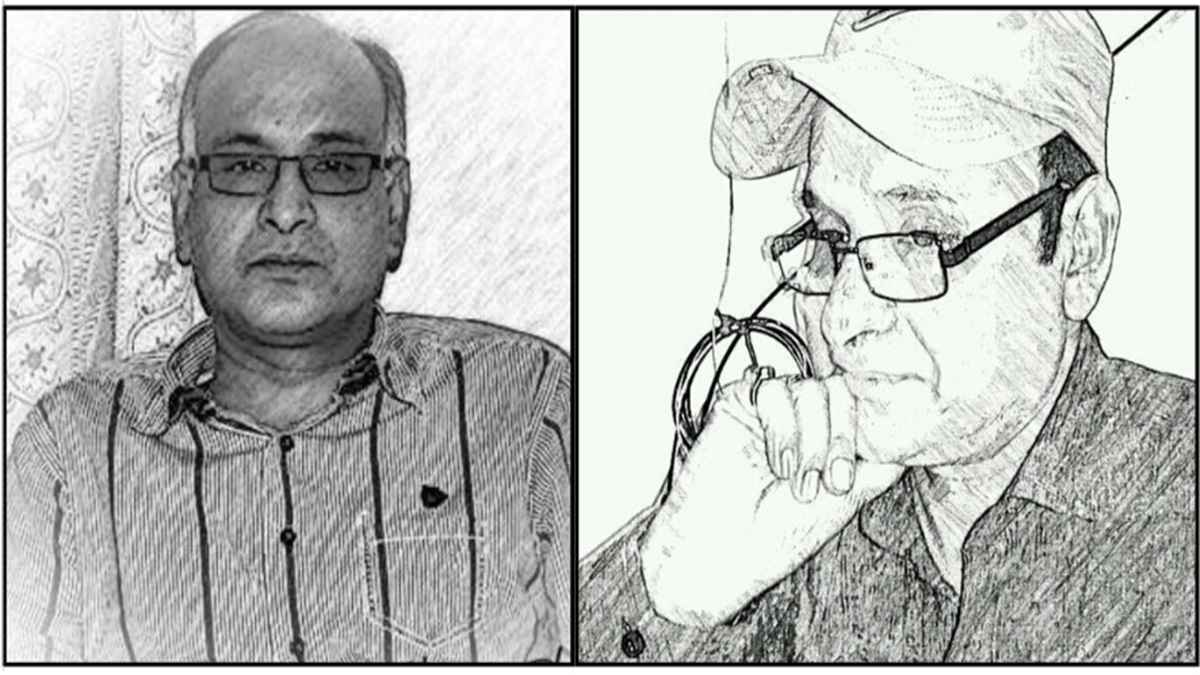
- August 30, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-19
शाम की सोच: रिश्तों की धूप-छाँव
शाम ढलते ही दीवारों पर पड़ी लम्बी छायाएँ कुछ कहती हैं- जैसे कोई पुराना रिश्ता धीरे से कंधे पर हाथ रख दे। हम सब इन्हीं छायाओं के बीच जीते आये हैं- कभी माँ की साँसों जैसी गर्म, कभी पिता के मौन जैसी ठिठुरी हुई।
रिश्ते ही तो हैं जो हमें बनाते-बिगाड़ते हैं। एक पत्नी की चुप्पी में पूरा घर बसता है, तो एक दोस्त की हँसी में खोयी हुई जवानी। किताबों में लिखा है कि पुरखे पेड़ों से बातें करते थे, नदियों को बहन कहते थे। आज हमने उन्हें सिर्फ़ ‘रिसोर्स’ कह दिया- पानी का, लकड़ी का, ज़मीन का।
***
एक बच्चा जब पहली बार किसी फूल को तोड़कर माँ के हाथ में देता है, तो वह सिर्फ़ फूल नहीं दे रहा होता- वह अपना हाथ भी दे रहा होता है। उसी हाथ में कभी उसकी शादी की अंगूठी होगी, कभी बुखार में पकड़ने के लिए कोई उँगली। पर आज तो हम अंगूठियाँ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और बुखार थर्मामीटर से नापते हैं।
रिश्ते अब ‘ट्रैक’ होते हैं- फ़ोन कॉल्स की लॉग लिस्ट में, मैसेज के नोटिफ़िकेशन में। कोई रोये तो इमोजी भेज देते हैं, कोई याद करे तो ‘रिएक्ट’ कर देते हैं। हमने अपनी धड़कनों को वाई-फाई सिग्नल समझ लिया है।
***
वह दादी जो कहानियों में भूत-पिशाच बताकर हमें डराती थी, आज उसका फ़ोन हम ‘मिस्ड’ कर देते हैं। वह पड़ोसी जिसके यहाँ बिना बताये चाय पी जाती थी, आज उसके दरवाज़े पर डोरबेल का कैमरा लगा है। हमने रिश्तों को ‘सेटल’ कर लिया है- जैसे कोई बैंक अकाउंट हो, जहाँ न निकासी की ज़रूरत हो, न जमा करने की।
पर ज़िंदगी तो वही है जो रिश्तों की जड़ों में बसती है। बिना जड़ के पेड़ कितने दिन हरा रहेगा?
***
आज शाम मैंने एक पुरानी अलमारी साफ़ की- उसमें से निकला पिता का वह पुराना कोट, जिसकी जेब में अभी भी उनके हाथ की गर्माहट थी। माँ की वह चिट्ठी, जिसमें उनकी अधूरी इच्छाएँ दबी थीं। ये चीज़ें सिर्फ़ कपड़े या कागज़ नहीं हैं- ये रिश्तों के वे धागे हैं जो हमें बाँधे रखते हैं। शायद हमें फिर से उन धागों को पकड़ना होगा। बिना इस डर के कि वे टूट जाएँगे।
नामों के जंगल में एक पुरानी कथा
एक गाँव था। उस गाँव में हर नाम के पीछे एक पेड़ लगा था- नीम वाला नीमचंद कहलाता, बरगद वाला बरगदी लाल। फिर एक दिन आँधी आयी। सारे पेड़ गिर गये। लोगों के नाम अब बे-पेड़ हो गये। तब गाँव वालों ने तय किया- अब हर नाम के आगे सिर्फ़ “इंसान” लगेगा। नीमचंद इंसान। बरगदी लाल इंसान… क्या यह कथा आज भी हमारे लिए कोई मायने रखती है?
नाम : पहचान या जंजीर?
हमारे नामों में जाति के फूल खिले हैं। उपनामों की जड़ें इतिहास के कुएं में पसरी हैं। कोई “शर्मा” है तो कोई “खान”, कोई “नेगी” तो कोई “राव”। ये सिर्फ़ शब्द नहीं, सामाजिक रसायन के वे फॉर्मूले हैं जो हमें अलग-अलग टेस्ट ट्यूबों में बंद कर देते हैं। जब कोई “सिंह” बनाम “विश्वकर्मा” की बहस छिड़ती है, तो क्या हम वास्तव में नामों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं? या उन पुराने पेड़ों की छाया के नीचे दबे हुए भूतों से?
धर्म के अक्षर, मज़हब के अंक
एक बच्चा स्कूल के फॉर्म में अपना नाम लिखता है- “मोहम्मद आरिफ़”। फॉर्म के नीचे एक कॉलम है— “धर्म”। वहाँ वह स्वतः भरा हुआ देखता है। उसकी उँगली हवा में ठिठक जाती है। क्या यह उसका चुनाव था? या किसी और का लिखा हुआ पुराना लेख? हमारे दस्तावेज़ हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, इससे पहले कि हम ख़ुद जान पाएँ।
क्या बदल सकते हैं हम?
1. नामों का भूगोल : केरल में “एस.एस. राजेंद्रन” जैसे नामों ने जाति को धुंधला कर दिया। क्या यह एक रास्ता हो सकता है?
2. धर्म का डिब्बा : जब कोई फॉर्म “धर्म” वाला कॉलम हटा दे, तो क्या आकाश गिर पड़ेगा?
3. उपनामों का अंतिम संस्कार : मराठी समाज ने “सावित्रीबाई फुले” के आंदोलन से उपनाम हटाने की शुरूआत की थी। आज वह धागा कहाँ खो गया?
एक पुरानी कथा का अंत
उस गाँव में जब सब “इंसान” हो गये, तो एक बूढ़े ने पूछा- “अब हम एक-दूसरे को कैसे पहचानेंगे?” एक बच्चे ने जवाब दिया- “आँखों से देखकर।” शायद यही उत्तर आज भी प्रासंगिक है। नामों के जंगल में हमें फिर से आँखें खोलनी होंगी। वे आँखें जो जाति नहीं, इंसान देख सकें। वे कान जो उपनाम नहीं, आवाज़ सुन सकें।
कमज़ोर
समय: रात के 11:47 बजे (वो वक़्त जब दिमाग़ शब्दों से खेलने लगता है)। आज “कमज़ोर” शब्द ने मुझे फिर से पकड़ लिया। यह कैसा शब्द है जो अपने भीतर ही अपना विरोध समेटे हुए है? ‘कम” और ‘ज़ोर”- दोनों मिलकर एक ऐसी ताक़त बनाते हैं जो दुर्बलता को भी चुनौती देती है। शायद यही भाषा का जादू है…
डॉ. शर्मा (मेरी काल्पनिक भाषाविज्ञानी मित्र) ने आज कहा- तुम्हारा ‘कमज़ोर’ वाला विचार तो सॉस्स्योर के ‘साइनिफायर’ और ‘साइनिफाइड’ के बीच की खाई को पाटता है! शब्द अपनी जड़ों से ही विद्रोह करता है।” मैंने हँसते हुए कहा- “तो क्या ‘कमज़ोरी’ भी एक तरह का ‘ज़ोर’ है? जैसे कोई कहे- ‘मेरी कमजोरी ही मेरी ताक़त है’?”
वह गंभीर हो गयीं- “बिल्कुल! यह ‘रिक्लेम्ड सेमैंटिक्स’ (Reclaimed Semantics) का उदाहरण है। समाज जिसे ‘कमज़ोरी’ कहता है, वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। देखो न, ‘क्वीयर’ शब्द तो अपमान से गर्व का प्रतीक बन गया!”
आज रात सोते समय यही ख़याल आया- “शब्दों के पंख होते हैं। वे अपने अर्थों से उड़कर नये आकाश छू लेते हैं।” शायद इसीलिए डायरी लिखना पसंद है… यहाँ शब्द बंधे नहीं होते। वे ‘कमज़ोर’ होकर भी ‘ज़ोर’ से भर जाते हैं।
माटी ने अपना एक सुर खो दिया
सांझ का धुँधलका, जब दीपक की लौ टिमटिमा रही है। आज शेख़ हुसैन चले गये। उनके जाने से लगा, जैसे छत्तीसगढ़ी लोकसंगीत के इतिहास का कोई जीता-जागता पन्ना फट गया हो। वे सिर्फ़ एक गायक नहीं थे, बल्कि हमारी सांस्कृतिक स्मृति के संवाहक थे। उनकी आवाज़ में वह सहजता थी जैसे कोई पुरखा किसी कथा को गा रहा हो- बिना लाग-लपेट के, बिना साज-सजावट के।
विद्यानिवास मिश्र जी कहा करते थे- “लोक की आवाज़ वह धागा है जो अतीत को वर्तमान से बाँधता है।” शेख़ हुसैन उसी धागे के धनी थे। जब छत्तीसगढ़ी गीत ‘प्रतिष्ठा’ के लिए तरस रहे थे, तब उन्होंने निर्मला इंगले के साथ मिलकर उन्हें गाया, और वह आवाज़ रेकॉर्ड्स पर उतरकर अमर हो गयी। क्या कोई भूल सकता है उनकी वह गायकी, जिसमें माटी की ख़ुशबू थी, नदियों का शोर था, और खेतों का रूहानी सन्नाटा?
आकाशवाणी पर उनकी आवाज़ सुनकर लगता था, जैसे कोई दादा-दादी हमें क़िस्सा सुना रहे हों। वे छत्तीसगढ़ के पहले कलाकार थे जिनका रेकॉर्ड जारी हुआ- यह कोई छोटी बात नहीं। यह एक सांस्कृतिक क्रांति थी, जिसकी गूँज आज भी सुनायी देती है। आज उनके जाने से एक प्रश्न मन में उठता है: क्या हमारी नयी पीढ़ी उस विरासत को संभाल पाएगी? जिस तरह नदियाँ पुराने किनारों को छोड़ देती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपनी जड़ों को भूलते जाएँ?
श्रद्धांजलि:
“तुम्हारा गाया हर गीत अब एक किवंदती है।
तुम्हारी आवाज़ में बसा छत्तीसगढ़,
अब हमारे दिलों में धड़केगा।”
-एक श्रोता, एक अनुगामी
(पन्ने के कोने में एक सूखा पलाश पत्ता रखा हुआ है, जैसे किसी विदाई का प्रतीक…)
11 जून, 2014
अगिन जल कर बन जाता अमरित
समय – सुबह की वह धुंध जब पत्तों पर ओस की लिपि लिखी जाती है। आज विजेन्द्र जी की वह बात याद आयी- “कवि को फूलों के मौसम और खेतों की लय जाननी चाहिए।” सच में, कितने कवि हैं जो चंपा के नारंगी रंग को, मोगरे की मदहोश महक को, पारिजात के रात-भर चटखने वाले सफ़ेद को जानते हैं? हम शब्दों से खेलते हैं पर उनकी जड़ें कहाँ हैं, यह भूल जाते हैं।
मैंने आज सुबह अपनी छत पर खड़े होकर देखा- एक मधुमक्खी जूही के फूल पर मँडरा रही थी। उसकी व्यस्तता में कितना संगीत था! क्या हम शहरों में रहने वाले इस संगीत से वंचित नहीं होते जा रहे? विजेन्द्र जी सही कहते थे- अरहर और सरसों में फ़र्क़ न जानना कोई गर्व की बात नहीं। यह तो हमारी संवेदनाओं के सूखने का प्रमाण है।
जब प्यार की बात आयी तो मन में वही पंक्तियाँ उठीं- “अगिन जल कर बन जाता अमरित…” क्या प्यार भी एक तरह का कवित्व नहीं है? जो हमें फूलों की भाषा, पेड़ों के संकेत, मौसमों के स्पर्श से जोड़ता है? वही तो है जो रास्तों को तीर्थ बना देता है, दिशाओं को मंत्र।
अब बचा हुआ रात में टांक रहा हूँ- आज चाँदनी में चमेली के पौधे को देखा। उसकी पत्तियाँ किसी प्राचीन ग्रंथ की पाण्डुलिपि सी लग रही थीं। शायद प्रकृति हमें रोज़ नयी कविताएँ लिखकर देती है, बस हमें पढ़ने की कला भूल गयी है।
ऊँचाई
बाज़ार ने कहा- “तुम्हारे पैर ज़मीन से ज़रा ऊपर उठेंगे तो दुनिया और सुंदर दिखेगी।”
उसने सोचा- “हो सकता है।” जूते ने उसके पैरों को ऊपर उठा दिया। सच, दुनिया ऊपर से थोड़ी अलग दिखी। लेकिन जब वह भागना चाहती तो पैर ज़मीन को याद करते। ज़मीन जो अब दूर थी।
एक दिन अंधड़ आया। पुराने पैरों वाली लड़कियाँ तो भाग गयीं। वह गिरी रह गयी। जूते अब भी ऊँचे थे। पैरों से लहू बह रहा था। बाज़ार वालों ने कहा- “यह नया डिज़ाइन लो, इसमें गिरोगी नहीं।” उसने देखा- वही ऊँचाई। बस रंग नया था।
(कहानी ख़त्म होते-होते एक पत्ता गिरा। वह ज़मीन से चिपक गया।)
जिस दिन दर्ज़ी फिर बदला
समय – सुबह की वह धूप जब सिलाई मशीन की सूई और छाया दोनों एक साथ चलते हैं। आज फिर नया दर्ज़ी मिला। उसने कहा- “यह कट तो बिल्कुल नया होगा।” मैं चुप रहा। पुराने कपड़े ही दे दिये। कमरे में लौटकर सोचा– कितनी बार कट बदला, धागे के रंग बदले, बटनों के छेद भरते-फिर से बनते रहे… पर शरीर तो वही रहा जो सिलाई के बाद भी ढीला ही लगता था।
दोपहर में देखा– चींटी वही पुराने रास्ते पर चल रही थी, चाहे दीवार का रंग बदल दिया गया हो। [पन्ने के निचले हिस्से में एक टूटा हुआ धागा चिपका है, जैसे किसी पुरानी सिलाई से गिर गया हो]
क्रमश:

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

