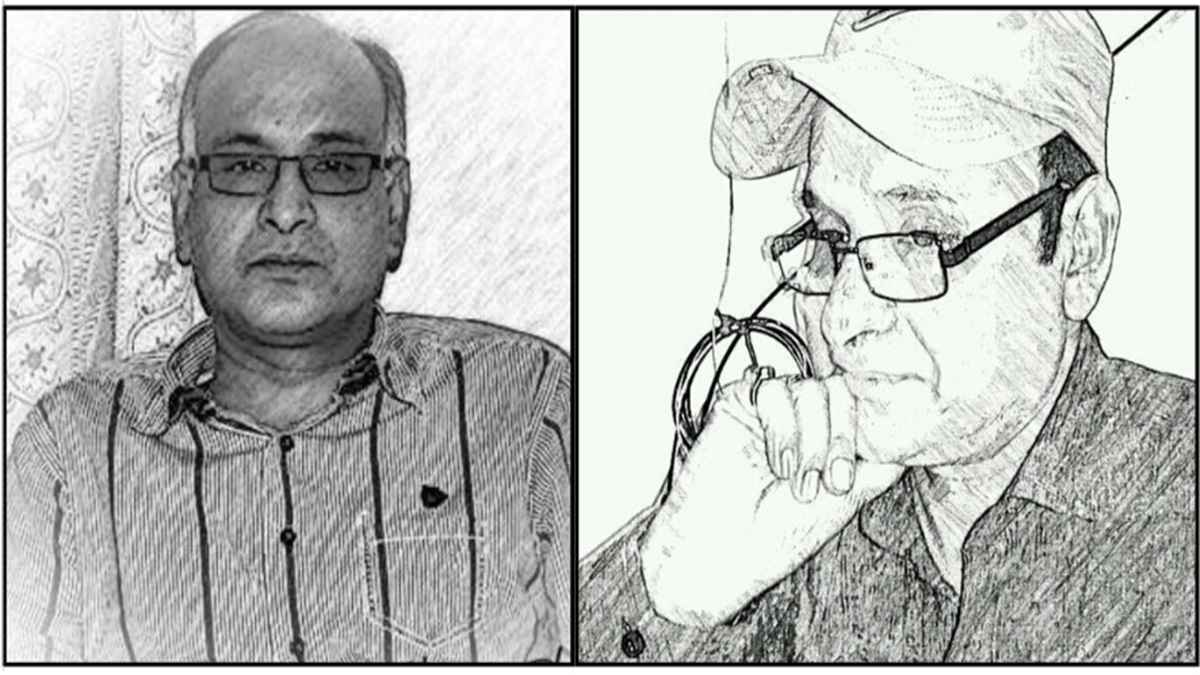
- September 6, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-21
20 जून, 2014
लेखकों के लेखक को बधाई
रायपुर से रायगढ़ की यात्रा सिर्फ़ दो शहरों के बीच की दूरी नापना भर नहीं थी। कल्पना मेरे साथ थी। कल्पना जो बाल कवि शंभुलाल शर्मा ‘वसंत’ जी ने अपने विद्यार्थियों की नोटबुक में बीज की तरह बोयी है। आज उनके पुत्र चिरंजीव ओमप्रकाश शर्मा के विवाह समारोह में शामिल होने आया हूँ।
‘वसंत’ जी को देखता हूँ तो लगता है जैसे शिक्षकों की उस अदृश्य परंपरा का साकार रूप देख रहा हूँ, जिसमें गुरु और शिष्य का संबंध पाठ्यपुस्तकों की सीमाओं से परे जाता है। करमागढ़ के इस शिक्षक ने न जाने कितने युवा मनों में साहित्य के बीज रोपे हैं। उनके द्वारा प्रेरित किये गये विद्यार्थी आज समर्थ लेखक हैं- यही तो किसी शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
शादी के इस अवसर पर उनका घर साहित्य की उस सामूहिक रचना की तरह लग रहा है, जिसमें हर मेहमान एक पात्र है। मैं देख रहा हूँ- यहाँ हर बधाई में एक कहानी छिपी है, हर मुस्कान में कोई पंक्ति दबी है। ‘वसंत’ जी की विनम्र मुस्कान में उन सभी युवा लेखकों का अहसास है जिन्हें उन्होंने रचना सिखायी।
आज का यह विवाह समारोह सिर्फ़ दो हृदयों का मिलन नहीं, बल्कि साहित्य की उस धारा का भी उत्सव है जिसे ‘वसंत’ जी जैसे शिक्षक निरंतर प्रवाहित करते रहते हैं।
वह बूढ़ा आदमी जो हमेशा जवान रहता है
तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की
यह एहतियात ज़रूरी है इस शहर के लिए
भोपाल के भाषा संचालनालय के उस कमरे में जहाँ दुष्यंत कुमार की ग़ज़लों की गर्माहट दीवारों से टकराती थी, एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वह चाय मँगवाने बाहर निकले तो उनके क़दमों की आवाज़ भी ग़ज़ल की तरह लग रही थी। चपरासी को चाय और बीड़ी भेजकर जब वे लौटे, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख़्ती थी- वैसी ही जैसे कोई अपनी ही रची हुई पंक्तियों से डर गया हो।
“जानते हो इन ग़ज़लों ने मेरे साथ क्या किया?” उन्होंने पूछा। बात 1975 की है, जब बीबीसी ने भारत के राष्ट्रपति से पूछ लिया था कि यह ‘बूढ़ा आदमी’ कौन है, जो देश की अँधेरी कोठरी में रोशनदान बनकर खड़ा है? दिल्ली से पूछताछ हुई, प्रदेश सरकार ने जवाब माँगा। आपातकाल के उन दिनों में यह सवाल एक ज़ख़्म की तरह था, जिसे हर कोई छूने से डर रहा था। बीबीसी ने उन्हें वह बूढ़ा आदमी वाला शेर भी सुना दिया:
एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यों कहो
इस अँधेरी कोठरी में एक रोशनदान है
कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए
मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है
मैंने देखा कि दुष्यंत के चेहरे पर अचानक एक शरारत भरी मुस्कान आ गयी। “मैंने लिख दिया कि वह बूढ़ा आदमी विनोबा भावे हैं,” उन्होंने कहा। यह वही विनोबा थे जिन्होंने आपातकाल को ‘अनुशासन पर्व’ कहा था। कवि ने अपनी क़लम की इस चाल से न सिर्फ़ खुद को बचाया, बल्कि उस पूरे दौर की विडंबना को भी उजागर कर दिया।
आज जब विजय बहादुर सिंह जी से सुना यह क़िस्सा डायरी में टाँक रहा हूँ, तो लगता है कि वह बूढ़ा आदमी कहीं गया ही नहीं। वह अब भी इस देश की गलियों में घूम रहा है- कभी चीथड़ों में, कभी नये कपड़ों में, पर हमेशा वही पुराना सवाल लिये हुए: “ये बूढ़ा आदमी कौन है?” शायद यही वह सवाल है जो हर युग में नये सिरे से पूछा जाता रहेगा, और हर बार इसका जवाब अलग होगा।
दुष्यंत ने उस वक़्त जो जवाब दिया था, वह सिर्फ़ एक बचाव नहीं था। यह उस कवि की चतुराई थी जो जानता था कि कभी-कभी सच को बचाने के लिए उसे मुखौटे की ज़रूरत होती है। आज जब हम उन पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो वह बूढ़ा आदमी हमारे सामने नये रूप में खड़ा हो जाता है- कभी विनोबा के भेष में, कभी किसी और के। पर वह है तो हमेशा वही- इस देश का अंतहीन सवाल, इसकी अँधेरी कोठरी का वह रोशनदान जो कभी बंद नहीं होता।
21 जून, 2014
शब्दों का देश
फ़ेसबुक के एक मित्र के प्रश्न पर: दुनिया, ग़रीब, जवाब, अमीर, मशहूर, किताब, तरक्की, अजीब, नतीज़ा, मदद, ईमानदार, इलाज़, क़िस्सा, मालूम, आदमी, इज्जत, ख़त, नशा, बहस अरबी भाषा के शब्द हैं।
रास्ता, आराम, ज़िंदगी, दुकान, बीमार, सिपाही, ख़ून, बाम, क़लम, सितार, ज़मीन, कुश्ती, चेहरा, गुलाब, पुल, मुफ़्त, खरगोश, रूमाल, गिरफ़्तार आदि फ़ारसी भाषा के शब्द हैं।
कैंची, कुली, लाश, दारोगा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर आदि तुर्की भाषा के शब्द हैं। अलमारी, साबुन, तौलिया, बाल्टी, कमरा, गमला, चाबी, मेज़, संतरा आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। बाक़ी फिर कभी…
23 जून, 2020
दोपहर में गाँव
हम कुछ ढूँढ़ रहे थे। कुछ खोया हुआ, कुछ छूटा हुआ, या शायद कुछ जो कभी था ही नहीं। अलमारी के कोने में धूल चाट रही कागज़ की पुरानी परतों के बीच यह लघु शोध-प्रबंध मिला— नौ साल पहले का, मेरे निबंध संग्रह “दोपहर में गाँव” पर लिखा हुआ। एक दक्षिण भारतीय छात्रा, कु.टी.एस. सरिता ने इसे अपनी एम.फ़िल. के लिए बनाया था। डॉ. शैल शर्मा के निर्देशन में।
कागज़ पीला हो चुका था। शब्दों की स्याही थोड़ी धुँधली। पर वहाँ एक जिज्ञासा थी— किसी और की नज़र से देखा हुआ मेरा लिखा। जैसे कोई दूर से आया हो और मेरे गाँव की धूल को अपनी उँगलियों पर मलकर कहा हो— “यह तो सोना है।”
ढूँढते समय क्या मिलता है? वह नहीं, जिसकी तलाश थी। बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जिसका पता भी नहीं था कि खोया हुआ है। चाबी गिर जाती है तो पुरानी किताब मिल जाती है। किताब खोलते हैं तो उसमें सूखा हुआ गुलाब मिल जाता है। गुलाब उठाते हैं तो याद आता है— कोई चेहरा, कोई दोपहर, कोई गाँव। और फिर लगता है—शायद यही तलाश थी।
रचना का रहस्य, या बिना रहस्य का रचना?
राजेश जोशी जी की बात पढ़कर लगा—क्या सचमुच रचना-प्रक्रिया को जाना नहीं जा सकता? या जान लेने से वह ‘प्रोडक्शन’ बन जाती है? मैंने अपनी डायरी के पन्ने पलटे। कुछ अधूरे वाक्य, कुछ कटे-फटे शब्द, कुछ ऐसे पैराग्राफ़ जिनके आख़िर में प्रश्नचिह्न लगे थे— मानो वे मुझसे पूछ रहे हों: “तुम्हारी रचना कहाँ से आती है?”
मेरे लिए लिखना एक साँस लेने जैसा है— बिना सोचे होता है, पर उसके पीछे फेफड़ों का पूरा तंत्र काम कर रहा होता है। कभी कोई दृश्य चुभ जाता है: एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा बूढ़ा, जिसकी छाया दोपहर की धूप में उससे भी ज़्यादा थकी हुई लगती है। कभी कोई वाक्य कान में गूँजता है: “इस शहर में अकेलापन भीड़-भाड़ में रहता है।” फिर वह मन में घर कर जाता है— जैसे अनाज के दाने को चिड़िया चोंच में दबाये उड़ती हो, और वह कहीं गिरकर अंकुरित होने लगे।
एकांत? हाँ, वह तो चाहिए। पर कभी-कभी शोर के बीच भी एकांत मिल जाता है— जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा कोई यात्री खिड़की से बाहर देखते हुए अपने भीतर उतर जाता है। मैं अक्सर ऐसे ही यात्रियों जैसा हूँ। शब्द पहले टुकड़ों में आते हैं। फिर उन्हें जोड़ता हूँ, तोड़ता हूँ, कभी दरवाज़े पर लटका देता हूँ, कभी अलमारी में धूल खाने के लिए छोड़ देता हूँ। छपने के बाद भी बदलाव होते हैं—क्योंकि रचना जीवित चीज़ है। वह साँस लेती है, बड़ी होती है, और कभी-कभी अपने ही जन्मदाता से मुँह फेर लेती है।
शायद यही मेरी मौलिक समस्या है— मैं नहीं जानता कि मैं कैसे लिखता हूँ। और अगर जान भी लूँ, तो कल का लिखा उस नियम को तोड़ देगा। रचना का रहस्य? वह तो हर बार नये सिरे से शुरू होता है— जैसे हर सुबह सूरज उगता है, पर उसकी किरणें कभी एक-सी नहीं होतीं।
दृश्य के पार, अदृश्य के घर
एक पेड़ देखा। उसकी छाया नहीं देखी। छाया को देखने के लिए धूप चाहिए। धूप को देखने के लिए आँख। आँख को देखने के लिए क्या? शायद वही अदृश्य जो दृश्य के भीतर साँस लेता है।
मैं बैठा हूँ इस कमरे में। मेज़ पर रखी किताबें, दीवार पर टँगी घड़ी, खिड़की से झाँकता आकाश– सब दिख रहा है। पर उस लड़के का क्या जो अभी-अभी इसी कमरे से निकला? वह तो चला गया, पर उसकी हँसी की आवाज़ अभी भी हवा में तैर रही है। क्या आवाज़ भी अदृश्य नहीं होती?
प्रसिद्ध उपन्यास ‘द साउंड एंड द फ्यूरी’ में क्वेंटिन कहता है– “समय तो वह चीज़ है जिसके बारे में सब जानते हैं, जब तक कोई उसके बारे में पूछ न ले।” अदृश्य भी ऐसा ही है। हम उसे जीते हैं, पर जब उसे समझने बैठते हैं तो वह हाथ से फिसल जाता है, जैसे नदी का पानी।
आज सुबह एक कौआ खिड़की पर आया। उसने काँव-काँव की। मैंने सोचा– यह आवाज़ कहाँ जाती है? हवा में घुल जाती है या किसी के कानों में जाकर बस जाती है? फिर याद आया– रिल्के ने लिखा था, “हर आवाज़ एक अनंत स्थान बनाती है।” शायद अदृश्य यही अनंत स्थान है जहाँ सब कुछ जाता है और कुछ भी नहीं जाता।
एक बच्चे ने पूछा– “हवा का रंग क्या होता है?” मैं चुप रह गया। हम दृश्य के इतने आदी हो चुके हैं कि अदृश्य को महज अभाव समझते हैं। पर अदृश्य तो वह आधार है जिस पर दृश्य टिका है, जैसे कैनवास पर चित्र।
महाभारत में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था– “क्या तुम देख पा रहे हो?” संजय ने कहा– “हाँ, मैं देख रहा हूँ वह सब जो दिखायी नहीं देता।” शायद रचनात्मकता भी यही है– दिखायी न देने वाले को देखने की क्षमता।
आज शाम बारिश हुई। बूँदें खिड़की के शीशे पर गिरीं और गायब हो गयीं। पर उनके गायब होने का अहसास बना रहा। अदृश्य का यही तो चमत्कार है– वह जाता नहीं, सिर्फ़ रूप बदलता है। जैसे प्रेम, जो कभी शब्दों में होता है, कभी मौन में, कभी स्पर्श में, और कभी सिर्फ़ एक अनुभूति में।
दृश्य को प्रणाम, जो हमें जीवन दिखाता है। अदृश्य को प्रणाम, जो हमें जीवन का अर्थ समझाता है।
मन कत्थक-कत्थक
रायगढ़ आया तो पैरों ने अपने-आप थिरकना शुरू कर दिया। यहाँ की हवा में ताल बजती है। सड़कें बोलती हैं– “धिं धिं, धागे तिरकिट!”
कत्थक और रायगढ़ एक दूसरे के पर्याय हैं और आदिवासी राजा महराज चक्रधर सिंह इस पर्याय के आदि प्रवाह। वे कत्थक सम्राट थे। महान् तबला वादक। संगीत के ऐतिहासिक और शास्त्रीय कृतियों के लेखक। आज भी रायगढ़ में प्रतिवर्ष 15 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय चक्रधर समारोह उनके जन्मदिन गणेश चतुर्थी से शुरू होता है।
भांजी प्रांजल थकी हुई लौटी थी। स्कूल बैग कंधे पर, पैरों में घुंघरू की आवाज़ नहीं। पर जैसे ही कहा– “एक परन हो जाये?”– उसके चेहरे पर वही रौनक़ आ गयी जो चक्रधर महराज के ज़माने में रही होगी।
वैष्णव संगीत महाविद्यालय से सीखकर आयी है। चौथी पीढ़ी की गुरु-शिष्या। पैरों ने ज़मीन को छुआ तो लगा– यह वही ज़मीन है जहाँ चक्रधर महराज ने ताल दिया था। उनके बाद फिरतू महराज, फिर राममूर्ति वैष्णव, अब बासंती और शरद जी– सबकी साँसें इसी हवा में घुली हैं।
प्रांजल ने शुरू किया – “शांताकारम्…”
पैरों ने कहा – “भुजगशयनम्!”
हाथों ने कहा – “पद्मनाभम्!”
और घुंघरुओं ने कहा – “सुरेशम्!”
धीमे-धीमे ताल बढ़ने लगा। “धिं धिं। धागे तिरकिट। तू ना। क त्ता।”
मन कहने लगा– यह सिर्फ़ नृत्य नहीं है। यह तो वह धागा है जो चक्रधर महराज के ज़माने से चला आ रहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। जैसे नदी बहती है तो अपने साथ पुराने पत्ते भी ले जाती है, नये फूल भी।
आलोचक डॉ. बलदेव (कका) कहते हैं – “यह परंपरा का तार है।” पर तार नहीं, साँस है। जैसे पेड़ की पुरानी शाखाएँ नयी कलियों को जन्म देती हैं, वैसे ही यह घराना भी आगे बढ़ रहा है। प्रांजल ने जब “धी ना” कहा तो लगा– चक्रधर महराज कहीं दूर से मुस्कुरा रहे हैं।
क्रमश:

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

