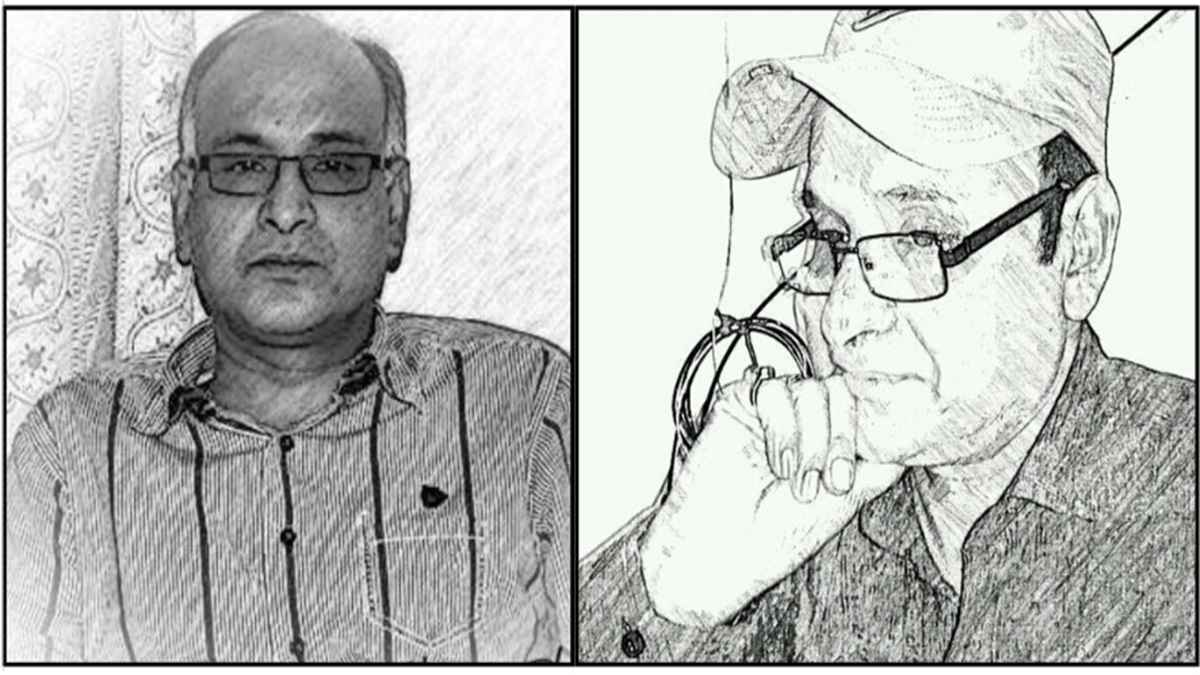
- August 5, 2025
- आब-ओ-हवा
- 1
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-12
धूणी तपे तीर
2 अप्रैल, 2014
कहीं किसी पुराने काग़ज़ के पन्ने पर लिख रहा था। 19 मार्च 2014 का वह पन्ना पूरा करता हूँ। आदिम जनों की भूत-भविष्य और वर्तमान की अभिव्यक्ति को समर्पित एक अच्छा नाम- हरिराम मीणा। आदिवासियों के संघर्ष पर रचित उनका उपन्यास- धूणी तपे तीर। आज उपन्यास की भूमिका से ही गुज़र पाया हूँ।
पूरी कथा को पी जाने की जिज्ञासा और भी बढ़ चली है। मेरे सम्मुख अपने गाँव के आदिवासी संगी-साथियों के निर्मल और निष्कलुष चेहरे झिलमिलाने लगे हैं। पार्श्व से उनके संघर्ष के लोकगीत जैसे गूँज उठे हों। आपने अपनी भूमिका में एक नृतत्वीय सच्चाई को फिर से रख इस विश्वास को और भी पुष्ट किया है: “आदिवासी दुनिया का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव की उत्पत्ति का।” पर उन भ्रमित समाजशास्त्रियों का क्या करें जो उन्हें पिछड़ा मानव ही घोषित करने पर तुले हुए हैं। और हमारे भोथरे नीति-नियंता प्रशासनिक अधिकारियों का भी, जो आदिवासियों के विकास को किताबी और पश्चिमी मॉडल से ही तय करने पर आमादा हैं। इस उपन्यास को भारतीय प्रशासनिक अकादमी और पुलिस अकादमी में आने वाले परमज्ञानवंत देवपुरुषों को मार-मार कर पढ़ाना क्यों नहीं चाहिए!
आप पिछले दिनों इधर आये भी थे। छत्तीसगढ़ और विशेषत: रायपुर भी। विश्वरंजन जी के साथ आपकी अच्छी बैठक भी हुई। मेरा सौभाग्य नहीं था उन दिनों जबकि संसूचित था भी। कुछ सरकारी काम की सीमाएँ और कुछ अपरिहार्य पारिवारिक ज़िम्मेदारी। अफ़सोस रहेगा- न मिल पाने का। लेकिन भूमिका पढ़कर मानगढ़ जाने की उत्कंठा बढ़ चली है। देखें कब यह उत्कंठा पूरी होती है। शायद आपके भी दर्शन हों। मुझे उन दिनों पता ही नहीं चला कि इसी उपन्यास पर आपको के.के. बिरला फाउंडेशन ने 2012 के 22वें पुरस्कार देने का सर्वोचित निर्णय लिया है। आप तक मेरी आत्मीय बधाई पहुँचे आत्मीय मार्ग से। देर से ही सही, बहुत दूरी से ही सही, लेकिन लेखक-पाठक के बीच दूरी कहाँ होती है: गर दोनों परम सच्चे हों।
पति : पत्नी : वह
किसी स्त्रीवादी लेखिका ने लिखा है: “पति प्यार नहीं होता, और प्यार पति नहीं होता।”
अर्थात् पति से प्यार संभव नहीं और प्रेमी से विवाह संभव नहीं। अर्थात् तन पति के पास और मन प्रेमी के पास। अर्थात् पति के लिए मन समर्पित नहीं और प्रेमी के लिए तन समर्पित नहीं। अर्थात् दो के बीच एक तीसरे की उपस्थिति की भी स्वीकार्यता। अर्थात् पति-पत्नी के बीच प्रेमी की स्वीकृति। अर्थात् वैवाहिक जीवन की सभी उपलब्धियाँ और मनोमय जीवन की सभी सौगातें साथ-साथ।
अर्थात् पत्नी को पति से नहीं, बल्कि किसी और से प्रेम करने की पूरी छूट। अर्थात् बेटे-बेटियाँ केवल पति की संतानें, पत्नी की नहीं। अर्थात् परिवार का संरक्षण एक औपचारिकता मात्र। अर्थात् विवाह के बाद बग़ावत। अर्थात् विवाह से पूर्व तक ही संस्कारों की विवशतामूलक रक्षा। अर्थात् विवाह के बाद सब कुछ तहस-नहस। अर्थात् बहुत सारे और अर्थात् भी…
लेखिका के उक्त विचार (या किसी लेखक के, जो पति-पत्नी के अलावा प्रेमिका की बात रखे) के पीछे की पीड़ा प्रेम की सर्वोच्च आकांक्षा और नैतिक लक्ष्य से उपजी हो सकती है। यह पारंपरिक विवाह पद्धति का सबसे बड़ा अमानवीय और अंधकारमय पक्ष भी हो सकता है। मूलतः यह विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं के विनाश का आमंत्रण है। यदि यह वास्तव में भारतीय विवाह पद्धति की कमियों से उपजा आक्रोश और आधुनिक वैकल्पिक उपाय मात्र है, तो समय रहते हम विवाह को लेकर किन-किन संशोधनों की वकालत करना चाहेंगे?
पत्नी : पति का आर्काइव!
अपने ही प्रकाशक से 3-4 साल बाद अपनी किसी पूर्व प्रकाशित किताब की 1-2 प्रतियाँ भला माँग कर देखें, क्या कहेगा वह? लेकिन शिल्पायन, दिल्ली के भाई ललित शर्मा का आभार जो उन्होंने मेरे तीसरे कविता संग्रह ‘अबोले के विरुद्ध’ की 4 प्रतियाँ फिर से मुझे भेज दीं। वह भी नि:शुल्क। भले ही विलंब से।
मैं किसी प्रिय पाठक को अपनी लेखकीय प्रति भी दे बैठा था। आज मन को बड़ा सुकून मिला। पत्नी को भी अब जबाब दे पाऊँगा कि ये लो 1 प्रति तो आप संभाल कर रखिए। जैसे मेरी सारी किताबों को संभाल कर रखी हैं। सचमुच एक भली पत्नी पति का आर्काइव ही नहीं संभालती वह पति की आर्काइव भी होती है।
3 अप्रैल, 2014
देश
भारत एक अजगर है, जिसका सिर 22वीं सदी की ओर बढ़ रहा है और पूँछ है कि ईसा पूर्व 1200 में ही ठहरी हुई।
5 अप्रैल, 2014
लेखक का आभारी
देश ये कैसा देश है! यहाँ तंत्र और व्यवस्था की सभी नादानियों और कारग़ुजारियों पर राजधानी के आसपास दशकों से अड्डा जमाये बैठे लेखक, पत्रकार और बुद्धिजीवी रोज़ रात में चैनलों के प्राइम टाईम आयोजनों में जमकर बोलते हैं पर उनके लिखा हुआ कुछ ख़ास असर नहीं कर पाता। लोग उनकी किसी एक किताब से भी उद्वेलित नहीं होते। अपनी लायब्रेरी के लिए सुरक्षित तो दूर की बात! कदाचित वे भी ऐसे लेखन को लफ़्फ़ाज़ी के अलावा कुछ नहीं मानते। शायद वे पढ़ते भी कहाँ हों! शायद उन्हें पढ़ना भी न हो! शायद वे अपने देशकाल को बदलना भी न चाहते हों! जो राजधानी से दूर के लेखक हैं उनकी सुनता कौन है?
जो भी हो : ऐसे समय जर्मन लेखक-पत्रकार ग्युंटर वल्लरफ्फ के पास मन और बुद्धि चली जाती है। वो ग्युंटर ही था, जिसने 80 के दशक में एक तुर्क के भेष में वर्षों जर्मन समाज में, सरकारी, ग़ैरसरकारी, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मुनाफ़ाखोरी, नस्लवाद, भ्रष्टाचार आदि समीं मामलों पर बड़ी-बड़ी, नामी-गिरामी हस्तियों के सबूत एकत्र करके पुस्तक लिखी, जिससे जर्मनी लगभग काँप उठा। किताब Genz Unten के छपते ही सरकारी प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। जाने कितने दुख झेले लेखक ने पर हिम्मत न हारी। जर्मनवासी आज भी इस लेखक का आभार मानते हैं- तहेदिल से।
सिर्फ़ इतना ही नहीं, उनकी यही किताब वहाँ अब तक की सबसे बड़ी बेस्टसेलर है। हमारे देश में, हम लेखकों में जोखिम उठाने का ऐसा माद्दा और सच्चा माद्दा कब आएगा? तब तक नहीं, जब तक हम अपनी भीतर की कमीनगी को टालते रहेंगे।
अर्थात्!
फ़ेसबुक पर ‘टैग’ करना अर्थात् उमस भरी रात में किसी पड़ोसी के छोटे-से आँगन में अपना बोरिया-बिस्तर लेकर जा धमकना।
क्या समुद्र का कोई अपना श्मशान होता है?
‘साहित्य अमृत’ पिछले 19 सालों से अनवरत् छप रही है। सारे देश में पढ़ी-सराही जा रही है। मन-आत्मा में प्रभाव भी छोड़ रही है। है तो यह प्रभात प्रकाशन, दिल्ली की निजी पत्रिका, पर इसका शुभारंभ प्रातः स्मरणीय पं. विद्यानिवास जैसे उद्भट विद्वान और साहित्यमनीषी के संपादन से शुरू हुआ है। ‘साहित्य अमृत’ के प्रबंधकों का आभार कि उनके आत्मीय सहयोग से साहित्य अमृत के सारे अंक मेरे पास सुरक्षित हैं– अब भी। जाने क्यों (वे ही जानें), हिंदी की इस सर्वाधिक प्रसारित और महत्वपूर्ण पत्रिका से वर्षों तक प्रलेस, जलेस और जसम के कार्ड होल्डर लेखक (?) इससे दूरी ही बनाकर चलते रहे, पर ‘साहित्य अमृत’ ने अपने आचरण में कोई तब्दीली नहीं की। न ही किसी ऐसे लेखकों की चिचौरी की।
अब कुछ समय से लगता है कि ऐसे लेखक भी यहाँ छपना ज़रूरी समझ रहे हैं। चलो, देर आयद दुरुस्त आयद।
अप्रैल 2014 का अंक इसका प्रमाण है। एक साथ यहाँ पहल सम्मान से सम्मानित ज्ञानेन्द्र पति, प्रलेस वाले आलोचक शैलेन्द्र चौहान, जनवादी कवि बोधिसत्व, जलेस के शिरोमणि कथाकार शेखर जोशी आदि घराने छाप लेखक छपे हैं। वैसे करें क्या कार्ड होल्डर लेखक! संगठन भी तो कभी-कभी ऐसी ग़ैर रचनात्मक दूरी का फ़तवा जारी करता रहता है। जैसे इन दिनों मध्यप्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका ‘साक्षात्कार’ से (जिसका संपादन कभी एक बड़े प्रगतिशील कवि भगवत रावत जी किया करते थे) प्रगतिशील लेखक संघ, मध्यप्रदेश के तीन कवियों राजेश जोशी, कुमार अम्बुज और नीलेश रघुवंशी की चेतावनीमूलक विज्ञप्ति के कारण बहुत सारे प्रगतिशील लेखकों ने भी दूरी बना रखी है। रखिए, आपके तर्क बिलकुल सही भी हो सकते हैं, और आपको यह अधिकार भी है, पर आप व्यवस्था में जिन राजनीतिक सात्विकता की वकालत करते हैं उस पर अमल भी तो समूचे स्तर पर होना चाहिए। यह नहीं कि एक छोर में कुछ और दूसरे छोर पर कुछ। भई सांगठनिक एकत्व के दर्शन तो सभी को हो ही जाते हैं।
और यह भी आपसे एक प्रश्न– आपने क्या अपने पाठकों के साथ धोखा नहीं किया? आपका आम पाठक (यानी आम आदमी भी) पत्रिका ख़रीदते वक़्त नहीं देखता कि यह किस वाद की, किस घराने की पत्रिका है भई! वह पत्रिका ख़रीदते वक़्त आप जैसे लेखकों को पहले तलाशता है।
खैर… मुझ जैसा पाठक क्यों पड़े आपके लफड़ों में। वह तो फिर से पढ़ना चाहेगा– मेरे राम का मुकुट भीग रहा है (पं. विद्यानिवास मिश्र), अमरकांत : वह जो हिंदी का चेखव था (प्रकाश मनु) और कवि बोधिसत्व की वह प्यारी और छोटी सी कविता (शीर्षक-सरल प्रश्न) और वह भी बिना वाद-फाद के चक्कर में पड़े:
क्या समुद्र का कोई अपना श्मशान होता है
क्या पेड़ों का कोई अपना आसमान होता है
क्या पंछियों का कोई अपना मचान होता है
क्या हमारे तथाकथित नामी (?) इस कविता से कुछ सबक़ लेना चाहेंगे और अच्छी पत्रिकाओं को अपनी रचनात्मकता से वंचित नहीं करते रहेंगे?
भिखारी
भिखारी कौन नहीं ? कुछ मंदिर के बाहर- कुछ मंदिर के भीतर!
7 अप्रैल, 2020
सजन रे झूठ मत बोलो!
सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं: मुंबईया लेखक नलिन सराफ़ की संस्मरणात्मक किताब। लोकधर्मी और जनचेतना के विख्यात गीतकार शैलेन्द्र जी पर। कल भोपाल से प्रकाशित और अरुण तिवारी जी द्वारा संपादित ‘प्रेरणा’ पत्रिका में उसी किताब की समीक्षा पढ़ते-पढ़ते शैलेन्द्र के गीत एक-एककर मन में गूंजने लगे….. सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी… तू ज़िंदा है तो ज़िंदग़ी की जीत में यक़ीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर..।
शैलेन्द्र जैसा दूसरा और कौन! ये फ़िल्मी गीत जीवन-यथार्थ के गीत हैं। हमारे बड़े-बड़े कवियों की कथित बड़ी कविताओं से अधिक पावरफ़ुल और मन-मनीषा को झकझोर कर रख देने में सक्षम।
हम साहित्य वालों से क्या एक बड़ा अनर्थ नहीं हो गया है, जो हमने जीवन से संबद्ध ज़रूरी फ़िल्मी कविताओं की साहित्यिकता को ईर्ष्यावश नहीं परखा? यह भी भुला बैठे कि देश से बाहर हमारी हिंदी और उसकी विश्वसनीयता इन्हीं फ़िल्मों और उनके ऐसे ही लोकप्रिय और मर्मस्पर्शी गीतों के माध्यम से स्थापित होती रही है? हो ही रही है।
शैलेन्द्र की ज़िदग़ी काँटों भरी रही। वे रेल्वे मे वेल्डिंग स्पेशलिस्ट थे। वेतन 150 रुपये मासिक। कुलियों के साथ भी काम किया। एक बार मथुरा में तो वे 45 रुपट्टी में ही गुज़र-बसर के लिए मजबूर। पर कहाँ हार मानी उन्होंने! पैसों के अभाव के बाद भी उन्होंने ‘तीसरी क़सम’ बनायी। वह बहुत नहीं चली पर गीत तो चल निकला:
तुम्हारे महल चौबारे
यहीं रह जाएंगे प्यारे
अकड़ किस बात की प्यारे
ये सर फिर भी झुकाना है
सजन रे झूठ मत बोलो…
क्या इन गीतों को दुनिया के होंठों पर हमारे समीक्षकों ने स्थापित किया, किसी पत्रिका ने स्थापित किया या किसी लेखक संगठन के झंडाबरदारों ने? झूठ मत बोलना मेरे प्यारे सजन!
अंतर
पुरुष सिर्फ़ ‘मकान’ बना सकता है, उसे ‘घर’ तो स्त्री ही बना सकती है।
क्रमश:

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky


रोचक, सराहनीय और साहित्यिक डायरी विधा का अत्युत्तम उद्धरण है