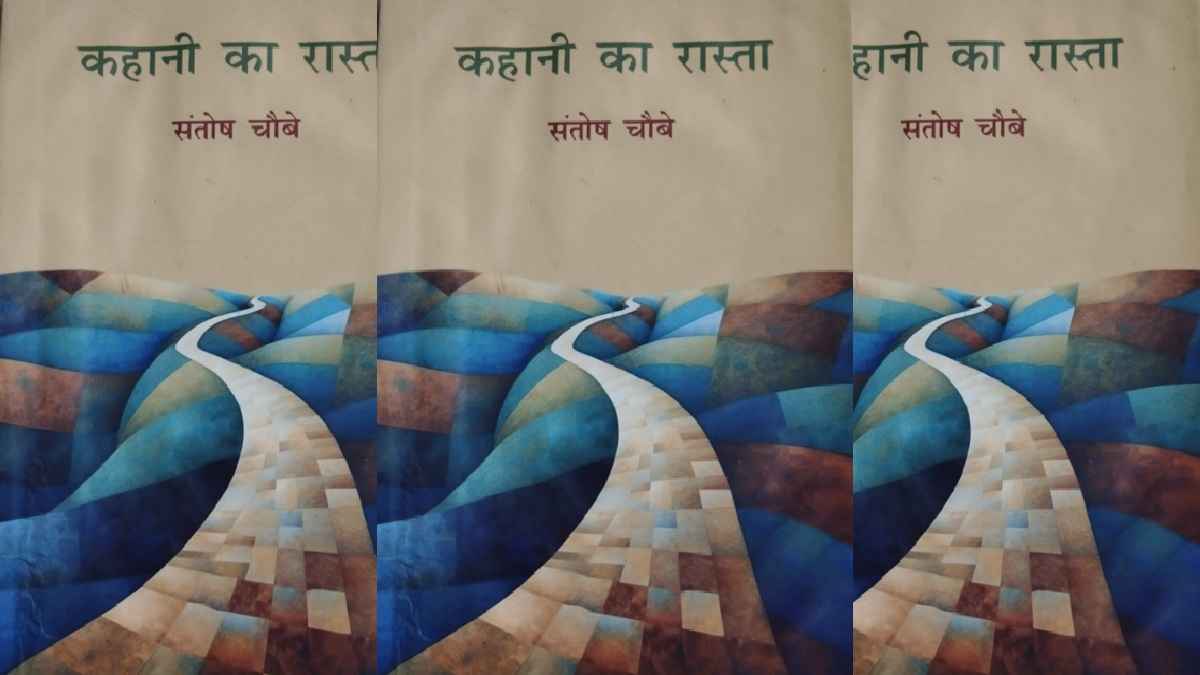
- August 7, 2025
- आब-ओ-हवा
- 4
ब्रज श्रीवास्तव की कलम से....
पुस्तक समीक्षा : कहानी की दुनिया की कहानी
पुस्तक- कहानी का रास्ता
लेखक- संतोष चौबे; प्रकाशक-आइसेक्ट प्रकाशन
वाचिक अथवा श्रुति में कथाएं हमारे जीवन में सबसे पहले आती हैं। दरअसल तो हमारे आसपास कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अलिखित कहानी के किरदार होते हैं। कुछ दृश्य कुछ घटित और कुछ कथन शायद किसी कहानी के हिस्से होते ही हैं। मेरे मन में ये विचार कहानी के तिलिस्म को समर्पित एक उम्दा किताब ‘कहानी का रास्ता’ पढ़कर आ रहे हैं। इस तरह मैं यह भी सोच रहा हूं कि एक अच्छी किताब हमारे भीतर न केवल संवेदनात्मक हलचल कर देती है बल्कि वैचारिक रूप से भी हमें द्रुत बना देती है।
कहानी की दुनिया साहित्य में इस तरह स्पेस लेती है कि ऐसा गद्य जो कहानी या कथा नहीं है उसे हम अभी तक इसी विधा के नाम में शामिल करके कथेतर नाम से जानते हैं। बड़ी-बड़ी कविताएं ठहर नहीं पातीं यदि उनमें कहानी नहीं होती। जैसे चौसर का प्रोलोग, जैसे वाल्मीकि की रामायण, जैसे मिल्टन का पैराडाइज़ लॉस्ट। आधुनिक कविता में भी लंबी कविताएं कहानी की मोहताज ही होती हैं। यह लिखने का मंतव्य काव्य को अवनमन कोण से देखने का नहीं, यह इस समय कथा संसार की व्यापकता को लखने का है जो ‘कहानी का रास्ता’ नामक किताब को पढ़कर ख्याल में आ रही है।
सुगठित गद्य शिल्प में इस किताब में प्रकाश डाला गया है कहानी के तत्वों, प्रादुर्भावों और प्रसवों पर। यह संतोष चौबे की एक मौलिक अन्वेषा है कि उनके ही नहीं किसी भी कहानी लेखक के कुछ औज़ार होते हैं, जो कहानी का रास्ता हासिल करने में शब्दों के पार अर्थ की तलाश भी करते हैं एवं नयेपन की तलाश भी। वे दृश्य विधान और विज्ञान के वाया आज की कहानी का शिल्प हासिल कर सकते हैं। यहाँ एक अनुच्छेद है जिसमें कथाकार वनमाली जी ने माया के संपादक और छायावाद के सुआलोचक रामनाथ सुमन को एक लंबी चिट्ठी में लिखा था:
“मेरे लिए जीवन नाम की चीज़ बड़ी gross है, वह शायद टुकड़ों में प्रत्यालोचना में ही दिख जाता है। और फिर कहानी में मैं सब बातें छोड़ने को तैयार हूं पर उसमें इंटेंसिटी और ड्रैमेटिक एलिमेंट का होना मैं बहुत लाज़िम समझता हूं। शायद यह दो चीज़ें ही कहानी की टेक्नीक की जान हैं।”
यह अंश इस किताब के पहले लेख से लिया है, जिसमें अनेक संदर्भों के साथ साथ एक निकटतम कथाकार से लेखक की मानस संगत की छवियां साहित्यिक क्लासिक में आयी हैं। सूत्र रूप में यह बात हमें आगे बढ़ने को कहती है, “कहानी का रास्ता कोई सपाट रास्ता नहीं। वह स्मृति से स्मृति में, मन से मन में और समय से समय में प्रवेश कर जाने वाला रास्ता है, कभी टेढ़ा—मेढ़ा, कभी घुमावदार, कभी पहाड़ों और कंदराओं से गुज़रता है और कभी मैदान में सरपट भागता”।
हम जानते हैं माधवराव सप्रे की कहानी ‘एक टोकरी का बोझ’ या ‘रानी केतकी की कहानी’ का पाठ और शिल्प अब दृश्य में नहीं है। न ही प्रेमचंद या जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, अश्क, मंटो या यशपाल जैसी संश्लिष्ट घटना प्रधान कहानी की त्वरा अब अनुपस्थित है बल्कि प्रतिस्थापित हो गयी है नयी कहानी से। हर विधा ने अब उत्तर आधुनिक युग का मिज़ाज अपना लिया है। ऐसा इसलिए भी कि समकालीनता को लाना लेखकीय ज़िम्मेदारी है। ‘आज की कहानी’ नामक लेख में संतोष चौबे ऐसे ही रिफ्रेंस लेकर कुछ विचार योग्य बातें लिखते हैं।
कहानी से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य विधाओं से अंत:क्रिया करे। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो ख़तरे पैदा किये हैं। हमारे विचार में तमाम वैविध्य के बावजूद यथार्थ की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां खोजी जा सकती हैं जो आमतौर पर स्पष्ट हैं और रचना के लिए पक्ष-विपक्ष के चयन का आधार भी तैयार करती हैं।
गांवों में व्याप्त अधूरेपन और सूचना तकनीक के विस्फोट के दृश्य के मद्देनज़र नयी कहानी की आमद के लिए संतोष चौबे ने सुचिंतित सुझाव इस निबंध में पेश किये हैं। मसलन नवीन सागर से साहचर्य के दिनों में वे किस तरह संवाद में रेलगाड़ी की गति को प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े होकर देखने के संबंध में सापेक्षता के सिद्धांत के सहारे कुछ विचार आवाजाही करते हैं। वहाँ गति, तापक्रम, टोन और दृश्यात्मकता अवयवों की तरह उपस्थित होते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक महत्वपूर्ण कोट यहाँ आया है: “कभी भी अपने पात्र के प्रति क्रूर और अन्यायी मत बनना।”
‘कहानी कहाँ है’ शीर्षक निबंध में हमें संतोष चौबे की उन सोहबतों के प्रसंग मिलते हैं जिनमें उन्होंने राजेश जोशी, शशांक, उदय प्रकाश और रमेश अग्रवाल से उनकी कहानियों पर कुछ टीकाएं पायीं।
‘उसने कहा था’ जैसी प्रतिमान कहानी के ज़िक्र के साथ लेखक कहानी में प्रेम पर एक चिंतन करते हैं। वह अ कहानी के लेखकों और गाँव, कस्बों, शहरों, महानगरों के किरदारों को लेकर बुनी कहानियों पर कुछ अच्छे निष्कर्ष देते हैं। इस सिलसिले में देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों और कहानीकारों के नाम आये हैं। मुझे यह कथन अच्छा लगा, “उनमें रुग्णता न हो.. प्रेम की मुक्ति का उल्लास हो या विछोह की गहरी उदासी, उसमें भावनात्मकता का होना आवश्यक है, शारीरिक आलंबन के साथ”।
संतोष चौबे अपने इन निबंधों में कहानी के रास्ते के जितने भी संभावित पड़ाव होते हैं, उन पर ठहरकर बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को लक्षित करते हैं। दृश्य विधान पर बात करते हुए वे प्रेमचंद की अनेक कहानियाँ सामने रखते हैं, ‘शतरंज के खिलाड़ी’ कहानी के एक दृश्य की मिसाल देते हैं। एक निबंध से दूसरे निबंध में प्रवेश करते हुए लगता ही नहीं कि कोई दरवाज़ा बाधा पैदा कर रहा है। कथाकार शशांक का तो जैसे उन्होंने पूरा मानस बांचा है। ‘सपने सोने नहीं देते’, ‘स्वप्न और यथार्थ’ पढ़कर वे एक बहुत अच्छा यूटोपिया देते हैं:
“यदि मैं स्वप्नयान में हूं तो मैं इधर-उधर नहीं जाउंगा, मैं एक ऐसे सपने में यात्रा करूंगा जो यथार्थ से स्वप्न में और सपने से यथार्थ में जाने का प्रयत्न करता है।”
इस किताब में मैं स्वयं संवेदनशील हो जाता हूँ, जब विदिशा (भेलसा) पर विजय का क़िस्सा एक लेख में पाता हूँ। मुझे मालूम होता है कि मोहम्मद फ़ारुख़ विदिशा का राजा था और उसने दोस्त मोहम्मद की अमानत में ख़यानत कर दी थी। इसके पहले वे इसी लेख में भोपाल के इतिहास के साथ-साथ इस्लामनगर आदि की बातें छेड़ते हैं। आज के भोपाल को सौ दो सौ साल पहले के भोपाल की सूरत से तुलना दिलचस्प है। डायरी के शिल्प में लिखा यह लेख स्थान और समय का अच्छा मैप बनाता है। नयेपन की तलाश जैसे संतोष जी का अभीष्ट है। वे बाज़ारीकरण, उपभोक्तावाद, उपनिवेशवाद जैसी वैश्विक बीमारियों को भी अपने चिंतन में लाते हैं। विधाओं के रसायन को वे भलीभांति जानते हैं। एक जगह लिखते हैं:
कविता संगीत के पास जाती है और संगीत कविता के पास। कहानी नाटक के पास जाती है और नाटक कहानी के पास। कविता कहानी के पास भी जा सकती है और कहानी चित्र कला से भी प्रभाव ग्रहण कर सकती है।
‘हिंदी कहानी के दो सौ बरस’ नामक लेख में तो हम समकालीन कहानी तक व्यवस्थित तरह से पहुंचते हैं। अंतिम लेख विज्ञान कथाओं का अद्भुत संसार को समर्पित है। यह सचमुच नवोन्मेषी है।

विस्तार से जानने के लिए यह पुस्तक पढ़ी ही जाना चाहिए। इस पुस्तक में कहानी के रहस्य भरे संसार की तरह ही जादू आया है। दृश्यों, क़िस्सों और अनुभवों की ऐसी यात्रा है जो स्मृति में बचे रह गये किसी स्वप्न के जैसी खटमिट्ठी लगती है। हम उससे गुज़रते हुए कभी उसमें शामिल भी लगते हैं और कभी उससे परे भी। तथ्य और कथ्य का अनुपात ग्राह्य कहा जा सकता है। एक निबंध में भोपाल शहर की स्थापना को अंजाम देने में कारगर भूमिका निभाने वाली रानी कमलापती, दोस्त मोहम्मद ख़ान की दिलचस्प दास्तानें आतीं हैं, जो श्याम मुंशी की किताब और राजेश जोशी के लेख में आयी बातों से भाषायी अभिव्यक्ति में अलग हैं। विदिशा, हलाली नदी के ब्यौरे भी आप केवल इसी किताब में पा सकते हैं। कहानी की दुनिया की भी कहानी बहुत तवील और ज़्यादा समावेशी हो सकती है, मगर इस किताब में सूत्र संकेत कम नहीं हैं। ऐसी अनेक कहानियाँ हैं जिन्होंने इस किताब के रास्ते से अपनी यात्रा की होगी। आगे आने वाली कहानियों को भी जाने-अनजाने में संतोष चौबे की रची इस वीथिका से गुज़रना समृद्ध ही करेगा।

ब्रज श्रीवास्तव
कोई संपादक समकालीन काव्य परिदृश्य में एक युवा स्वर कहता है तो कोई स्थापित कवि। ब्रज कवि होने के साथ ख़ुद एक संपादक भी हैं, 'साहित्य की बात' नामक समूह के संचालक भी और राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक आयोजनों के सूत्रधार भी। उनके आधा दर्जन कविता संग्रह आ चुके हैं और इतने ही संकलनों का संपादन भी वह कर चुके हैं। गायन, चित्र, पोस्टर आदि सृजन भी उनके कला व्यक्तित्व के आयाम हैं।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky


आपने ऐसा समां बांधा है कि किताब पढ़ने की ख़्वाहिश जाग उठी है।
जब समीक्षा इतनी अच्छी है तो पुस्तक कितनी अच्छी होगी।
धन्यवाद
समीक्षा बहुत अच्छी लगी, और लगा कि किताब ‘कहानी का रास्ता ‘ जितनी जल्दी हो, पढ़ लेना चाहिए। बस, पुस्तक मिलने की देर है। कहानी विधा पर इधर कई किताबें आई हैं इन दिनों। पर चौबे जी का लिखना कुछ अलग है-वे चीजों के आर-पार गुजरने और काफ़ी खोज-खबर के बाद ही लिखते हैं।
उनकी कहानियां पसंद आती हैं। बहरहाल, लेखक और समीक्षक को बधाई और शुभकामनाएं।