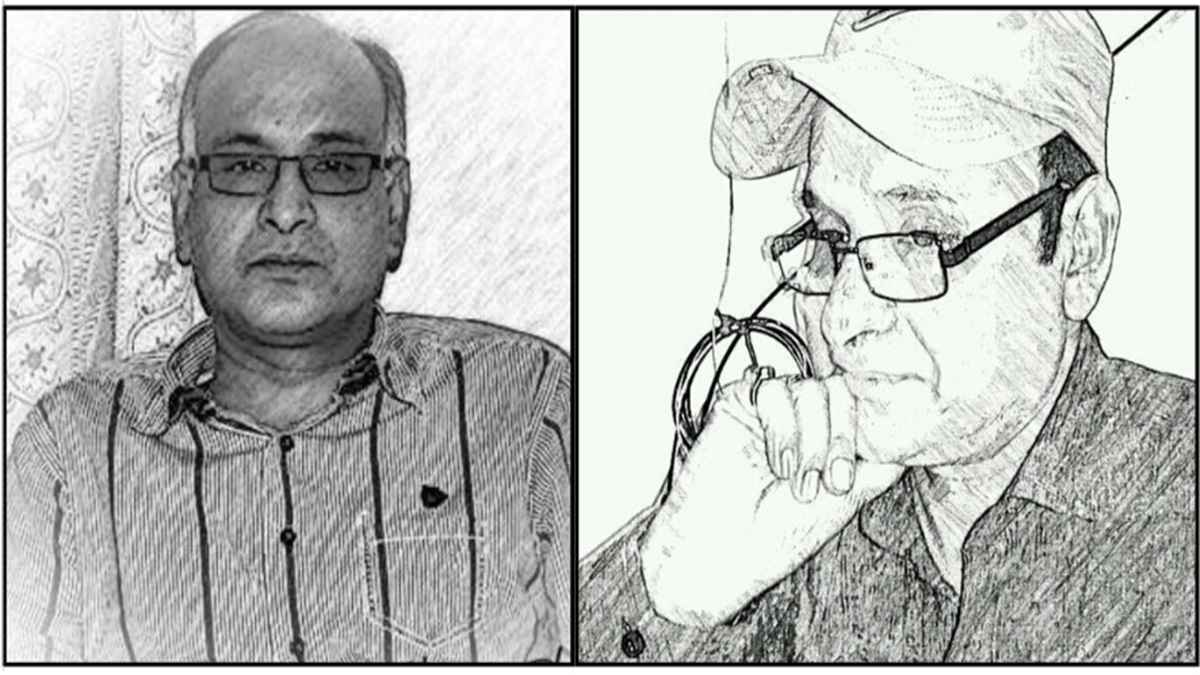
- August 26, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-18
नीत्शे, भेड़ें और एक अधूरा सवाल
8 जून, 2014
आज फिर नीत्शे की वह उक्ति याद आयी— “समाजवाद प्रगति की मृत्यु है।” कितना कठोर, कितना निर्मम वाक्य। जैसे कोई हँसते हुए कुल्हाड़ी से किसी सपने की जड़ काट रहा हो।
क्या वाक़ई समाजवाद भेड़ों का झुंड बना देता है? जहाँ सब एक जैसे चरते हैं, एक जैसे बैठते हैं, और कोई गड़रिया नहीं होता? या फिर यह नीत्शे का वह ‘अतिमानव’ का भूत है, जो हर झुंड को अपनी छाया से डराता है?
भारत में तो समाजवाद कभी लाल झंडे की तपिश नहीं रहा। यहाँ तो यह नीले आकाश के नीचे फैला एक खुला मैदान रहा है— जहाँ अंबेडकर की क़लम ने छुआछूत के ख़िलाफ़ संविधान की दीवार खड़ी की, जहाँ लोहिया ने ‘सप्तक्रांति’ के सपने बोये, और इंदिरा ने ‘ग़रीबी हटाओ’ का नारा दिया। क्या यह सब आलस्य था? या फिर उस भूखे भिखारी को रोटी देने की कोशिश, जिसे नीत्शे की दार्शनिक दृष्टि शायद नहीं देख पायी?
हाँ, यह सच है कि कभी-कभी यहाँ की राजनीति ने भेड़ों को “मुफ़्त के चारे” का आदी बनाया। वोट के लिए लुटाये गये लाभ, योजनाओं के नाम पर बँटते भ्रष्टाचार के टुकड़े… लेकिन क्या यह समाजवाद का दोष है, या फिर लूटने वाले गड़रियों की मंशा? नीत्शे शायद भूल गये कि भेड़ें भी कभी शेर बन सकती हैं। जब कोई दलित बच्चा आईएएस बनता है, कोई आदिवासी लड़की डॉक्टर बनती है— तो क्या यह समाजवाद की ही देन नहीं? या फिर नीत्शे के लिए ये सब भी “बिचौलियों की भीड़” में शामिल होगा?
शाम होते-होते एक बात समझ आयी— नीत्शे का डर यूरोप की दहशत थी, जहाँ समाजवाद ने कभी क्रांति के गिलोटिन चलाये। पर भारत का रास्ता अलग है। यहाँ समाजवाद नदी की धारा की तरह है— कभी तेज़, कभी धीमी, लेकिन हमेशा पत्थरों को घिसते हुए। आज रात चाँद निकलेगा, और शायद नीत्शे की ‘भेड़ें’ उसकी रोशनी में अपने पैरों के निशां तलाश करेंगी। पर मैं जानता हूँ— यहाँ कोई गड़रिया नहीं है, सिर्फ़ एक सामूहिक सपना है… जिसमें हर कोई अपनी राह ख़ुद बनाता है।
चारू छ और शहरनामा की प्रतीक्षा
सुधीर सक्सेना हिन्दी के उन थोड़े से मित्र कवियों में हैं– शुरू-शुरू में जिनकी किताबें हाथो-हाथ ख़रीदी जाती हैं। वे उन थोड़े से पत्रकारों में भी हैं, जिनकी रपटों में ख़बर नहीं, ख़बर का रस होता है — जैसे कोई आम के बाग़ से गुज़रते हुए पके फलों की मिठास हवा में पहचान ले। और वे उन बिरले मित्रों में हैं जिन्हें ‘दादा’ कहने में भी एक अजीब-सा इत्मीनान मिलता है, जैसे कोई पुराना राग अचानक गुनगुनाने को मन करे।
सुबह होते ही हमारी बात हो जाती है। कभी फ़ोन पर, कभी चैट पर, नहीं तो एसएमएस की संक्षिप्त लय में। लखनऊ की गलियों में जन्मे, रायपुर की धूप में पले, पर वे किसी एक शहर के नहीं। उनका तो पता ही कुछ यूँ है— “जहाँ आज रात गुज़रनी हो, वहीं का हूँ अभी।” शायद इसीलिए उनके शहरनामों में सिर्फ़ जगहें नहीं, जगहों की साँसें होती हैं।
हमारे बीच ‘हाय-हैलो’ नहीं चलता। बस एक ‘चारू छ’ ही काफ़ी है। यह शब्द उन्हीं की देन है— जैसे कोई यायावर रास्ते में मिले एक गुप्त मंत्र की सौगात दे जाये। मैं इसका इकलौता शागिर्द हूँ, पर अब आप भी इसे अपना सकते हैं। जैसे वे कहते हैं— “यूँ ही कोई मिल जाये रास्ते में
तो समझ लेना—चारू छ वही है”
आज ‘चारू छ’ के बाद पता चला— उनकी नयी किताब ‘शहरनामा’ ज़ल्द आ रही है। यह कोई साधारण यात्रा-वृत्तांत नहीं, बल्कि शहरों के साथ बिताये पलों का निचोड़ होगी। वैसे भी, जिसने इतने शहरों की धड़कन सुनी हो, उसकी क़लम से निकली बातें कैसे मामूली हो सकती हैं? शायद इसमें ‘चारू छ’ का रहस्य भी खुले— वह शब्द जो न मिलने का एहसास है, न बिछड़ने का दर्द, बस बीच का वह आसमान है जहाँ दो यात्री एक पल के लिए ठहर जाते हैं।
और हाँ, यह बताना भूल ही गया— वे रसरंजन के भी पुजारी हैं। चाय की चुस्कियों के बीच ग़ज़लों का ज़िक्र छिड़ते ही उनकी आँखों में एक चमक दौड़ जाती है। जैसे कोई बहता हुआ शेर उनकी ज़ुबान पर आ टिका हो—
“हम वही हैं जो बिखरते रहे शहर-ब-शहर
तुम वही हो जो समेटते रहे ख़्वाब हमारे”
अब बस इस किताब का इंतज़ार है। शायद इसमें वह शहर भी हो, जहाँ ‘चारू छ’ का जन्म हुआ, या वह मोड़ जहाँ दो यात्रियों ने इस शब्द को गढ़ा। पर इतना तय है— जैसे ही किताब हाथ लगेगी, पन्नों से शहरों की ख़ुशबू नहीं, बल्कि सुधीर दादा की वह हँसी निकलेगी जो हमेशा कहती है— “चारू छ, यार!”
लेखक या संत? एक अधूरा सवाल
कृष्ण बलदेव वैद (कहानी ‘लेखक की बद्दुआएँ’ में) कहते हैं: “यह भी तो सोचो कि एक लेखक होने के नाते तुम्हें हर क़िस्म के इंसान में, हर क़िस्म के अनुभव में, हर तरह की स्थिति में दिलचस्पी होनी चाहिए, प्रूस्त को थी, बाल्ज़ाक को थी और इस क़िस्म के आदमी में तो ख़ास तौर पर क्योंकि तुम चाहो तो इसके माध्यम से सारे राजनैतिक दाँव-पेंच और माफ़ियाई दुनिया को क़रीब से जान सकते हो।
अगर तुम ऐसे संबंधों से कोई निजी फ़ायदा नहीं उठाना जानते हो तो तुम्हें मजबूर कौन कर सकता है। …अपने अनुभव का विस्तार करना सीखो। तुम लेखक हो, संत नहीं। तुम्हारी नैतिकता संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई अनुभव वर्जित नहीं, कोई इंसान वर्जित नहीं..।”
वैद साहब की बात सुनकर लगता है, जैसे कोई पुराना दरवाज़ा खुल गया हो— वह दरवाज़ा जिस पर “अनुभवों की दुनिया” लिखा था, और जिसके पार खड़ा था एक लेखक, अपनी नैतिकताओं से जूझता हुआ। क्या सचमुच एक लेखक के लिए कोई अनुभव वर्जित नहीं? क्या वह ‘माफ़ियाई दुनिया’ में घुसकर भी निर्मल बना रह सकता है? या फिर यह सब एक भ्रम है — जैसे कोई आग में हाथ डालकर यह सोचे कि वह जल नहीं सकता?
प्रूस्त ने मेडलीन के स्वाद में पूरी याददाश्त खोज डाली। बाल्ज़ाक ने पेरिस के गलियारों में पैसों की बदबू सूँघी। पर क्या वे नैतिक थे? या सिर्फ़ जिज्ञासु? मैं सोचता हूँ— शायद लेखक की नैतिकता यही है कि वह किसी भी अनुभव से डरे नहीं। पर साथ ही, वह किसी भी अनुभव का ग़ुलाम भी न बने। वह नदी की तरह हो— जो गंदे नालों के पानी को भी अपने में समेट ले, मगर ख़ुद साफ़ बहती रहे।
लेकिन यहाँ एक दिक़्क़त है— क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं ‘माफ़िया’ से हाथ मिलाकर भी अपनी क़लम को बेचने नहीं दूँगा? क्या मैं राजनीति के दाँव-पेंच देखकर भी सिर्फ़ दर्शक बना रह सकता हूँ? या फिर एक दिन मैं भी उसी खेल का हिस्सा बन जाऊँगा— बस इस बहाने कि “मैं तो सिर्फ़ अनुभव ले रहा हूँ”?
वैद साहब कहते हैं— “तुम लेखक हो, संत नहीं।” ठीक है। मगर क्या लेखक का धर्म सिर्फ़ देखना है? या देखकर कुछ कहना भी? शायद इसका जवाब यह है कि लेखक बदल सकता है, पर बिकना नहीं चाहिए। वह हर आदमी से मिले, मगर हर आदमी की तरह न बने। वह हर अनुभव को छुए, पर हर अनुभव में न घुल जाये। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता— अगर मैं ‘माफ़िया’ की दुनिया में जाकर माफ़िया ही बन जाता हूँ— तो फिर मेरी क़लम किस काम की? शायद इसीलिए लेखक का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, ख़ुद से होता है।
9 जून, 2014
मेरी एक ही चिड़िया : चिड़िया की कई चिड़िया
मेरी एक ही बिटिया। यानी एक ही चिड़िया। उसकी अपनी कई चिड़ियाँ। कई सहेलियाँ। मैं अपनी चिड़िया को रोज़ दाना-पानी देता हूँ और वह रोज़ अपनी चिड़ियों को। जाने कहाँ से ये सारी चिड़ियाँ उसकी कमरे की खिड़की पर रोज़ पानी पीने, दाना चुगने चली आती हैं।
वे चली आती हैं कि मेरी चिड़िया को चिड़िया की उड़ान सिखा सकें। आकाश की ऊँचाई का नाप-जोख सिखा सकें। चोंच भर पानी में ज़िंदगी की प्यास बुझाने की कथा सुना सकें। कोयल, कबूतर, पंछी, मैना, फूलचुहकी… सब अलग-अलग होकर भी एक साथ एक ही आकाश में एक ही राग का गीत गुनगुना सकती हैं।
मुझे लगता है मैं एक चिड़िया का नहीं, कई चिड़ियों का पिता हूँ। मैं इस तपिश और सुनसान दोपहर वाले शहर में अकेला कहाँ हूँ? सारा संसार है मेरे पास। पूरा भरा-पूरा चहचहाता घर-परिवार। आभार मेरी चिड़िया (प्रगति, मेरी बिटिया) और उसकी सभी सहेली चिड़ियों का भी! रोज़ आना मेरे घर। उड़कर न जाना कभी… कहीं मुझे, इस घर को, इस खिड़की को छोड़कर…
10 जून 2014
कवि क्यों मृत्यु वरे?
आज ही ‘सतह के नीचे’ मुझ तक पहुँची। बल्कि, वह नहीं पहुँची, मैं उस तक पहुँचा। जैसे एक रेतीला मनुष्य जाकर शीतल और शांत जल से लबालब किसी गहरे पोखर तक पहुँचता है। यह हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि-आलोचक और मार्गदर्शक रचनाकार विजेन्द्र जी की अनमोल कृति है।
मार्गदर्शक इसलिए भी कि वे उम्र के आठवें दशक में भी देह की तमाम सीमाओं को धता बताते हुए कवियों की नयी पीढ़ी को समय, संस्कृति और विशेषतः कविता का निःशुल्क पाठ पढ़ा रहे हैं, अनवरत और व्यावहारिक। विश्वास नहीं, तो आप स्वयं फ़ेसबुक पर स्थापित और संचालित उनके आश्रम में शिष्य-भाव से प्रवेश ले सकते हैं।
मुझे नहीं पता कि निराला, नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल प्रभृति हमारे युग-कवि यदि आज होते, तो क्या वे विजेन्द्र जी की भाँति स्वतःस्फूर्त होकर नवागत कवियों को इतना वक़्त दे पाते क्योंकि वे बहुत-से महान् कवि, जो इस परंपरा में आज भले ही अपने आपको अग्रगण्य घोषित करते-करवाते फिरते हैं, उनके नाम और धाम का आतंक एक युवा रचनाकार को उनसे बहुत विलग कर देता है। विजेन्द्र जी का कवियों की युवा पीढ़ी पर यह अहैतुकी प्रीति एक नये इतिहास जैसी ही है। फ़ेसबुक पर उनकी सक्रियता काव्य-लेखन और अध्ययन के प्रति निष्ठावान विद्यार्थियों के लिए ऋषि-आश्रम के नये अभिकल्प जैसी है।
तो ‘सतह के नीचे’ मात्र एक बड़े कवि की डायरी ही नहीं, कविता पर आस्था रखने वाले मुझ जैसे हर काव्य-समर्थक के लिए काव्य-शास्त्र की एक अत्यंत ज़रूरी किताब है। उनके लिए भी, जो अपने आपको ‘सतह के ऊपर’ मानने का भ्रम पाले बैठे हैं, लगभग ऐंठे हुए।
फ़िलहाल, डायरी के भीतरी पृष्ठों में प्रवेश करने या इस किताब के बारे में आपसे कुछ और बात करने से पहले ही उनकी इस कविता की आभा में मैं इतना रससिक्त हो उठा हूँ कि लगभग मौन, किंतु ऊर्जा से परिपूर्ण:
लगता है पात झरे
देख-देख दुख आस-पास आँख भरे
हैं अभी सूर्य, चन्द्र, नभ, जल, फूल और रज
कवि क्यों मृत्यु वरे।
रचना : अकेलेपन का साझा विज्ञान
कवि अकेला बैठा है। मेज़ पर रखा काग़ज़ भी अकेला है। दोनों के बीच एक खालीपन है जिसमें शब्द तैरते हैं। पाठक अकेला बैठा है। किताब खुली है। दोनों के बीच एक खालीपन है जिसमें अर्थ तैरते हैं।
यह खालीपन ही रचना है।
अकेलेपन का गणित
जब कवि लिखता है तो वह सिर्फ़ क़लम नहीं चलाता। वह अपने मन के अंदर उतरता है— जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से सेल की दरारें गिनता हो। हर शब्द एक प्रयोग है। हर पंक्ति एक हाइपोथीसिस। पाठक जब पढ़ता है तो वह सिर्फ़ आँखें नहीं घुमाता। वह कवि के माइक्रोस्कोप में झाँकता है— पर वहाँ कुछ और ही दिखता है। क्या यह ग़लती है? नहीं, यह विज्ञान है।
मनोविज्ञान की प्रयोगशाला
कविता दरअसल कहीं नहीं होती। न कवि के दिमाग़ में, न काग़ज़ पर, न पाठक की समझ में। वह इन सबके बीच की जगह में होती है— जैसे दो आँखों के बीच का वह बिंदु जहाँ त्रिआयामी दृष्टि बनती है। कवि का अकेलापन और पाठक का अकेलापन जब मिलते हैं तो यह तीसरी चीज़ पैदा होती है। इसे हम ‘रचना’ कहते हैं।
शून्य का सिद्धांत
एक प्रयोग करें:
1. कवि ने लिखा – “चाँद टूट गया है।”
2. पाठक ने पढ़ा – “चाँद टूट गया है?”
क्या यह एक ही वाक्य है? हाँ और नहीं। कवि के यहाँ यह एक तथ्य था। पाठक के यहाँ यह एक सवाल बन गया। बीच में जो अंतर है, वही कविता का घर है।
निष्कर्ष : अकेलेपन की भौतिकी
रचना का कोई एक स्थान नहीं होता। वह हमेशा दो जगहों के बीच होती है:
• कवि की निजता और पाठक की अपेक्षा के बीच
• लिखे गये शब्द और पढ़े गये अर्थ के बीच
• स्मृति और कल्पना के बीच
इसलिए कविता हमेशा अकेली ही रहती है— वह कभी कवि की नहीं होती, न पाठक की। वह उस जगह की है, जहाँ दो अकेलेपन मिलते हैं।
क्रमश:
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

