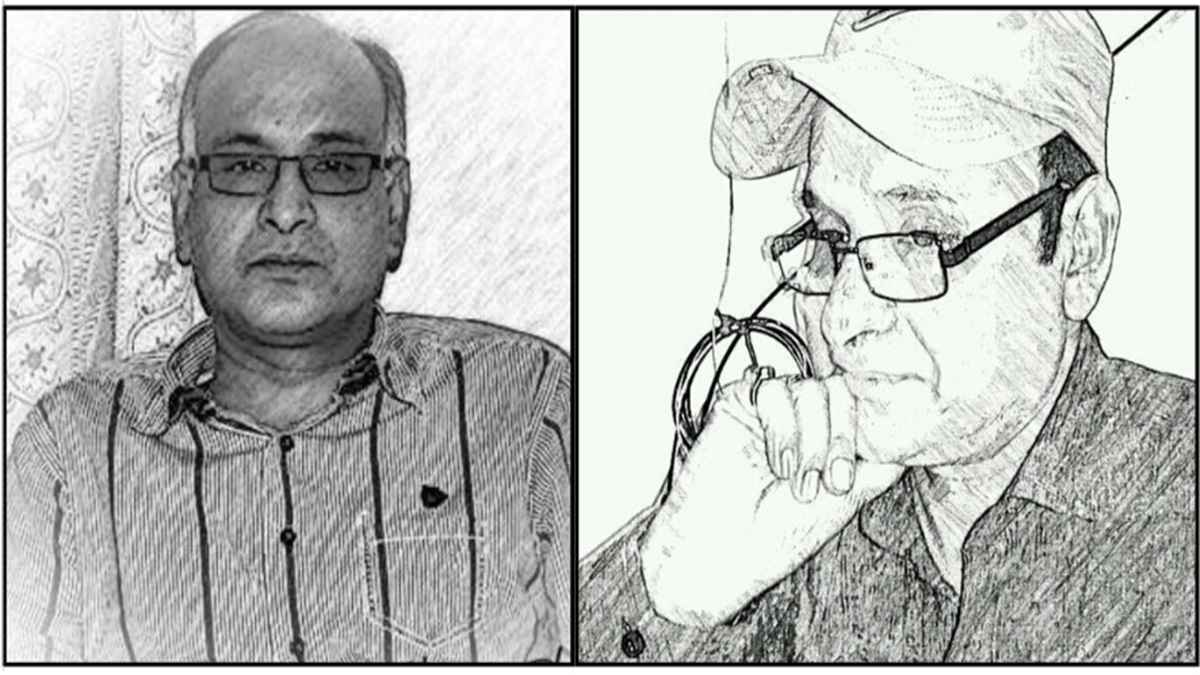
- August 12, 2025
- आब-ओ-हवा
- 1
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-14
कोई दूसरा नहीं होता
16 अप्रैल, 2014
कबीर साहेब के साथ कई चेले रहते थे पर कोई दूसरा कबीर नहीं बन सका।
मीरा की अनेक सहेलियाँ थीं पर मीरा एक ही रहीं।
तुलसीदास के साथ हुजूम उमड़ता रहा पर दूसरा ‘राम चरित मानस’ कोई नहीं रच पाया। ‘मार्क्स मार्क्स’ चिल्लाते रहने वालों में से कोई मार्क्स बन पाया क्या?
अब के महान् लोगों का नाम आप ही धर लें और देख लें- क्या कोई है, जो उनके जैसा साँस लेता हो? नहीं न?
नहीं ना तो फिर आप ख़ुद तय कर लें आप कौन हैं, क्या है? और कुछ हैं भी या कुछ भी नहीं? यदि आप कुछ भी नहीं हैं तो फिर किस उन्माद में हैं कि कोई आप जैसा भी हो? तो फिर तुम कौन हो? क्या हो? कुछ हो या बस हवा में उड़ते धुएँ का गुबार? अगर कुछ भी नहीं, तो ये कैसा बुख़ार कि कोई तुम जैसा हो जाये? सच तो ये है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी छाया, सिर्फ़ तुममें ही बसती है। तुम्हारा होना अपने आप में एक अनोखा घर है। किसी और जैसा हो जाना, अपने इस घर को उजाड़ देना है।
सच तो यही कि आप के जैसा कोई दूसरा नहीं। आपका बिम्ब सिर्फ़ आप से मिलता है। आपका होना सबसे मौलिक होना है। किसी और जैसा हो जाना अपनी समूचे अस्तित्व को ख़ारिज कर देना है। अपनी छवि को बरक़रार रखना सबसे सच्चा जीवन जीना है। अनुकरण एक खोखली चाल है। और अनुकरण अशुद्ध क्रिया है।
हवा से कहो कि पानी बन जाये, या आकाश को समझाओ कि धरती हो सकता है- ये सब मन का धोखा है, एक फीका सपना। प्रकृति की किताब देखो, एक पेड़ की सारी पत्तियाँ अलग-अलग रंग लिये खड़ी हैं। हर तारा अपनी रोशनी में टिमटिमाता है। भिन्नता ही तो असली बात है। अपने रंग में रहो, अपनी छाया को थामे रखो। वही जीना है। वही तुम हो।
प्रकृति भी कहती है यही: किसी एक पेड़ की सारी पत्तियाँ रूप-रंग से भिन्न होती हैं। भिन्नता मौलिकता का ही मानी है। भिन्न रहिए- मौलिक कहलाएंगे!
17 अप्रैल, 2014
पाठक के क़रीबी
कुछ समीक्षक प्रकाशक के क़रीबी होते हैं, कुछ लेखक के क़रीबी, कुछ लेखन के क़रीबी, कुछ गुट के क़रीबी, कुछ गिफ़्ट के क़रीबी। जो इनमें से किसी के क़रीबी नहीं होते हैं- क्या वे पाठक के क़रीबी होते हैं?
19 अप्रैल, 2014
आभी का तिनका: झील की कहानी
पिछले सात दिन से मन में एक चिड़िया उड़ रही है। छोटी-सी, हल्की-सी, जैसे कोई अनजाना गीत जो सुना तो नहीं, पर गुनगुनाया जा रहा है। वह मेरे भीतर कहीं बैठी है, मेरी आत्मा की डाल पर, और उसकी चोंच में एक तिनका है। तिनका नहीं, शायद एक झील का सारा पानी, साफ़, चमकता, जैसे कोई शीशा जो टूटने से पहले हँसता हो।
मैं सोचता हूँ, यह चिड़िया कौन है? कहीं मेरे बचपन की वन-सखा तो नहीं, जो ताल-तलैया के किनारे मेरे साथ दौड़ती थी? या कोई अनजान परीक्षा, जो मेरे मन को टटोल रही है? नहीं, नहीं, मेरा मन कहता है, यह चिड़िया थकी है। उसकी आँखों में आँसू की काली पपड़ी है, उसकी चोंच में तिनके का बोझ। वह क्लांत है, पर रुकती नहीं। वह आभी है।
आभी, जो सरेऊलसर झील की रखवाली करती है। कुल्लू की उस ऊँचाई पर, जहाँ हवा ठंडी है और पेड़ चुपचाप तप करते हैं। 11,500 फीट ऊपर, जहाँ बूढ़ी नागिन माँ का मंदिर है, और झील का पानी इतना साफ़ कि उसमें आसमान की परछाईं डूबती है। आभी वहाँ रहती है। वह झील में एक तिनका भी नहीं पड़ने देती। हवा का झोंका पत्ता लाये, पर्यटक कोई कचरा फेंके, या जंगल से कोई सूखी टहनी गिरे- आभी अपनी चोंच में उसे उठाकर किनारे रख देती है। जैसे कोई बच्चा अपनी किताब पर धूल न जमने दे।
मैं आभी को देखता हूँ। वह छोटी-सी है, पर उसका काम बड़ा है। वह झील को पानी की तरह रखना चाहती है- पानी, जो पानी हो, न गंदला, न गंधला। वह हवा से लड़ती है, पेड़ों से बात करती है, पर्यटकों की लापरवाही से जूझती है। लोग नहीं जानते। वे मैदानों से कचरा लाते हैं, और झील में फेंक देते हैं। वे नहीं देखते देवदार की तपस्या, बुरांश के फूलों की लाल सुगंध। वे नहीं सुनते हवा की ताज़गी, जो आभी की साँस में बसी है।
आभी छह महीने सूरज से सूरज तक व्यस्त रहती है। जब बर्फ़ आती है, झील जम जाती है। तब आभी को तीन महीने का आराम मिलता है। वह कहीं चली जाती है, शायद किसी और झील की तलाश में, या शायद मेरे मन में उड़ते-उड़ते आ बैठती है। मैं उससे पूछता हूँ, “आभी, तुम इतना क्यों करती हो?” वह चुप रहती है। उसकी चोंच में तिनका है, और आँखों में झील।
मैं सोचता हूँ, यह दुनिया कितनी अजीब है। लोग पर्यावरण की बात करते हैं, बड़े-बड़े शब्दों में। पर आभी? वह तो बस एक चिड़िया है। न स्वार्थ, न प्रलोभन। वह झील को साफ़ रखती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का चेहरा साफ़ करती है। वह तिनके उठाती है, और मेरे मन में एक गीत छोड़ जाती है।
कभी-कभी मैं उस पोटली को देखता हूँ, जो हरनोट जी ने भेजी है। ‘लिटन ब्लॉक गिर रहा है’ लिखा है उस पर। पर मैं पोटली नहीं खोलता। मैं आभी से बात करता हूँ। वह कहती है, “पानी को पानी रहने दे। हवा को हवा।” और मैं सुनता हूँ, जैसे कोई पुराना दोस्त अपनी पुरानी बात कह रहा हो।
आरम्भ आरोह चरम स्थिति अवरोह या अंत
आज की यथार्थवादी कहानी, जैसे कोई सादा-सी नदी, अपने किनारों को छूती हुई बहती है- वह यथार्थ को केवल देखती नहीं, बल्कि उसे कोमलता से गढ़ती है, ताकि वह और सुंदर, और जीवंत हो सके। यह कहानी कभी निरुद्देश्य नहीं होती; यह एक बच्चे की तरह जिज्ञासु, एक बूढ़े की तरह अनुभवी, और एक कवि की तरह संवेदनशील होती है। यह उन सारे सिद्धांतों-कलावाद, आधुनिकतावाद, उत्तर-आधुनिकतावाद- को हल्के से मुस्कुराकर टाल देती है, जो यथार्थ को केवल ‘जो है’ तक सीमित करते हैं। यह कहती है, ‘जो होना चाहिए, जो हो सकता है, वही असल यथार्थ है।’
आज का कहानीकार, जैसे कोई गाँव का कारीगर, जो मिट्टी से बर्तन गढ़ता है, भूमंडलीय यथार्थ को उसी तरह बुनता है। वह जानता है कि एक गाँव का यथार्थ और सारी दुनिया का यथार्थ एक ही मिट्टी से बना है। गाँव को सुंदर बनाने के लिए दुनिया को सुंदर बनाना होगा, जैसे एक फूल को खिलाने के लिए सारी बगिया को सींचना पड़ता है। यह नया यथार्थवाद है- भूमंडलीय, फिर भी उतना ही नाज़ुक, जितना एक पत्ते पर ठहरा हुआ ओस का क़तरा। यह कहता है: ग़रीबी, भूख, लाचारी को मिटाना है- हर उस कोने से, जहाँ आदमी की साँस चलती है।
इस यथार्थवाद में ‘जो है’ के साथ-साथ ‘जो हो सकता है’ भी उतना ही सच है। यह कहानी दो नन्हे पंखों पर उड़ती है: एक, कि दुनिया को सुंदर बनाना चाहिए; और दूसरा, कि दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है। कोई इसे दिवास्वप्न कह सकता है, कोई इसे प्रेमचंद का ‘आदर्शोन्मुख यथार्थवाद’ कहकर पुराना ठहरा सकता है। पर यह कहानी उस बच्चे की तरह है, जो पत्थर को देखकर उसमें छिपी मूर्ति देख लेता है। यह उस पारस पत्थर की तलाश नहीं, जो काल्पनिक है, बल्कि उस संवेदना की तलाश है, जो हर दिल में कहीं न कहीं बसती है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कविता सुनने वाला ‘ज़रा फिर से कहिए’ कहता है, और कहानी सुनने वाला पूछता है, ‘हाँ, तब क्या हुआ?’ कविता, जैसे कोई तितली, अपने रंगों में खो देती है; पर कहानी, जैसे कोई रास्ता, चलते हुए अपने अंत तक ले जाती है। कहानी का श्रोता, जैसे कोई प्यासा यात्री, तब तक संतुष्ट नहीं होता, जब तक वह पूरी कहानी न सुन ले- वह कहानी, जो उसके जीवन की उलझन को छू ले, और उसे सुलझाने का रास्ता दिखा दे। यह मुकम्मल कहानी वही है, जो किसी गाँव के दुख को, या सारी दुनिया की पीड़ा को, अपनी गोद में लेकर उसे सँवार देती है।
दोस्तोएव्स्की ने कहा था : ‘सुंदरता ही दुनिया को बचाएगी।’
सुंदरता, जैसे कोई नन्हा दीया, जो तूफान में भी टिमटिमाता है। कहानीकार की संवेदना, जैसे वह हवा, जो इस दीये को बुझने नहीं देती। वह दुनिया की क्रूरता, हिंसा और ठंडेपन के बीच से अपनी राह बनाता है, जैसे कोई नदी पत्थरों को चीरकर बहती है। विनोद कुमार शुक्ल की तरह, वह सादगी को अपनी ताक़त बनाता है- वह हर उस छोटे-से पल में, हर उस साधारण चीज़ में, सुंदरता और संवेदना ढूँढ़ लेता है। उसकी कहानी, जैसे कोई पुरानी चिट्ठी, जो पढ़ते ही दिल को छू लेती है, हमें याद दिलाती है: जब तक संवेदना है, तब तक कहानी है; और जब तक कहानी है, तब तक दुनिया को सुंदर बनाने का सपना ज़िंदा है।
22 अप्रैल, 2014
स्वगत
जैसे कोई नदी किनारे पर ठहरकर ख़ुद से बात करती है, वैसे ही हम दोनों हैं- न तुम्हें मुझसे कुछ कहना बाक़ी है, न मुझे तुमसे कुछ सुनना। न मैं तुम्हें छूकर तुम्हारा सच जान सकता हूँ, न तुम मेरे भीतर की हवा को पकड़ सकते हो। हम दोनों, जैसे दो पेड़, अपनी-अपनी जगह खड़े हैं, हवा में हिलते हुए, अपनी पत्तियों की सरसराहट में ही समझदार।
समझदारी शायद यही है- न कोई किसी को समझने की ज़िद करे, न कोई किसी को समझाने की। जैसे कोई बच्चा, जो पत्थर को उठाकर सिर्फ़ उसका वज़न महसूस करता है, बिना यह पूछे कि वह पत्थर कहाँ से आया। हम भी, अपने-अपने भीतर की सैर करते रहें, अपने ही सवालों के जवाब ढूँढते रहें। क्या यही समझ है? शायद, जैसे कोई पुराना गीत, जो बिना मतलब के भी कानों में गूँजता रहता है, और फिर भी सब कुछ कह देता है।
24 अप्रैल 2014
मेहनत को बधाई
जैसे कोई नन्हा बीज, मिट्टी के भीतर धीरे-धीरे अपनी जड़ें फैलाता है, वैसे ही प्रशांत की मेहनत ने आज एक छोटा-सा अंकुर फोड़ा है। एनआईटी, रायपुर की राहों से, जहाँ किताबों की स्याही और सपनों की चमक एक-दूसरे से बातें करते हैं, वह ग्लोबल कंपनी वेदांता/स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की छाँव में पहुँचा है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में, जैसे कोई नदी किनारे की मिट्टी को छूकर आगे बढ़ती है, उसने अपनी पहली मंज़िल पा ली।
यह सफलता, जैसे सुबह की ओस, जो पत्ते पर ठहरकर सूरज की किरण में चमकती है। यह उसकी मेहनत का दीया है, जो रात की गहरी चुप्पी में भी टिमटिमाता रहा।
जैसे कोई पुराना रेडियो, जो बरसों बाद भी साफ़ स्वर में गीत गाता है, वैसे ही प्रशांत का यह क़दम, छोटा-सा, पर अपने आप में एक पूरी धुन है। बधाई उसकी मेहनत को, जो पत्थर में भी फूल उगा देती है, और उसकी हिम्मत को, जो आसमान की ओर देखकर कहती है- अभी तो बस शुरूआत है।
बदल गयी घड़ी!
दुकालू यादव। हमारा गोरसवाला। 13 किमी दूर देहात से आता है। चौथी तक पढ़ा-लिखा। ये आ गया तो समझो दिन के 2 बज रहे हैं। बिलकुल घड़ी मिला लें! आश्चर्य!
“आज कइसे साढ़े बारह बजे दू बजा देहे दुकालू!”
“वा, आज जल्दी गोरस बाँट के बोट देहे बर जाना हे न गा!”
खुली आँखों का समय
कविता, जब खुली आँखों से समय को देखती है, तो वह न केवल अपने समय की साँस को पकड़ती है, बल्कि हर समय की धड़कन बन जाती है। वह सामयिकता का आलिंगन करती है, पर उससे बँधी नहीं रहती। वह वर्तमान को उसके अतीत की छायाओं और भविष्य की आहटों के साथ पढ़ती है, जैसे कोई पुराना पत्र, जो आज भी उतना ही जीवंत है। कवि, अपनी सारी प्रतिबद्धता और निजी सरोकारों को थामे, फिर भी समय को एक तटस्थ लेकिन संवेदनशील नज़र से देखता है। यह दृष्टि, जैसे कोई साफ़ झील, जिसमें सारा आकाश झलकता है, कविता को सार्वभौम और सदा प्रासंगिक बनाती है।
ऐसी कविता का धर्म है कि वह सबसे कमज़ोर, सबसे आहत, सबसे निर्दोष मनुष्य की आवाज़ बने। वह उसका पक्ष लेती है, जो समय के हाशिये पर धकेल दिया गया है। वह सिर्फ़ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है- उस मनुष्य के प्रति, जिसका दुख कविता के बाहर भी उतना ही वास्तविक है।
1987 में लिखी गयी मदन कश्यप की कविता ‘हत्यारों के दोस्त’ आज भी मेरे सामने है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर, जिसमें रंग फीके नहीं पड़े। वह कविता, ‘लेकिन उदास है पृथ्वी’ में संग्रहीत, तब के किसी अनाम दर्द से उपजी थी। आज वह बस्तर के ज़ख़्मों में, या दुनिया के किसी और कोने की चीख में, उतनी ही सटीक लगती है। कवि शायद उस भूगोल में नहीं था, शायद आज भी नहीं है, पर उसकी कविता वहाँ है- मुकम्मल, साफ़, और तीखी। वह कहती है:
हत्यारों के दोस्त बनोगे
वे तुम्हें रक्तपिपासु बनाएंगे
अभियान में ले जाएंगे
मरना सिखाएंगे
परन्तु यह भी कि अगर कहीं
हताहत हो रहे लोगों ने दबोच लिया तुम्हें
तो वे साथ छोड़कर भाग जाएंगे
क्योंकि हत्यारे सिर्फ़ मारना जानते हैं!
यह कविता आज भी चेतावनी है, जैसे कोई दीया जो अंधेरे में टिमटिमाता है। यह हमें याद दिलाती है कि कविता का काम सिर्फ़ देखना नहीं, बल्कि उस देखे हुए को एक ऐसी आग में बदलना है, जो मनुष्यता को झकझोर दे। यह कविता, और ऐसी हर कविता, समय के पार जाकर भी समय की सच्चाई को पकड़े रहती है क्योंकि उसकी आँखें खुली हैं, और उसका दिल धड़कता है।
अपने-अपने देवता
ऐसा कौन है जो किसी-न-किसी देवता का पुजारी न हो? कोई गाँधी को माथे पर चढ़ाये घूमता है, कोई मार्क्स की किताबों में अपनी दुनिया का सच ढूँढता है। किसी का देवता पत्थर में बसता है, ठंडा, चुप, सदियों से एक ही जगह टिका। किसी का पानी में तैरता है, लहरों की तरह बेपरवाह, हर बार छूने पर नया। कोई गूँगे देवता को पूजता है, जो बोलता नहीं, सिर्फ़ सुनता है। और कोई बड़बोले की भक्ति में डूबा है, जो हर सवाल का जवाब चीख-चीखकर देता है। कोई शाकाहारी भगवान को हरसिंगार के फूल चढ़ाता है, तो कोई माँसाहारी देवता के सामने बलि का ख़ून बहाता है। कोई शांत देवता की छाया में सुकून पाता है, तो कोई गुस्सैल भगवान की आग में अपनी बेचैनी जलाता है।
ये देवता हमारे भीतर के ख़ालीपन को भरते हैं। या शायद हम ही उन्हें गढ़ते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। बचपन में माँ और मेरी मामा (मझली माँ) की गोद में बैठकर सुनी माँ मंगला की कहानियाँ आज भी कहीं गहरे में बसी हैं। हर साल मंगलाष्टमी पर घर में छोटा-सा पंडाल सजता था। पिताजी लकड़ी के चौकी पर मंगला-स्तुति रखते, और मैं, नन्हा-सा, उनके पीछे बैठकर घंटियों की आवाज़ में खो जाता। वो माँ मंगला मेरा पहला देवता (देवी) थी- माँ की तरह सौम्य, क्षमावान, किन्तु गर्व कतई न सहने वाली – ऐसा जो मेरी ग़लतियों को भी मुस्कुराकर माफ़ कर दे। लेकिन फिर समय बदला। कॉलेज के दिनों में दोस्तों की बहसों में, किताबों के पन्नों में, एक नया देवता मिला- चेतना का, विद्रोह का। वो गाँधी नहीं, मार्क्स नहीं, बल्कि मेरे अपने सवालों का देवता था।
मैं भी इन देवताओं को देखता हूँ। उनके लेखन में एक ठहराव है, एक ऐसी नज़र जो रोज़मर्रा की सतह को छीलकर उसके नीचे की सच्चाई को छू लेती है। कवि की कविताएँ जैसे मेरे गाँव की उस मिट्टी की बात करती हैं, जहाँ मैं नंगे पाँव दौड़ा करता था। वहाँ एक पुराना बरगद था, जिसके नीचे गाँववाले अपने देवताओं को बुलाते थे। कोई हनुमान को, कोई शीतला माता को। मैं सोचता हूँ, क्या ये देवता सचमुच अलग-अलग हैं? या ये बस हमारे मन के रंग हैं, जो हर किसी के लिए अलग चमकते हैं?
आज भी, जब शहर की भागदौड़ में साँस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, मैं अपने देवता को ढूँढता हूँ। कभी माँ के पुराने पत्रों में, जो अब भी उनकी हस्तलिपि की गंध से भरे हैं। कभी उस दोस्त की हँसी में, जो बरसों बाद मिलने पर भी वही पुरानी बातें छेड़ देता है। शायद मेरा देवता कोई एक नहीं। शायद वो हर उस लम्हे में बिखरा है, जो मुझे मेरे होने का एहसास दिलाता है।
तो आपका देवता कौन है? क्या वो भी आपके बचपन की किसी स्मृति में छिपा है? या वो आपके आज के सवालों में उलझा है, जवाब की तलाश में?
कवि का द्वैत
हिंदी में कुछ कविता-प्रेमी कवि ऐसे भी हैं, जो अपने कवि-मित्रों की श्रेष्ठ कविताओं को फूटी आँख देखना-पढ़ना पसंद नहीं करते पर उनसे ही अपनी साधारण कविता को श्रेष्ठ घोषित करवाने के लिए पलक पाँवड़े बिछाये रहते हैं।
भाषा का पानी
दुनिया : एक बंजर खेत
खेत का कृषक : कवि
कवि का कुँआ : भाषा
भाषा का पानी : कविता
क्रमश:

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky


इसे पढ़ना अपने आप में अलग अनुभव है। धन्यवाद।