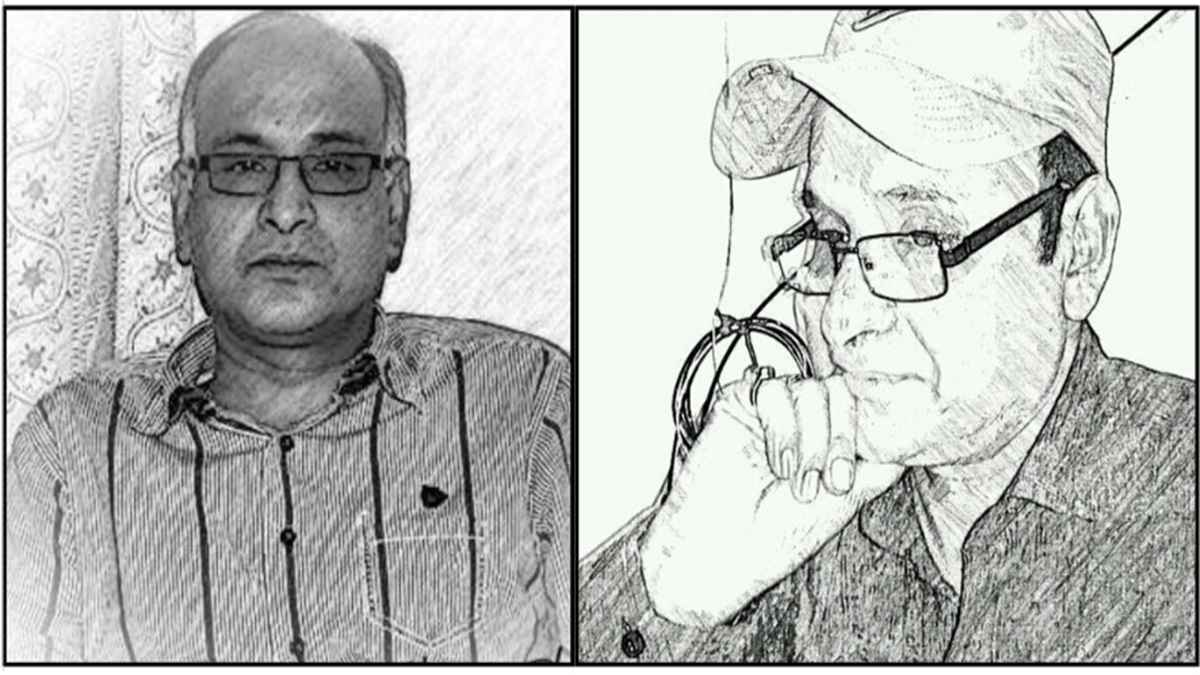
- August 19, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-16
माटी की सिपाही: चींटियाँ
28 मई 2014
चींटियाँ धरती की सबसे बड़ी सफ़ाई कामगार हैं। माटी की सिपाही। नमक, गुड़, मिठाई, या गोरस— जो कुछ भी खुला छूट जाये, वे एक दिन उसे चट कर जाती हैं। उनका काम है धरती पर बिखरे अकारज को साफ़ करना। वह सब, जो संभाला न जाये, जो कहीं भी बेतरतीब पड़ा हो। जैसे कंजूस की तिजोरी में उदास पड़ा धन, जो न स्वयं के काम आये, न दूसरों का भला करे।
चींटियों को व्यर्थ कुछ भी रुचता नहीं। वे न रोकती हैं, न टोकती। बस, चिढ़ती हैं कि इतना क्यों इकट्ठा किया, जो न तुम्हारे काम आये, न दूसरों को सुख दे। लघु जीव हैं चींटियाँ, पर उनकी शक्ति असीम। उनके दाँत हमारी लोभ और लाभ की नुकीली डाढ़ों से भी तेज़। वे जड़ से फूल तक, सब कुछ चाट जाती हैं। पर्वत को भी हज़म कर लेंगी।
चींटियों की पहुँच अनंत है। वे हमसे पहले थीं, और हमारे सौ-सौ जन्मों के बाद भी रहेंगी। माटी के भीतर, माटी के संसार में। व्यर्थ को माटी में बदलती रहेंगी।
उन्हें ऊँची आवाज़ पसंद नहीं। न ही किसी की गरमी बर्दाश्त। पर प्यार से स्पर्श करो, तो लजा जाती हैं। मन ही मन गुनगुनाती हैं, जैसे कह रही हों— प्यार एक मौन गीत है, बेआवाज़ संगीत है। माटी की चींटियाँ हमारे सपनों को भी लपक लें, इससे पहले अपनी नींदों को सहेज लें, समेट लें। फिर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं।
29 मई 2014
सुबह: भाषा का सबसे बड़ा शब्द
सुबह भाषा का सबसे बड़ा शब्द है। एक उदास रात के शोर का अंत, मुस्कान का भोर। उदासी आख़िरी पहर का आचरण है। उदासी में भटकना, उसमें अलसाना, सुबह का संकेत है। सुबह नींद के बाद का अनिवार्य विस्तार है। स्वप्न का आकार। घनी विश्रांति का उपरांत। धरती का सर्वश्रेष्ठ प्रांत। उसकी पहली पहचान है अथाह शांति। यह शांति क्रांति का पहला चरण है। शांति के बिना हर क्रांति अनाहूत मरण है, अनर्थ है। सुबह न केवल शब्द है, बल्कि व्याकरण का सबसे गहन अर्थ है।
परभाती खग-वृंद रात भर उदास घोसलों में कलपते नहीं। वे सोते हैं, मन भर उदास। उदासी तड़पने से नहीं कटती, सुबकने से नहीं मिटती। नींद उदासी की काट है। स्वप्न उजाले का मार्ग है।
उदासी कोई अपरिचित पहाड़ नहीं। वह मुरझाया-सा, पथराया-सा बरसाती नाला है। वेग से आता है, और जाने कहाँ चला जाता है। नाला कभी नदी नहीं बनता। वह क्षणिक है, सदी नहीं। न उज्ज्वल, न धवल। चपल है, पर कमल उसमें नहीं खिलता। नाले की उपस्थिति जीर्ण-शीर्ण है, अवशिष्ट की अनुपस्थिति। यह अनुपस्थिति ज़रूरत है, हकीकत है, नयी सृष्टि का आधार है।
नदी में नाला विसर्जित होता है। वह नदी का शरणार्थी है। नदी स्त्री है—हर विसर्जन पर संभार, शरण का आश्रय। नाला पुरुष है, इसलिए परुष। परुष पाषाण है, और पाषाण उदास। उदास नहीं होना है। हम पानी हैं, प्यास नहीं बनना है।
जंगल और घर
जंगल है। घर है। जंगल के आगे घर। घर के पीछे जंगल। जंगल के नीचे जंगल ही। ऊपर भी जंगल-जंगल। जंगल से दूर है घर। फिर भी जंगल पास है। घर से बाहर जंगल। जंगल से बाहर घर।
घर के भीतर घर। जंगल के बाहर जंगल। घर में जंगल नहीं। जंगल में घर नहीं। फिर भी घर जंगल है। जंगल घर है। घर जंगल नहीं। जंगल घर नहीं। जंगल बाहर है। घर भीतर। जंगल बहुत बाहर। घर बहुत भीतर। जंगल में घर ढूँढो, घर नहीं मिलता। घर में जंगल ढूँढो, जंगल नहीं मिलता। जंगल और घर पास-पास। जंगल और घर दूर-दूर।
जंगल कहता है, मैं जंगल हूँ। घर कहता है, मैं घर हूँ। जंगल घर को देखता है। घर जंगल को देखता है। जंगल घर नहीं बनता। घर जंगल नहीं बनता। फिर भी जंगल में घर है। घर में जंगल है। जंगल में पेड़ हैं। घर में दीवारें। पेड़ जंगल को जंगल बनाते हैं। दीवारें घर को घर। पेड़ बाहर हैं। दीवारें भीतर। पेड़ जंगल को छूते हैं। दीवारें घर को थामती हैं। जंगल पेड़ों में फैलता है। घर दीवारों में सिमटता है। फिर भी जंगल सिमटता नहीं। घर फैलता नहीं।
जंगल में हवा चलती है। घर में हवा रुकती है। हवा जंगल की है। हवा घर की भी। जंगल हवा को छोड़ता है। घर हवा को पकड़ता है। हवा जंगल से घर आती है। हवा घर से जंगल जाती है। जंगल और घर हवा में एक। जंगल और घर हवा में अलग।
जंगल में चुप है। घर में चुप है। जंगल की चुप में पत्तों की सरसराहट। घर की चुप में साँसों की आवाज़। जंगल चुप को सुनता है। घर चुप को रखता है। चुप जंगल की। चुप घर की। फिर भी चुप एक है।
जंगल में रास्ता है। घर में दरवाज़ा। रास्ता जंगल को खोलता है। दरवाज़ा घर को बंद करता है। रास्ता जंगल में भटकता है। दरवाज़ा घर में ठहरता है। जंगल रास्ते से जाता है। घर दरवाज़े से आता है। जंगल और घर रास्ते में मिलते हैं। जंगल और घर दरवाज़े में अलग।
जंगल सोचता है, मैं जंगल हूँ। घर सोचता है, मैं घर हूँ। जंगल घर को सोचता है। घर जंगल को सोचता है। जंगल घर को नहीं समझता। घर जंगल को नहीं समझता। फिर भी जंगल घर को जानता है। घर जंगल को जानता है।
जंगल में कुछ नहीं है। जंगल में सब कुछ है। घर में कुछ है। घर में सब कुछ नहीं। जंगल का कुछ घर में आता है। घर का कुछ जंगल में जाता है। जंगल और घर एक-दूसरे में। जंगल और घर एक-दूसरे से बाहर। जंगल कहता है, मैं जंगल रहूँगा। घर कहता है, मैं घर रहूँगा। जंगल जंगल रहता है। घर घर रहता है। फिर भी जंगल घर हो जाता है। घर जंगल हो जाता है। जंगल और घर। घर और जंगल। पास-पास। दूर-दूर। एक-एक। अलग-अलग।
31 मई 2014
पर्वत, चट्टान, और उनके सगोत्री
पर्वत है। चट्टान है। पत्थर है। गिट्टी है। कंकड़ है। रेत है। सब सगोत्री हैं। एक गोत्र। फिर भी अलग-अलग। रंग अलग। रूप अलग। तासीर अलग। कर्म अलग।
पर्वत ऊँचा है। चट्टान ठोस। पत्थर छोटा। गिट्टी टूटी। कंकड़ बिखरा। रेत बारीक़। सब एक मिट्टी से। सब एक पत्थर से। फिर भी सब अपने-अपने। पर्वत पर्वत है। चट्टान चट्टान। रेत रेत। कोई किसी का नहीं।
रंग है। रूप है। तासीर है। यही बाहरी। यही भीतरी। यही धर्म। पर्वत का धर्म ऊँचाई। चट्टान का धर्म ठहराव। पत्थर का धर्म चुप रहना। गिट्टी का धर्म टूटना। कंकड़ का धर्म लुढ़कना। रेत का धर्म बिखरना। एक धर्म नहीं। एक प्रार्थना नहीं। एक देवता नहीं। एक मंत्र नहीं।
सबके घर अलग। पर्वत का घर हवा में। चट्टान का घर ज़मीन पर। पत्थर का घर रास्ते में। गिट्टी का घर ढेर में। कंकड़ का घर नदी में। रेत का घर हवा के साथ। सबके घर सब नहीं जाते। सबके घर सब पहुँना नहीं। पर्वत चट्टान को बुलाता है। चट्टान पत्थर को देखता है। पत्थर गिट्टी को छूता है। गिट्टी कंकड़ को जानती है। कंकड़ रेत को पुकारता है। रेत सबको छूती है। फिर भी सब अकेले।
पर्वत कहता है, मैं सम्राट हूँ। चट्टान कहती है, मैं मजबूत हूँ। पत्थर कहता है, मैं हूँ। गिट्टी कहती है, मैं टूटी हूँ। कंकड़ कहता है, मैं लुढ़कता हूँ। रेत कहती है, मैं बिखरती हूँ। सब अपनी बात कहते हैं। सब अपनी सुनते हैं। कोई किसी की नहीं सुनता।
पर्वत चट्टान को पास रखता है। चट्टान पत्थर को देखता है। पत्थर गिट्टी के पास पड़ा है। गिट्टी कंकड़ को छूती है। कंकड़ रेत के साथ बहता है। रेत सबके साथ। फिर भी पर्वत रेत को नहीं अपनाता। चट्टान कंकड़ को नहीं समझता। पत्थर गिट्टी को नहीं पुकारता। सब पास-पास। सब दूर-दूर।
जाति नहीं। गोत्र नहीं। कर्म है। कर्म ही पहचान। पर्वत रेत का पड़ोसी नहीं। चट्टान पत्थर का सगा नहीं। गिट्टी और कंकड़ रिश्तेदार नहीं। फिर भी सब एक। सब अलग। पर्वत ऊँचा है, पर रेत के बिना अधूरा। चट्टान ठोस है, पर कंकड़ के बिना चुप। पत्थर छोटा है, पर गिट्टी के बिना ख़ाली।
सब पाषाण हैं। सब पाषाण युग के गवाह। फिर भी सब एक जैसे नहीं। पर्वत कठोर है, पर निर्मम नहीं। चट्टान मजबूत है, पर बेशर्म नहीं। पत्थर चुप है, पर उदास नहीं। गिट्टी टूटी है, पर हारी नहीं। कंकड़ बिखरा है, पर खोया नहीं। रेत बारीक़ है, पर ग़ायब नहीं।
जंगल में पर्वत है। नदी में रेत। रास्ते में पत्थर। ढेर में गिट्टी। किनारे पर कंकड़। चट्टान सबके बीच। सब अपनी जगह। सब अपनी बात। फिर भी सब एक-दूसरे में। पर्वत रेत को देखता है। रेत पर्वत को छूती है। चट्टान कंकड़ को ढूँढती है। कंकड़ गिट्टी को पुकारता है। पत्थर सबको चुपचाप देखता है।
सबके घाम में सब नहीं। सबके शीत में सब नहीं। सबके वर्षा में सब नहीं। पर्वत घाम को सहता है। चट्टान शीत को थामती है। पत्थर वर्षा में भीगता है। गिट्टी ढेर में रहती है। कंकड़ नदी में बहता है। रेत हवा में उड़ती है। फिर भी सब एक मिट्टी। सब एक पत्थर। पर्वत सोचता है, मैं पर्वत हूँ। चट्टान सोचती है, मैं चट्टान हूँ। पत्थर सोचता है, मैं पत्थर हूँ। गिट्टी, कंकड़, रेत सब सोचते हैं। सब अपनी सोच में। सब अपने कर्म में। फिर भी सब एक-दूसरे को जानते हैं। सब एक-दूसरे को छूते हैं। सब एक-दूसरे से अलग।
कभी पर्वत रेत से बात करता है। रेत हँसती है। चट्टान पत्थर से पूछती है। पत्थर चुप रहता है। गिट्टी कंकड़ को देखती है। कंकड़ लुढ़क जाता है। सब अपने-अपने। फिर भी सबके बीच एक बात। एक चुप। एक मिट्टी। एक पत्थर। सब सगोत्री। सब अलग। सब एक।
1 जून, 2014
च से चाचा, चीला, और चटनी
च से चाचा। च से चीला। च से चटनी। और जब चाचा घर आएँ, तो चीला-चटनी के बिना बात बने? अरे, ऐसा भला कहीं होता है!
हमारे साहित्यिक मित्र– प्यार से चाचा, यानी डॉ. जे.आर. सोनी, रायपुर नगर निगम के बड़े अफ़सर, धनी रचनाकार, पर दिल से ठेठ छत्तीसगढ़िया। वो जब आये, तो घर में चीला-चटनी की खटपट शुरू। ये तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का वही नाश्ता है, जो पेट भरता है और जीभ को चटख़ारे लेने पर मजबूर करता है।
सुबह से तैयारी। चावल और उड़द दाल को दो-तीन घंटे भिगोया। फिर पानी डालकर ग्राइंडर में नहीं, बल्कि पुराने ज़माने के सिल-लोढ़े पर पिसाई। महीन-महीन। अब चटनी की बारी। टमाटर, धनिया पत्ती, लहसुन, हरी मिर्च, और ज़रा-सा नमक। सब सिल पर चटपट चटकाया। अरे, ग्राइंडर में वो बात कहाँ? सिल की चटनी में तो जान बसती है, वो लहसुन की तीखी ख़ुशबू, वो मिर्च का तड़का!
चाचा आये। हमने तवे पर चीला डाला। गोल-गोल, पतला-पतला। चटनी का कटोरा सामने। लहसुन की महक ने तो जैसे घर को मेला बना दिया। चाचा और मैं, दोनों बैठे। चीला खाया, चटनी चाटी, चटख़ारे लिये। एक, दो, तीन, और हाँ, चौथा चीला भी उड़ा लिया। बड़े चाव से। चाचा बोले, “बेटा, ये चीला-चटनी तो अमृत है!” मैंने कहा, “चाचा, आप ठेठ छत्तीसगढ़िया हो, मैं भी कम नहीं!”
चाचा की बातें, चीला की तपिश, और चटनी का ज़ायक़ा— सब मिलकर ऐसा समा बाँधा कि पेट भरा, दिल भरा, और मन झूम उठा। ठेठपन का यही तो मज़ा है, जो चाचा में है, मुझमें है, और इस चीला-चटनी में भी।
2 जून, 2014
सुबह रायपुर शाम नागपुर
सुबह नौ बजे से तैयार। घर पर प्रतीक्षा। आ ही नहीं रहे– आ ही नहीं रहे। संदीप की दोस्ती जी का जंजाल। चट्टान की छाती चीरकर खिलखिला रहा यह नीम भरी दोपहरी (रायपुर से नागपुर रास्ते पर कहीं किनारे)। फोटो खिंचवाने और खींचने का जानलेवा शौक़!
कार की खिड़की से बाहर खेत, खेत पर काम करते लोग, लोगों के उजले चेहरे देखे जा सकते हैं। मुस्कान उनकी प्रिय भाषा है। वे कुछ भी नहीं कहना जानते– मुस्काना जानते हैं। हम सब कुछ कहना जानते हैं– एक मुस्काना ठीक से नहीं जानते। मैं यही कहता हूँ– संदीप और एहफाज़ भाई से। बात भाषा पर चली जाती है– स्टीरियो पर बज रहे छत्तीसगढ़ी गाने के बहाने।
एक शब्द है पिरोहिल। संदीप की जिज्ञासा है– मैं समझाने का प्रयास करता हूँ- छत्तीसगढ़ी का एक प्रिय शब्द। पिरोहिल यानी जिसे हम प्राण से अधिक चाहते हैं अर्थात् प्राणों से प्यारा। मोर पिरोहिल ओ! कइसे तोला समझावंव। मोर हिरदे मा तैं बसे हस। चिरके कइसे दिखावंव।
बात छोटा नागपुर में प्रचलित भाषा की ओर बढ़ चलती है। मैं कल की बात सुनाने लगता हूँ दोस्तों को– एक मुहावरा है, सुनेंगे- हरक दन्द, न फरक दन्द, मुक्का न खद्द पेटक दन्द। कल जब अपने एक मित्र से मैंने पूछा कि भाई कैसी गुज़र रही है तो मुहावरेदार भाषा में ऐसा जवाब था उनका। मित्र ऊराँव भाई हैं। मतलब- केवल पेट की चिन्ता।
बाघ नदिया, झन जाबे मझनिया…
तरुणाई के कानों में गूँजता यह लोकगीत- बाघ नदिया, झन जाबे मझनिया… ममता चन्द्राकर की आत्मीय, मिट्टी-सी सनी आवाज़ में, छत्तीसगढ़ के जन-मन में रचा-बसा है। “भरी दोपहरी में मत जाना बाघ नदी”, यह पंक्ति जैसे दिल की दीवार पर उकेरी गयी हो। बाघ नदी, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को प्रेम से जोड़ती है, अपने शांत, सुंदर, विनम्र जल के साथ बहती है। इसके किनारे सायंकाल की ठंडी हवा, पेड़ों की छाँव, पक्षियों की चहचहाहट—सब मिलकर मन को बाँध लेते हैं। नदी का किनारा जैसे गाँव वालों की साँसों में बसता हो, उनके सुख-दुख का साथी, चुपचाप साक्षी।
यहाँ कुछ मछुआरे मिले, जिनके चेहरे पर समय की लकीरें और नदी की लहरें एक-सी नाचती हैं। ये लोग वर्षों पहले ओडिशा से आये, पर उनकी जड़ें और भी दूर, पूर्वी पाकिस्तान की उजड़ी मिट्टी में बिखरी हैं। शरणार्थी बनकर पहले ओडिशा, फिर कांकेर के परलकोट क्षेत्र— बांदे, पखांजूर, कापसी— में बसे। पखांजूर को “मिनी बंगाल” कहते हैं, क्योंकि यहाँ की बोली, खान-पान, रहन-सहन में बंगाल की गंध है। मछली पकड़ते हैं, नदी के सहारे जीते हैं। उनके गीतों में नदी की लहरों का संगीत है, और कहानियों में विस्थापन की चुप्पी। एक ज़मीन से उखड़कर दूसरी ज़मीन पर जड़ें जमाने की कथा, जिसमें दर्द है, पर उम्मीद भी है। नदी उनके लिए माँ है— जो भोजन देती है, पानी देती है, जीवन देती है।
उनकी आँखों में खारा पानी है, जो शायद समंदर से आया, या शायद आँसुओं से। घर छूटा, तो जैसे सारी दुनिया छूटी। फिर भी, वे हँसते हैं, जैसे हँसी उनकी आख़िरी संपत्ति हो। पूछने पर बोले, “हम ओम् नमो शुद्राय हैं।” हमने कहा, “तो फिर यह दोपहरी आपके साथ बिताएँगे।” और फिर, जैसे नदी का पानी किनारे से टकराया हो, उनकी बातें बहीं— लोककथाएँ, गीत, पीड़ाएँ, चुपके से छिपी चिंताएँ। हर कहानी में एक उजड़ा घर, हर गीत में एक अधूरी चाह। वक़्त कम था, ज़ुबान छोटी। पर उनकी बातें, जैसे नदी की लहरें, कहीं ठहरती नहीं थीं।
वे कहते हैं, नदी सब जानती है। उनके दुख, उनकी हँसी, उनके दिन-रात। पर नदी कुछ नहीं कहती। बस, बहती रहती है। जैसे कह रही हो— जो छूट गया, उसे छूने की कोशिश मत कर। जो है, उसे जी ले।
लौटता हूँ
पेड़, फूल, पत्ती मेरे पास नहीं आते, जैसे कोई अपने घर का रास्ता भूल जाये। वे खड़े रहते हैं, अपनी जगह, अपनी मिट्टी में, और मैं, एक बेचैन राहगीर, उनकी ओर चला जाता हूँ।
मेरे क़दमों में कोई जल्दी नहीं, बस एक ठहराव है, जैसे धरती से बात करने की आदत। मैं उनके पास पहुँचता हूँ, उनकी छाँव में साँस लेता हूँ, और वे मुझे देखते हैं— बिना कुछ कहे, बिना कुछ माँगे। फिर मैं लौट आता हूँ, हर बार, जैसे कोई पुराना वादा निभाने। धरती पर बिछकर, पेड़ की तरह सीधा, फूल की तरह नरम, पत्ती की तरह हल्का। मेरे लौटने में कोई शोर नहीं, बस एक चुप्पी है, जो धरती समझती है।
क्रमश:

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

