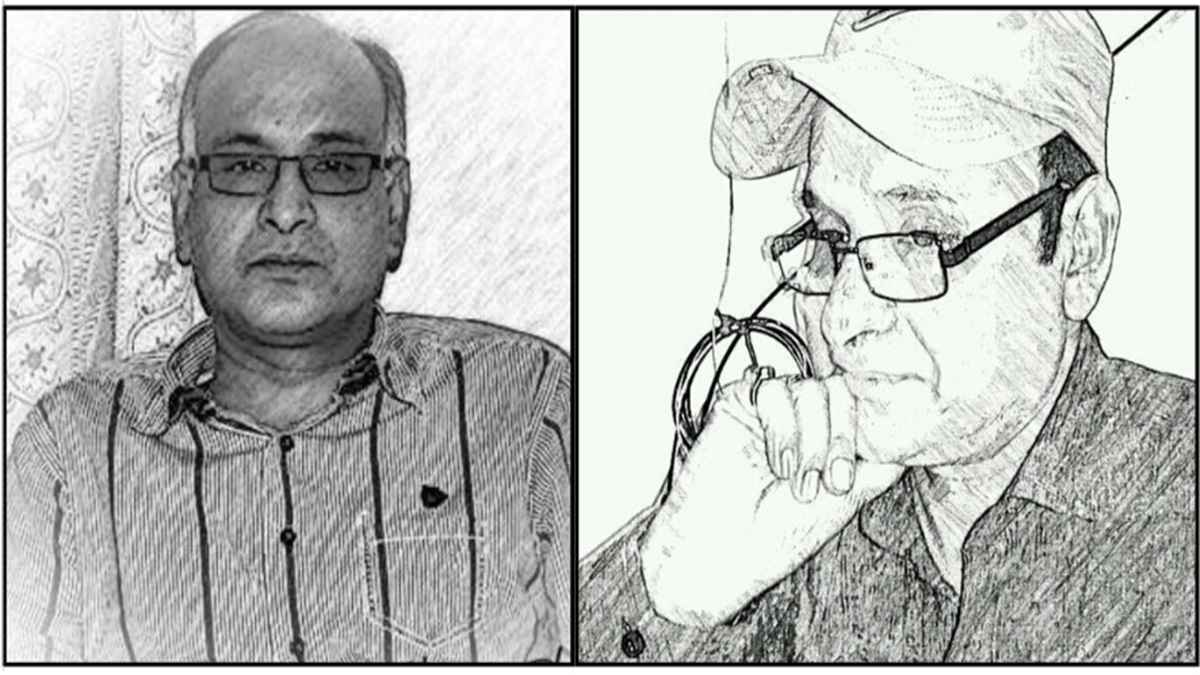
- August 9, 2025
- आब-ओ-हवा
- 0
कवियों की भाव-संपदा, विचार-वीथिका और संवेदन-विश्व को खंगालती इस डायरी का मक़सद प्रकाशन पूर्व पाठक-लेखक संवाद बनाना है...
जयप्रकाश मानस की कलम से....
पूर्वपाठ — एक कवि की डायरी : भाग-13
और सब ठीक है?
10 अप्रैल 2014
आज के ज़माने में किसी का हस्तलिखित पत्र आना किसी बड़ी घटना से कम नहीं। कोरे काग़ज़ पर स्याही से लिखे हुए शब्दों को देखने की प्रतीति ऐसी कि जैसे निर्जन रेगिस्तान में एकबारगी कोई पथिक दिख गया हो। या गहन अंधियार और डरावनी रात में जुगनुओं से मुलाक़ात हो गयी हो। हाथ से चिट्ठी-पतरी लिखना हमारी पीढ़ी के लोग तो भूल ही चुके हैं, गोया उन्होंने कभी क़लम या पेन से कुछ लिखा ही न हो!
दोपहर पटना से डॉ. खगेन्द्र ठाकुर जी का पत्र मिला। लिखते हैं: मैं ठीक हूँ। हाल में कई किताबें छपी हैं। एक उपन्यास भी ‘सेन्ट्रल जेल’ नाम से लिखा, वह छप गया है। कहानी-आलोचना की भी एक किताब ‘कहानी- संक्रमणशील कला’ वाणी से छपी है। और सब ठीक है! आपका भी सब ठीक है ना? आपका स्नेही- खगेन्द्र ठाकुर।
लेखक भी सब नहीं पढ़ता
आज सुबह किताबों के बीच बैठा था, और मन में एक पुरानी बात कौंध गयी। शायद भारत भारद्वाज जी ने कभी गपशप में सुनायी थी। स्वीडन में नोबेल पुरस्कार समारोह के दौरान कुछ महान लेखकों से एक पत्रकार ने सवाल किया था— उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी कौन-सी किताबें हैं, जिन्हें आप अब तक नहीं पढ़ सके और पढ़ना चाहते हैं? जवाब हैरान करने वाले थे। दांते, होमर, मिल्टन, रूसो, चेखव, दोस्तोव्स्की, बाल्ज़ाक, रोम्यां रोला, गांधीजी, रवीन्द्रनाथ टैगोर— ये वो नाम थे, जिन्हें न पढ़ पाने का मलाल उन लेखकों को था। सोचता हूँ, अगर नोबेल विजेता भी ऐसी कृतियों को छू न सके, तो हम जैसे साधारण पाठक कितने अधूरे हैं। किताबें अनंत हैं, और जीवन कितना छोटा।
यह बात मुझे और भी कुरेदती है। पढ़ना तो दूर, कई बार किताबें ख़रीदकर अलमारी में सजा लेते हैं, मानो उन्हें रख लेना ही पढ़ लेने का पर्याय हो। फिर टालते रहते हैं— अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। पर वह ‘तब’ कभी नहीं आता। कितना कुछ छूट जाता है, और हम कितने कम को छू पाते हैं।
एक और प्रसंग याद आता है: कुछ साल पहले पेरिस में एक साहित्यिक गोष्ठी में दुनिया भर के लेखक जुटे थे। वहाँ भी एक पत्रकार ने सवाल उछाला— आपके लिए सबसे ज़रूरी किताब कौन-सी है, जिसे आपने अब तक नहीं पढ़ा? एक लेखक ने हँसते हुए कहा, “काफ्का की ‘मेटामॉर्फोसिस’। हर बार शुरू करता हूँ, और हर बार कुछ अधूरा छोड़ देता हूँ।” दूसरे ने जोड़ा, “मुझे तो प्रूस्त की ‘इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम’ का इंतज़ार है। सात खंड! समय कहाँ है?” तीसरे ने टॉल्स्टॉय की ‘वॉर एंड पीस’ का नाम लिया। कितना अजीब है कि जो लोग ख़ुद साहित्य रचते हैं, वे भी साहित्य के इस विशाल सागर में डूबने से डरते हैं।
एक वाकया और: न्यूयॉर्क में एक किताब मेले में मशहूर लेखिका टोनी मॉरिसन से किसी ने पूछा था, “आपके लिए पढ़ने का मतलब क्या है?” उन्होंने जवाब दिया, “पढ़ना मेरे लिए हवा जैसा है। लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने कितना कम पढ़ा है। गाब्रिएल गार्सिया मार्केस की ‘वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड’ को मैं अब तक टालती आयी हूँ। हर बार लगता है, इसे पढ़ने के लिए एक ख़ास मन चाहिए।” यह सुनकर लगा, शायद यही पाठक की नियति है। हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, पर कुछ न कुछ छूट ही जाता है।
कभी-कभी सोचता हूँ, क्या पढ़ना इतना ज़रूरी है? या बस यह समझना काफ़ी है कि कुछ किताबें हमारी प्रतीक्षा में हैं, और शायद किसी और जन्म में, किसी और समय में, हम उन्हें खोलेंगे। पर फिर मन कहता है— नहीं, जो पढ़ सको, उसे अभी पढ़ लो। समय तो वैसे भी कम है।
कौन तय करता है मुख्यधारा
आज फिर वही पुराना सवाल मन में कौंधा— यह ‘मुख्यधारा’ क्या है? हिंदी साहित्य में यह शब्द किसी जादुई छड़ी की तरह घुमाया जाता है, मानो इसके बिना कोई रचनाकार अधूरा हो। कवि, संपादक, समीक्षक, प्रकाशक, यहाँ तक कि पाठक भी इस मुख्यधारा के पीछे भागते हैं। पर यह है क्या? किसी नदी का साफ़ पानी, या फिर किसी गंदे नाले की मैली धार, जिसमें बहने वाला ही ‘मुख्यधारा’ का कहलाता है?
मैं सोचता हूँ, और हँसी आती है। यह मुख्यधारा कोई पवित्र गंगा तो नहीं, बल्कि एक ऐसी कृत्रिम रेखा है, जिसे कुछ लोग अपनी सुविधा से खींचते हैं। जो उनके ख़ेमे में नहीं, वह इस धारा में नहीं। डॉ. राजेन्द्र मोहन भटनागर की बातें याद आती हैं। उनकी पुस्तकों के संस्करणों की गिनती नहीं, विश्वविद्यालयों में उनकी रचनाएँ पढ़ी जाती हैं, ‘नीले घोड़े पर सवार’ का फ़िल्माँकन हो चुका, फिर भी कुछ लोग उन्हें मुख्यधारा से बाहर मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी ख़ेमे में नहीं बँधे। क्योंकि उन्होंने साहित्य को राग-द्वेष, ऊँच-नीच, तुच्छ-महान की सीमाओं से ऊपर रखा।
उनके शब्द मेरे मन में गूँजते हैं— ‘मैं नहीं जानता कि मुख्यधारा में मैं नहीं हूँ। यह मुख्यधारा क्या है और कौन तय करता है कि इसमें अमुक व्यक्ति है कि नहीं?’ सचमुच, कौन है इसका ठेकेदार? वे कहते हैं कि साठ के दशक के बाद साहित्य की समीक्षा की जगह व्यक्ति की समीक्षा होने लगी। साहित्य गौण हो गया, व्यक्ति और उसकी दलबंदी प्रमुख। साहित्य को ख़ेमों में बाँट दिया गया, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी हो।
मुझे उनकी वह स्वतंत्रता भाती है। किसी ख़ेमे में न बँधने का साहस, किसी राजनैतिक या साहित्यिक गिरोह का हिस्सा न बनने का स्वाभिमान। वे कहते हैं, ‘शाश्वत साहित्य ख़ेमेबाज़ी से ऊपर होता है।’ और यह बात मेरे मन को छूती है। साहित्य वही, जो समय की सीमाओं को लाँघ जाये, जो अंधेरे में उजाले की किरण तलाश ले।
उनकी बातों में एक सादगी है, एक निश्छल विश्वास। लिखने से उन्हें शांति मिलती है, सुकून मिलता है। वे कहते हैं, ‘मेरे पास समय का नितांत अभाव रहा। मैंने अपने साहित्य का बहुत सारा भाग बोलकर लिखाया है।’ फिर भी, जो लिखा, वह शाश्वतता की तलाश में लिखा। वे हल्क़ी हँसी और निश्छल मुस्कान के साथ कहते हैं, ‘जो आदमी साहित्यकार ही नहीं है, वो मुख्यधारा में क्यों आएगा?’
उनके शब्द मेरे लिए जैसे एक मंत्र बन गये हैं। साहित्य मेरे लिए भी वही है— शांति, विश्वास, सुकून। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जो लिखूँ, वह मेरे भीतर के उजाले को बाहर लाये। पाठकों का प्यार, उनकी स्वीकार्यता— यही तो पर्याप्त है। मुख्यधारा? वह तो एक भ्रम है, जो ख़ेमों की दीवारों में क़ैद है। मैं तो उस शाश्वतता की तलाश में हूँ, जो किसी धारा की मोहताज नहीं।
13 अप्रैल, 2014
मतलब
पिता जब से बेटों की नज़रों में मात्र सुविधा दिलाने वाला रह जाता है, तबसे उसकी धीमी मौत शुरू हो जाती है।
मैय्यत का सामान
नागपुर। मृत्यु स्वयं में जीवन का एक संस्कार है। ऐसा संस्कार जो मनुष्य को सदा-सदा के लिए यादगार बना जाता है या फिर उससे नाराज़ दुनिया को उसकी अनुपस्थिति से निश्चिंत होने का उपहार दिला जाता है। दरअसल मृत्यु वास्तविक जीवन का प्रवेशद्वार है। जीवन का समापन नहीं। वह रोज़-रोज़ की वास्तविकता है। वास्तव इन शब्दों में भी कि बहुतों का जीवन ही मृत्यु जैसा।
जो भी हो : हम संसारी जन उससे डरते बहुत हैं और वह डराती भी बहुत है। संस्कार का डर तो होता ही है। डर का भी एक संस्कार होता है। संस्कार और डर शायद आबद्ध हैं परस्पर। अर्थात् संस्कार उसी के पास जो डरना जानता है, जिसे डर है उसके पास संस्कार का धन है। शायद इसीलिए मरने के बाद दुनिया की लगभग हर सभ्यता और जातियों में मृत्यु-संस्कार किया जाता रहा है। पुराने से पुराने आदिवासी समाज से लेकर अब के उत्तर आधुनिक परिवार में भी। यानी डर से मुक्ति का संस्कार। हम मनुष्य को मात्र देह नहीं मान सकते। उसकी भौतिकता से चाहे जितना छेड़छाड़ कर लें, जाने क्यों उसकी कायिक अनुपस्थिति के बाद उसकी आत्मिक उपस्थिति को लेकर सशंकित हुए रहते हैं। कदाचित् संस्कार का डर कह लें चाहे डर से संस्कार। कहीं-कहीं तो अंधविश्वास की सारी सीमाओं को लाँघकर भी। बहरहाल…
मृत्यु अपने आगमन का कोई विज्ञापन नहीं करती। नितांत अदृश्य। नितांत एकाकी। लेकिन उसके गमन की मुनादी चारों दिशाओं में होती है। दुनिया मृत्यु के पधारने पर नहीं, उसकी वापसी पर तामझाम करती है। ये तामझाम चाहे मृतक की देह की शांति के लिए हो या फिर आत्मा की, सोचें तो भला! मृतक के घर-परिवार वाले ठीक से रो रुआ कर जी को हल्का भी नहीं कर सकते। कफ़न ख़रीदने भागो। लकड़ी जुटाने दौड़ो। चंदन लाओ। हल्दी रखो, नमक रखो। शुद्ध घी तलाशो। फूल खोजो। धूप ढूँढ़ो। उदबत्ती ढूँढो। ऊपर से सारे रिश्ते-नाते वालों को ख़बर दो वरना क्या पता कौन भड़क उठे। और सबसे बड़ी चुनौती कि ये सब चंद घंटे की सीमा में ही हों।
सारी भावनाओं और असह्य वेदना को कचरे की तरह बुहारकर- मृत्यु पर सबसे अधिक और विरल कविता रचने वाले कवि अशोक वाजपेयी के शब्दों मे कहूँ तो: वह आँसुओं, हिचकियों का घर- चीख और आर्तनाद का घर- विषाद का घर- भला हो शहर वालों का जहाँ मैय्यत का सारा सामान एक जगह ही मिल जाता है। इतनी सुविधा यदि बाज़ार दे रहा है तो ग़रीब और दीन-दुखियों की ओर से ऐसे बहादुर दुकानदारों का भी आभार, जो मृत्यु की बाट जोहते वर्षा-शीत-घाम में उँघते हुए सबसे उदास और आँसुओं से छलछलाते चेहरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं।
क्या आप या हम मैय्यत का दुकान खोल सकते हैं? बेरोज़गारी हमारी चाहे कितनी भी गर्दन क्यों न मरोड़े। आज नागपुर में एक बड़े अस्पताल के पास दवाई दुकान के बीच मैय्यत के सामान का दुकान देखकर इतना ही सूझ पा रहा है और इतना ही सोच पा रहा हूँ।
14 अप्रैल, 2014
एक लकीर में होती है कविता
‘एक डरा हुआ आदमी ख़तरनाक हो सकता है।’
बलिया के युवा कवि भाई समीर कुमार पांडेय की एक कविता में बीच की लकीर। एक कभी न भुला पाने वाली लकीर। कवि के संपूर्ण स्वप्न और सरोकार को परत-दर-परत बयान करती लकीर। सच कहूँ तो इस आततायी समय में डरे हुए को भीतर तक ताक़त देती लकीर। कविता का प्राण है इस एक लकीर में। कविता चाहे कितनी भी बड़ी हो कहीं-न-कहीं अक्सर उसके प्राण किसी एक ही लकीर में होती है। वह एक लकीर ही पाठकों को बार-बार अपनी ओर खेंचती है। आस्वाद जगाती है, कविता के भीतर के सारे कहे-अनकहे को अर्थ देती है। पूरी कविता में चाहे कितना भी विस्तार हो उसका निस्तार एक ही उजली लकीर से होता है। और उस एक ही लकीर को साध लेना संपूर्ण कविता को साध लेना भी होता है। बाक़ी लकीरें तो कविता के हाथ, पैर, कान, नाक, मुँह आदि होते हैं प्राणतत्व तो केवल एक ऐसी लकीर में होता है। यही एक लकीर सारी भोथरी लकीरों को भी जीवन देती है। कविता में इस प्राणतत्व को पा लेना, कविता को पा लेना है। कविताई दरअसल यही है। पूरी कविता कुछ इस तरह:
सोये हुओं को
वैचारिक गान(भोंपू) से
सपनों की नींद से जगाना
जितना ज़रूरी है लोकतांत्रिक देश के लिए…
उतना ही ज़रूरी है
उनको निडर बनाना भी
अलग-अलग बातें है दोनों
एक द्योतक है निर्माण की
तो दूसरी विध्वंस की
क्योंकि एक डरा हुआ आदमी ख़तरनाक हो सकता है
ख़ुद के लिए समाज के लिए
और देश के लिए भी..।
तमीज़
इर्ष्यालु कवि सबसे नीच पशु होता है और पशुओं को कविता की तमीज़ आती ही नहीं।
अच्छी कविता की पहचान
कविता लिखाई और छपाई सरल है परन्तु अच्छी कविताओं की छँटाई और पढ़ाई सरल नहीं है।
कविता लिखना और छापना सरल हो सकता है, पर अच्छी कविता को चुनना और उसकी गहराई को समझना आसान नहीं। अच्छी कविता वह नहीं जो केवल शब्दों का सुंदर खेल हो, बल्कि वह जो विचारों की गहराई, कला की उत्कृष्टता और सामाजिक संवेदना को एक साथ समेटे। यह आलेख अच्छी कविता की पहचान, उसकी चयन प्रक्रिया की कठिनाइयों और श्रेष्ठ तरीकों पर विचार करता है, जिसमें विचारगत और कलागत आयामों को संतुलित किया गया है। साथ ही, एक विदेशी संपादक के अनुभव को संदर्भ के रूप में जोड़ा गया है।
विचार और संवेदना का मेल
अच्छी कविता सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना को छूती है। वह अन्याय, असमानता और पीड़ा को आवाज़ देती है, साधारण जीवन की असाधारणता को उजागर करती है। जैसे, एक किवाड़ की सादगी में गहरे अर्थ छिपे हों, वैसे ही कविता रोज़मर्रा के अनुभवों को गहन दर्शन से जोड़ती है। वह केवल भावनाओं का उच्छ्वास नहीं, बल्कि विचारों की गहराई लिये होती है, जो पाठक को जीवन के जटिल प्रश्नों पर सोचने को मजबूर करती है। प्रामाणिकता उसका मूल तत्व है— वह व्यक्तिगत अनुभूति को सामूहिक संवेदना से जोड़कर सार्वभौमिक बनाती है।
कला का शिल्प
कविता की भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली और मौलिक होनी चाहिए। वह शब्दों के माध्यम से एक नया संसार रचती है, जिसमें ध्वनियाँ और लय पाठक को बाँधे रखती हैं। प्रतीकों और बिंबों का उपयोग ऐसा हो कि विचार को गहराई मिले और मन में दृश्यात्मक प्रभाव बने। साधारण वस्तुएँ— जैसे एक दरवाज़ा या खिड़की— गहन प्रतीक बन जाएँ। संरचना में संतुलन और लय हो, जो मुक्त छंद में भी पाठक को अपने साथ बहा ले जाये। कविता का शिल्प उसकी आत्मा को उजागर करता है, जो उसे साधारण शब्दों से ऊपर उठाता है।
चयन की चुनौतियाँ
अच्छी कविता को चुनना आसान नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है विषयपरकता— हर पाठक या संपादक का स्वाद अलग होता है। “अच्छी” कविता की परिभाषा धुंधली पड़ती है, क्योंकि एक के लिए जो उत्कृष्ट है, वह दूसरे के लिए साधारण हो सकता है। आज के डिजिटल युग में कविताओं की बाढ़ है— सोशल मीडिया, ब्लॉग और पत्रिकाएँ कविताओं से भरे पड़े हैं। इस प्रचुरता में गुणवत्ता को छाँटना एक टेढ़ी खीर है। संपादक की अपनी विचारधारा या सौंदर्यबोध चयन को प्रभावित करता है, जिससे निष्पक्षता भंग हो सकती है। पाठक की साहित्यिक और भावनात्मक परिपक्वता भी ज़रूरी है, क्योंकि सतही पढ़ाई कविता की गहराई को नहीं पकड़ पाती। समय और संदर्भ भी कविता के प्रभाव को तय करते हैं— एक युग की प्रासंगिक कविता दूसरे युग में फीकी पड़ सकती है।
चयन के रास्ते
अच्छी कविता को चुनने के लिए कुछ तरीके अपनाये जा सकते हैं। पहला, कविता में विचार और कला का संतुलन हो— वह न केवल भावनात्मक हो, बल्कि बौद्धिक रूप से भी समृद्ध हो। दूसरा, उसका प्रभाव देखा जाये— क्या वह पाठक को सामाजिक यथार्थ पर सोचने को मजबूर करती है? तीसरा, मौलिकता और नवाचार— कविता में भाषा, शैली या दृष्टिकोण में कुछ नया हो। चौथा, सामाजिक प्रासंगिकता— कविता समाज की नब्ज़ को पकड़े और संदर्भ में प्रासंगिक हो। अंत में, निष्पक्षता के लिए विविध दृष्टिकोणों या समिति का सहारा लिया जाये, ताकि संपादक की व्यक्तिगत पसंद गुणवत्ता के सामने गौण रहे।
एक विदेशी नज़रिया
प्रसिद्ध अमेरिकी कवि और संपादक टेड ह्यूज ने कविता की गुणवत्ता पर कहा था: “कविता वही है जो पहली बार पढ़ने के बाद भी पाठक के मन में जीवित रहती है। यह केवल तकनीक या भावना का मसला नहीं, बल्कि एक अनूठी आवाज़ है, जो मानवीय स्थिति को सार्वभौमिक और गहराई से व्यक्तिगत रूप में बयान करती है।” ह्यूज का यह कथन कविता में विशिष्टता और स्थायित्व की खोज को रेखांकित करता है। उनके संपादकीय अनुभव से यह सीख मिलती है कि कविता में एक ऐसी आवाज़ होनी चाहिए जो स्थानीय होते हुए भी सार्वभौमिक हो और पाठक के मन में लंबे समय तक गूँजे।
अंतिम बात
अच्छी कविता विचार, कला और संवेदना का संगम है। वह समाज को आईना दिखाती है और पाठक के मन को छूती है। चयन की कठिनाइयों— विषयपरकता, प्रचुरता, पूर्वाग्रह— को निष्पक्षता और गहरी समझ से पार किया जा सकता है। कविता वही है, जो समय और स्थान की सीमाओं को लाँघकर मनुष्यता को आवाज़ दे।
क्रमश:

जयप्रकाश मानस
छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ अधिकारी जयप्रकाश मानस की कविताओं, निबंधों की दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने आधा दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया है और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको और आपकी पुस्तकों को नवाज़ा जा चुका है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

