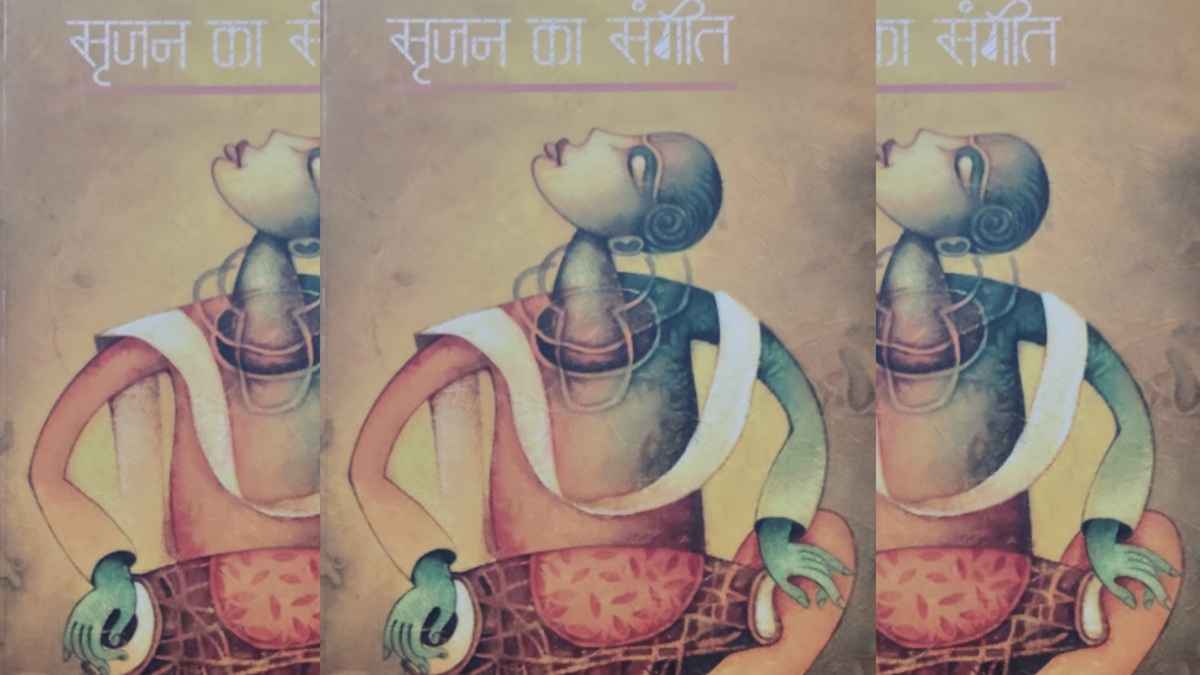
- August 3, 2025
- आब-ओ-हवा
- 1
भरत प्रसाद की कलम से....
सृजन का सांगीतिक सौंदर्य
यह प्रश्न आज अधिक ज़रूरी है, कि सृजन किसे कहा जाये? केवल मनुष्य के द्वारा निर्मित, उत्पन्न सृजन है, या उसके अतिरिक्त दृश्य जगत भी सृजन है? हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग मनुष्यगत सृजन के लिए ही करते हैं, परन्तु प्रकृतिजन्य सृजन को क्या कहेंगे? दृष्टि को ज़रा विस्तार दें, परिभाषा को व्यापक बनाएं और शब्द के अर्थ को अनुभूति का स्तर दें, तो सृजन के बाहर कुछ भी नहीं। दृश्य, अदृश्य, ज्ञात, अज्ञात, सरल, जटिल, सुंदर, असुंदर, प्रिय, अप्रिय, सुपरिचित, अजनबी सब सृजन के विविध रूप हैं। कुछ भी न होने के बाद, जिस भी प्रकार के ‘कुछ’ की शुरूआत हुई, वहीं से सृजन का सिलसिला शुरू होता है। इस अर्थ में शून्य भी एक सृजन है, बल्कि महासृजन। क्योंकि यह ख़ालीपन, यह अवकाश, यह असीम, अनंत गैप सब कुछ के होने का मूलाधार है, पहली शर्त है।
सब कुछ का होना, कुछ भी न होने से संभव हुआ। हवा, मिट्टी, पानी, रौशनी, अंधकार, ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सबके सब नैसर्गिक, प्राकृतिक सृजन हैं। ये सभी अप्रत्याशित और अज्ञात संभावना के कोष हैं, धारक हैं। इनमें छिपी अज्ञात शक्तियों का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। विज्ञान भी नहीं कर सकता। जो दृश्य है, प्रत्यक्ष है, प्रकट है- विज्ञान उनमें मौजूद प्राकृतिक तथ्यों की खेाज करता है, यथार्थ की ख़बर देता है, उसके भौतिक सत्य का ज्ञान कराता है, परन्तु विज्ञान यह बताने में असमर्थ है, ठंडे जल को पीने से हमारी सकारात्मक दृष्टि पर क्या फर्क पड़ता है ? आग को देखकर हमें हंसी क्यों नहीं आती ? आकाश को देखकर हम रहस्य से क्यों भर उठते हैं ? अंधकार हमें प्रसन्नता क्येां नहीं दे पाता ? उजाला हमें क्येां भयमुक्त कर देता है ?
ऐसे भावात्मक, मनोवैज्ञानिक, आंतरिक सत्यों का विश्लेषण और मीमांसा विज्ञान के पास नहीं। सच तो यह है कि प्रकृति की शक्तियों का कितना व्यापक और स्थायी प्रभाव हमारे विवेक पर पड़ता है, यह मनोविज्ञान भी नहीं सुनिश्चित कर पाता। यह प्राकृतिक, नैसर्गिक सृजन जो हमारे बाहर है, और भीतर भी है, जो सांस दर सांस हमारे वजूद को ढंके हुए है, हमकों आप्लावित किए हुए हैं, हमें संचालित, नियंत्रित और प्रेरित करता है, सही अर्थों में सर्वशक्तिमान है। वैदिक कालीन ऋषियों ने इन नैसर्गिक शक्तियों को देवी/देवता की उपाधि दे दी, परन्तु सत्य यह है कि बिना किसी दैवीय उपाधि के ही, ये अद्वितीय हैं, स्वयंभू हैं, निर्विकल्प हैं। मनुष्य बौना ही नहीं, नाकाफी और अधूरा है, इनकी सत्ता, महत्ता और असीमता को व्यक्त करने के लिए। वह चाहे बोलकर इनकी महिमा प्रकट करे या लिखकर। दोनों ही रूपों में उसकी क्षमता की सीमाएं तय हैं। सूर्य पर हज़ारों कविताएं मिलकर भी सूर्य को परिभाषित नहीं कर सकतीं। वैदिक वांङ्मय में ‘पृथ्वी सूक्त’ निर्मित हुआ। किन्तु पृथ्वी की महिमा को वैदिक ऋषि भी अपने मंत्रों में न बांध सके। विलियम वडर््सवर्थ, वाल्ट ह्विटमैन, सुमित्रानंदन पंत तीनों तीन भाषाओं के अमर प्रकृतिभक्त। परन्तु आज भी प्रकृति के पल-पल परिवर्तित वेश पर नाचने वाली कलम मिल ही जाएगी। ऐसे अलक्षित, अज्ञात बिम्ब कृतज्ञ हृदय से फूट ही पड़ते हैं, जो पहले अन्य किसी आत्मसजग कवि के द्वारा नहीं प्रकट हुए। सृजन का सबसे बड़ा, अनादि और कालजयी मंच यह प्रकृति है, जिसमें क्षण-क्षण लाखो रूपों में रंग-ढंग और अंदाज में सृजन का उत्थान-पतन, बनना-मिटना, फैलना-सिमटना मचा हुआ है। यह कब, कैसे शुरु हुआ। कहाँ, किस तरह समाप्त होगा, कोई नहीं जान सकता, न बता सकता है। जब मनुष्य तक की सामर्थ्य नहीं, तो शेष जीवित सत्ता के बारे में क्या कहा जाये?
बहुत सहजता किन्तु अकुंठ दृढ़ता के साथ कहना ज़रूरी है, अब ‘नेति-नेति’ किसी ईश्वर को नहीं, बल्कि इस अपरिभाषेय, अद्वितीय और स्वयंभू सृष्टि को कहना चाहिए। सहज ही एक प्रश्न उठता है भीतर कि सृष्टि के भीतर निरंतर मचे हुए इस नैसर्गिक सृजन का मूल कारण या रहस्य क्या है? वह क्या है, जो सृष्टि के सृजनात्मक स्वरूप का मूल कारण है ? वह है स्थिरता का भ्रम पैदा करता हुआ अमर परिवर्तन। यह परिवर्तन ही वह पहला और अंतिम कारण है, जो सृजन का चमत्कार संभव करता है। अंकुर पौधे में तब्दील होता है, फिर धीरे-धीरे वृक्ष का आकार, फिर छतनार दरख़्त, फिर अंग-अंग से डालियाँ, पत्ते गिराता हुआ बूढ़ा पेड़, और आख़िर में ? कैसे हुआ यह सब, किस कारण एक बीज, गिरे हुए पेड़ में तब्दील हो गया ? यह बदलाहट की अदृश्य प्रक्रिया के कारण हुआ। वस्तु की दशा में जब बदलाव आता है, तो परिवर्तन महसूस होता हैं उसे हम प्रत्यक्षतः कभी देख नहीं सकते। बदली हुई दो स्थितियों के अंतराल में हम परिवर्तन का एहसास मात्र पाते हैं। यहीं पर सृजन करवट ले लेता है। अर्थात् परिवर्तन और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
आइए, अब अपने सृजन की ओर चलें। मनुष्य स्वभावतः सृजनात्मक होता है। कलम-काग़ज़ से हटकर सृजनात्मक। वह अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी गढ़ता है, तराशता, निर्मित करता है, वह सृजन है। विशुद्ध मनुष्यगत सृजन। साहित्यिक सृजन उसके हाथों बहुत बाद में आरंभ हुआ। अग्नि का आविष्कार, पहिये की खोज ओर अन्न का उत्पादन मानव इतिहास के महानतम सृजन में से एक हैं इस विश्वजनीन सृजन के आगे कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि का सृजन बहुत सीमित और छोटा है। मनुष्य के भीतर भी दो प्रकार के सृजन रूप मौजूद है। एक सकारात्मक आंतरिक सृजन और दूसरा नकारात्मक आंतरिक सृजन। प्रेम, दया, करुणा, ममता, मोह, सेवा, परहित, सहिष्णुता इत्यादि अमिट सकारात्मक सृजन हैं। जबकि घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, वैमनस्य, शत्रुता इत्यादि स्थायी नकारात्मक सृजन। इन्हें सृजन इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य के ढांचे में ये दोनेां उत्पन्न हुए हैं, विकसित हुए हैं उम्र में बदलाव के साथ-साथ ये भी दिन-प्रतिदिन बदलते रहते हैं। इसमें दो मत नहीं कि मनुष्य के भीतर नकारात्मक शक्तियों की गति प्रबल है, और सकारात्मक शक्तियों की चाल बहुत धीमी, किन्तु गहन, गुरु, गंभीर। इसीलिए मनुष्य सर्वाधिक अपनी नकारात्मकता के दबाव, नियंत्रण और तनाव में जीता है। सारी योग्यता, सफलता, प्रसिद्धि और महानता के बावजूद वह बादशाही नकारात्मकता से मुक्ति नहीं हासिल कर पाता।
जिसे हम सृजन कहते हैं- वह अपनी प्रकृति में है क्या? वह है- आवेग, राग, प्रवाह और तरंग और ये चारों भाव से उत्पन्न होते हैं। जहाँ भाव प्रबल होगा, वहाँ संगीतात्मकता रहेगी, वहाँ सृजन की संभावना मौजूद होगी। इस तरह संवेदना जमीन है, सृजन की और संगीत प्राणरस है- सृजनात्मकता का। ये तीनों एक-दूसरे से गूंथे हुए आपस में एक-दूसरे को संभाले रहते हैं। अभी तक मनुष्य ने सृजन में संगीत तत्व को कभी लय, कभी ताल, तुकबंदी, कभी गेयता के माध्यमों से प्रकट किया। जबकि क्रिएटिविटी के क्षेत्र में संगीत की संभावना की कोई सीमा नहीं। वह अनेक ढंग से, कई शैलियों, रूपों, तरीकों में प्रकट हो सकता हैं संभवतः हमारे बीच जितने भी क्लासिकल संगीत और लोक संगीत के रूप हैं, सबमें नितांत नयी, मौलिक और अत्याधुनिक कविताएं लिखी जा सकती हैं। बस कवि को उसकी अंतध्र्वनि साधना है। उस शैली के मर्म को समझना है, उस संगीत में मौजूद अंतर्लय को आत्मसात करना है। कवि केवल दत्तचित्त होकर क्लासिकल या जनपदीय आंचलिक, ग्रामीण लोकसंगीत को सुन ले, गुन ले, पी जाये हृदय से, फिर देखिए कैसे नहीं फूटती है- चुम्बकीय लय में सधी हुई तत्वपूर्ण कविताई। यदि कहन में बस एक आवेग है, यदि अंदाज़े-बयां में एक प्रवाह, एक बेफिक्र, मस्ती और रवानगी है, तो बह चला संगीत कविता के भीतर। ‘मुझे पुकारती हुई पुकार, खो गयी कहीं…।’ मुक्तिबोध की अकेली एक कविता इस उद्दाम आवेग का सशक्त उदाहरण है। कवि जब तक अपने कहन के तरीके से बंधा है, जब तक वह तरीके को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, जब तक वह तेवर में छलांग नहीं पैदा करता, वह लिखेगा, साधारण कविताएं ही। वह प्रबल बौद्धिक कविताएं भले रच डाले, मगर चित्त को भिगो देने वाली तरंगमय कविताई नहीं कर सकेगा। कहने को तो कवि के लिए समूची कायनात ही सीखने की प्रयोगशाला है। वह पत्तियों की मर्मर, नदियों की कलकल और बारिश की रिमझिम से बहुत नये, अप्रत्याशित महत्व की बात सीख सकता है, परन्तु संगीतात्मक घटनाओं की सूक्ष्मता में वह जितना ही उतरेगा, जितना ही अभिनव ध्वनियों की खेाज में भटकेगा, जितना ही प्रकृति के निःशब्द नृत्यों में तबीयत से डुबकी लगाएगा, उसकी कलम में संगीत की रागिनी उतनी ही प्रबल होगी। कहीं गंवई मानव विरह की तार छेड़े है, कहीं काकी सोहर गीत गा रही हैं, कहीं युवती इशारे इशारे एकांत में प्रेमी को पुकार लगा रही है, कहीं पत्नी अपने विरह में अपार दुख का रोना रो रही है। ये सब सृजन को समृद्धि देने वाले जीवनराग हैं।
हिन्दी कविता में प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध, त्रिलोचन जैसे आधुनिक कवियों ने परम्परागत संगीत का रचनात्मक उपयोग अपनी कविताई के लिए किया। इन मानक कवियों का सर्वश्रेष्ठ लय प्रधान और संगीतात्मक है। जैसे निराला की क्लासिक कविता ‘राम की शक्ति पूजा’, ‘सरोज स्मृति’ और ‘तुलसीदास’। निराला की उत्तरकालीन कविताएं गीतात्मक हैं, निवेदन प्रधान हैं, विनय के भावों में अंकुरित हुई हैं। संगीत विमुख कविता एक सपाटपन पैदा करती है, जो कि अर्थ को सीधी चाल में प्रस्तुत कर देता है। जबकि संगीतात्मक कविता अर्थ में उछाल लाती है। अर्थ में छलांग पैदा करती है। अर्थ ध्वन्यात्मक हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अपने भीतर संघनित भी हो उठता है, जिसका समग्र प्रभाव चित्त पर हावी होने लगता है। मुक्तिबोध जो कि गद्य शैली में अपनी प्रबल कल्पनाशीलता को ढाल रहे थे, भावावेग को उद्दीप्त करते हैं, कलम में। ‘‘अंधेरे में’’ कविता आद्यंत सस्वर मंत्रपाठ जैसी है। ‘‘भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़।’’ या ‘‘तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब’’, ‘‘लिया बहुत बहुत ज्यादा, दिया बहुत बहुत कम।’’ जैसी अनेक पंक्तियां अभिनव रागात्मकता और असंतोष के सांचे में ढली हुई हैं।
संगीत विधा अपने आप में एक बेमिसाल सृजन है। परन्तु है यह ग़ैर-साहित्यिक। शायद साहित्यिक सृजन से पुरानी सृजनात्मक विधा। भावााभिव्यक्ति की दोनों विलक्षण शैलियां। दोनों का उद्देश्य मनुष्य के अंतर को समृद्ध, संवेदनशील और व्यापक बनाना है। साहित्यिक सृजन की कहानी संगीतमयता के साथ ही शुरु होती है। जो कि गीत विधा के रूप में स्थापित हुई। भावपूर्ण सृजन संगीत की ओर झुकता है और कलावादी सृजन बौद्धिकता की ओर। सृजन के दोनों रूप महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही कविता को ऊँचाई मिलती है, नयापन मिलता है। परन्तु प्रभाव जमाने वाली कविताई भावनात्मक कविताई ही मानी गयी है। यह अवश्य है, जिसे बौद्धिकता अधिक प्रिय है, वह भावनात्मक सृजन के बजाय कलात्मक सृजन अधिक पसन्द करेगा। सृजन में संगीत की भूमिका उसमें अलौकिक रस का संचार करना है। सृजन के स्थायित्व के लिए केवल ऊँचे, मौलिक, अलहदा और महत विचार काफी नहीं। जिस तरह वृक्ष चाहे कितना प्रकाश में नहाता रहे, किन्तु जड़ों में बहते रस के बगैर जीवित नहीं रह सकेगा, वैसे ही संगीत के बिना कविता। सृजन में संगीतात्मकता लाने की कोई तय युक्ति नहीं। कोई बना-बनाया फार्मूला नहीं। कोई नुस्ख़ा नहीं। जिस तरह सृजन अप्रत्याशित, अज्ञात प्रेरणा है। वैसे ही संगीतात्मकता। इसके अनिर्धारित रहने में ही इसकी उपयोगिता छिपी है। जब बंध जाती है, तो अनिवार्यतः सीमित हो जाती है। और बहुत हद तक बासी और अनुपयोगी भी। यह बेहद आवश्यक है कि सृजन में ढाली गयी लयात्मकता सामयिक हो, समीचीन और समय सापेक्ष हो। यदि हूबहू पुराने ढर्रे पर कविता को संगीत में ढाल दिए, तो सृजन का असफल और निरर्थक होना तय है।
यह दर हक़ीक़त है कि समूची समकालीन हिन्दी कविता की कहानी लयविमुख और संगीत विहीन होते चले जाने की यात्रा है। धूमिल के बाद बमुश्किल ऐसा कवि नज़र आएगा, जिसने लय और अंतःसंगीत को कविता में साधने की प्रतिबद्ध कोशिश की हो। कथन, संवाद, बतकही, वर्णन, व्यासपरकता समकालीन कविता के अनिवार्य, अखंड, अटूट स्वभाव बन गये। कोई तैयारी, अनुशासन, संयम या सलीके का साहित्यिक दबाव न रह गया। समकालीन कविता के दौर ने कविता लिखना इतना सस्ता, सुलभ और मामूली बना दिया, कि यूं ही बैठे-बैठे ऊपर-नीचे बतकही धर देने वाला भी कवि, चर्चित कवि बन सकात है। सृजन का एक अंतरानुशासन होता है, जो हर दौर में सृजन की गरिमा, विशिष्टता और ऊँचाई को थामे रहता है। समकालीन कविता ने किसी भी प्रकार के सृजनात्मक अनुशासन की अनिवार्यता ही खत्म कर दी। इसलिए सुधीश पचौरी जैसे आलोचक ‘कविता की मृत्यु’ की घोषणा करते हैं, तो उसके पीछे कारण हैं। इसमें दो मत नहीं, कि हिन्दी कविता ने अपने पाठक लगभग खो दिये हैं। केवल साहित्यिक पाठक रह गये हैं, जिनका किसी न किसी रूप में साहित्य से मतलब है, या साहित्यिक में भविष्य आजमाना चाहते हैं, वे ही कविता के स्थायी पाठक हैं। वरना नैसर्गिक पाठक, साहित्येतर पाठक समाप्त हो चुके हैं। समकालीन कविता ने तयपूर्वक तुकबंदी, तालबद्धता और छंदात्मकता से विदाई ली, एक अर्थ में उचित हुआ, क्योंकि इस शैली की नियमबद्ध मर्यादा में समय के नग्न, विकट, भीषण यथार्थ को बांधा ही नहीं जा सकता था। अभिव्यक्ति के अंदाज़ में खुलापन, स्वाधीनता बहुत अनिवार्य थीं परन्तु समकालीन कवियों ने इसका अर्थ लय से मुक्ति के अर्थ में भी ले लिया, संगीत से छुटकारा पाने के अर्थ में ले लिया। और यही आसान निष्कर्ष उनकी कविताई के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। तल्खी, तेवर, प्रवाह, आवेग और अंत-नृत्य समयजयी कविता के लिए बहुत जरूरी है, जिसे समकालीन कविता ने बेतरह खोया है। मुक्तिबोध स्वयं सारी वैचारिकी, संवेदना, प्रतीक और अभिनव कल्पनाशीलता भर देने के बावजूद लयात्मक आवेग का दामन नहीं छोड़ते। वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं, एक संकल्पबद्ध हृदय के उद्दाम आवेग और फक्कड़पन में ही। जैसे उनकी कविता की दो पंक्तियां:
सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं भूलूँ
तुम्हें भूल जाने की।
सवाल बहुत स्वाभाविक और ज़रूरी है कि समकालीन कविता में लय और संगीत को कैसे लौटाया जाये, कैसे उसमें रसात्मकता को पुनर्प्रतिष्ठित किया जाये। यह संभव होगा कविता में मौन भरने से, अर्थों के बीच गैप लाने से, पूरी कविता में गूंजती हुई चुप्पी पैदा करने से। जैसे संगीत में अंतराल का अनिवार्य महत्व है, जैसे ईंटों के जोड़ को मजबूती देने के लिए गैप का बड़ा महत्व है। जैसे आत्मीय रिश्तों के टिकाऊ रहने के लिए मर्यादा एक शर्त है, वैसे ही कविता में अर्थों की जीवंतता बनाए रखने के लिए अवकाश को। इस गैप, अंतराल और अवकाश में अर्थ की गूंज बनी रहती है। वह गूंज जो पाठक को महसूस होती है, उसे आंदोलित रखती है, बांधे रखती है, और कई बार विलक्षण अर्थों को खोज निकालने की प्रेरणा भी देती है। इसे ही हम ‘मर्म का संगीत’ कहते हैं, जो अनकहे में मौजूद रहता है, अप्रकट में प्रकट होता है, अनुपस्थिति में विद्यमान रहता है। विलक्षण अर्थ हमेशा रहस्यमय होते हैं, अप्रकट रहते हैं, अपरिभाषेय और अलक्षित भी। समकालीन कविता में ऐसे बहुत कम सर्जक हैं, जो अवकाश पैदा करके अर्थ में संगीत जगाने की कला जानते हैं। हमारे कवियों से हुनर लेना चाहिए, नाज़िम हिकमत जैसे कवियों से, जो गद्यात्मक कविता लिखते अवश्य हैं, परन्तु उसमें बड़े अर्थ की छलांग पैदा करने के साथ, आइए देखते हैं:
सिर्फ़ एक दिन के लिए यह दुनिया
चलो बच्चों को दे दें, खेलने के लिए

सृजन की किसी भी विधा में प्राणशक्ति, तात्विक मार्मिकता, संगीतमयता तभी आती है, जब जीवन में अनगढ़ नैसर्गिकता हो, जब जीवन धाराप्रवाह में हो, जब वह प्रतिबद्धता के राग में तरंगमय हो, जब वह एक पानी, एक चेहरे, एक जमीन का हो। जिसके भीतर अधिकांश आंतरिक शक्तियां खांटी, मौलिक, प्राकृतिक और अमिस्रित हो। सच्ची-कच्ची और अनगढ़ भावनायें अधिक उर्वर सिद्ध होती हैं, सशक्त सृजन के लिए। व्यक्तित्व में कांट-छांट, तराश, गढ़ाव, बनाव, खिलाव कवि के लिए अहितकर सिद्ध होता है। केवल धूमिल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसने कोई तराश, अतिरिक्त चमक और कारीगरी नहीं है, लेकिन वह आज भी समकालीन कविता में सबसे आगे उपस्थित हैं। रशियन भाषा के शीर्षस्थ कथाकार टालस्टाॅय का एक विचार बड़े महत्व का है, देखिए क्या कहते हैं- ‘‘लेखक को अपनी रचना से कहीं अधिक बड़ा होना चाहिए।’’ वे यह कह क्यों रहे हैं। इसीलिए कि वह भीतर से जितना बड़ा होता है, सृजन में उससे कम ही बड़ा हो पाता है। भीतर का शिखरत्व पैमाना है, बाहरी उच्चता का। जितना वह है, हूबहू उतना प्रकट हो ही नहीं सकता। अंतःव्यक्तित्व को बहुआयामी बनाकर, मार्मिकता देकर, अन्वेषी स्वभाव का बनाकर वह सृजन को भी विलक्षण गहराई और ऊँचाई दे सकता है, संदेह नहीं। मनुष्य द्वारा निर्मित संगीतात्मकता से भिन्न, बृहद और असाधारण सृष्टि का संगीत है, जो हमारे हर तरफ निनादित है। हर क्षण बज रहा है, हर दिशा में उपस्थित है। नदी का प्रवाह, बादलों की गरजन, बिजली की चमक या हवाओं का बहना, पक्षियों की बोल, जंगलों की झूम सबमें सृष्टि का वही अनादि, अखंड, अमर संगीत व्याप्त है। जो प्रचंड भी है और मधुर भी। जो प्रिय भी है, अप्रिय भी, जो आकर्षक और मोहक है, तो भयावह और भयकारी भी। हिन्दी ही नहीं, किसी भी भाषा की कविता यदि सृष्टि या प्रकृति के इस अनादि, रोमांचक, विस्मयकारी संगीत को साध ले जाय, तो निश्चय ही कविता का अविस्मरणीय नवजागरण हो सकता है। युगांत उपस्थित हो सकता है। जब सृजन में सृष्टि का संगीत उतरता है, तो शब्द आंधी के पत्ते रह जाते हैं, अर्थ लाचार नजर आते हैं। कविता विशुद्ध महाभाव हर जाती है। सृष्टि की लय से आप्लावित कविता, कविता नहीं विस्फोट है। कहना जरूरी है, कि यदि गद्यात्मकता के तनाव, आतंक और खिंचाव में शक्तिहीन, जीवनहीन होती चली जा रही समकालीन कविता को नवप्रतिष्ठित करना है, तो चित्तहारी अभिनव संगीतात्मकता उसकी एक अनिवार्य शर्त होगी।
(पुस्तक अंश : डॉ. भरत प्रसाद लिखित ‘सृजन का संगीत’ पुस्तक से यह वैचारिकी आब-ओ-हवा के लिए विशेष रूप से प्राप्त)

डॉ. भरत प्रसाद
हिंदी विभाग में प्राध्यापक, पूर्वांगन के अध्यक्ष और देशधारा वार्षिकी के संपादक भरत प्रसाद के नाम पर क़रीब डेढ़ दर्जन साहित्यिक पुस्तकें दर्ज हैं। इनमें काव्य संग्रह, उपन्यास, आलोचना, कहानी और वैचारिकी आधारित किताबें हैं। अनेक प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। आप अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाज़े जा चुके हैं और कुछ पत्रिकाओं के विशेषांकों का संपादन भी आपने किया है।
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit
- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky


अनुकरणवाद पहले ही कह चुका है कि कला प्रकृति की नकल है।यह अलग बात है कि अरस्तू ने इस नकल को रचनात्मक प्रक्रिया कहकर सृजन का सम्मान किया।
सृजन शब्द के लिए प्रथम प्रकृति जन्य सृजन ही अधिकारी है। हमेशा से ही विश्व में सृष्टि को परमसत्ता या ईश्वरीय सृजन कहा जाता है। मानव कृत सृजन बाद में ।
▫️’ संगीत शायद साहित्यिक सृजन से पुरानी विधा है। ‘—
शायद नहीं निश्चित ही। प्रकृति के सभी कार्यों की ध्वनि संगीतमय है -वर्षा, बूँदों की ध्वनि, पवन की गति और नदियों के बहाव की ध्वनि सभी संगीतात्मक ध्वनियाँ हैं जिनका अनुसरण मानव ने किया है।
संगीत के तत्व जैसे लय और धुन भाषा के विकास से पहले से ही मानव समाज में मौजूद थे ।
सृजनात्मक अनुशासन का पालन करने वाले, अनेक कवि स्वांत:सुखाय , छंदबद्ध, संगीतबद्ध उत्कृष्ट काव्य सृजन में लगे हैं । सभी साहित्यिक पत्रिकाएंँ लामबद्ध होकर इन छंदबद्ध पारंपरिक शैली की रचनाओं को प्रकाशित नहीं करतीं। वे रस ,लय , तथ्य विहीन गद्य को कविता के रूप में प्रस्तुत कर पाठकों को कविता के संसार से भलीभांति निष्कासित कर चुकी हैं।